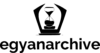अपठित गद्यांश (class 12 apathit gadyansh)
नीचे सभी अपठित गद्यांश (class 12 apathit gadyansh) नवीनतम परीक्षा प्रश्न-पत्र के अनुसार दिए गए हैं।
अपठित शब्द का अर्थ है- जो कभी पढ़ा न गया हो। अर्थात अपठित गद्यांश वं गद्द्यांश हैं जिनको छात्रों ने पहले कभी अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ा नहीं है। अपठित गद्यांश देकर उस पर भाव-बोध संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को उसी गद्यांश के आधार पर देने होते हैं। उत्तर देते समय यह कोशिश होनी चाहिए कि उत्तर में गद्यांश के वाक्यों को जैसा का तैसा न उतारा जाए बल्कि उसमें कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए।
अपठित गद्यांश (class 12 apathit gadyansh) का उद्देश्य
मूल्यांकन हेतु अपठित गद्यांश दिए जाने का अर्थ है- विद्यार्थियों का भाव या भाषा-बोध संबंधी ज्ञान का पता लगाना। अर्थात यह जानना कि छात्र उस गद्यांश की भाषा को समझते हैं या नहीं। साथ ही इससे उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का भी पता चल जाता है।
अपठित गद्यांश (class 12 apathit gadyansh) हल करते समय ध्यान देने योग्य बातें-
• दिए गए गद्यांश का एक-दो बार मौन वाचन करें और उसे गहराई से समझने का प्रयास करें।
• पहला कदम, सभी प्रश्नों को एक-एक करके पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के संभावित उत्तर को गद्यांश में तुरंत रेखांकित कर लें।
• उत्तर लेखन प्रारंभ करते समय, लेखक द्वारा कही गई मूल बात को सरल और स्पष्ट भाषा में छोटे-छोटे वाक्यों में व्यक्त करें। उत्तर लिखते समय गद्यांश के वाक्यों को ज्यों-का-त्यों न उतारें, बल्कि अपनी शब्दावली का उपयोग करें।
• शीर्षक देने की आवश्यकता होने पर, किसी रफ़ कागज पर दो-तीन उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखें। इसके बाद, उनमें से जो सर्वाधिक उपयुक्त लगे, उसे उत्तर के रूप में अंतिम रूप दें।
• यदि प्रश्नों का प्रारूप बहुविकल्पीय (MCQ) है, तो सारे विकल्पों को ध्यान से पढ़कर ही सबसे उचित विकल्प पर निशान लगाएँ।
हिंदी व्याकरण के नवीनतम पाठ्यक्रम और अन्य संसाधनों की जाँच के लिए आप NCERT की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
(Download 12 Hindi A & B papers in word format – Click Here)
अपठित गद्यांश (class 12 apathit gadyansh) के उदाहरण (नए पाठ्यक्रम विनिर्देशन के अनुसार)
अपठित गद्यांश (class 12 apathit gadyansh)
- विकास की प्रक्रिया केवल आर्थिक उन्नति तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और नैतिक पहलुओं का भी योगदान होता है। जब किसी देश की आर्थिक वृद्धि उसके नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में वास्तविक सुधार नहीं लाती, तब वह विकास अपूर्ण रह जाता है। उदाहरणस्वरूप, अगर किसी क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा हो लेकिन आम जन की पहुंच प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक न हो, तो उसे विकास नहीं कहा जा सकता। भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में समावेशी विकास की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ धर्म, भाषा, जाति, आर्थिक स्थिति और भौगोलिक अंतर इतने व्यापक हैं कि एकरूप विकास की परिकल्पना तभी साकार हो सकती है जब प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र को समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ। आज भी भारत के अनेक ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में स्वच्छ जल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ, शुद्ध पर्यावरण और सस्ती ऊर्जा जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। सरकारें इन समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न योजनाएँ और नीतियाँ बनाती हैं, लेकिन इनका सफल क्रियान्वयन कई बार धीमी प्रशासनिक प्रक्रियाओं, जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वार्थों के कारण प्रभावित होता है। इसके साथ ही, जनभागीदारी की कमी भी इन प्रयासों को अधूरा छोड़ देती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की सक्रिय भूमिका आवश्यक होती है; जब लोग अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक रहते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं, तब सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता है। इसके अलावा, वर्तमान में तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण, पारंपरिक रोजगारों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे भी विकास की परिभाषा को चुनौती दे रहे हैं। तकनीकी प्रगति और औद्योगीकरण के लाभों के साथ-साथ उनके दुष्परिणामों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। सतत विकास का अर्थ केवल आर्थिक संसाधनों की वृद्धि नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और सामाजिक समानता भी है। सच्चा विकास वही है जो प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करे, समाज में न्याय और समानता लाए तथा पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाए रखे।
प्रश्नपत्र:
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक प्रत्येक):
प्रश्न 1: भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता क्यों अधिक है? (1 अंक)
(क) आर्थिक असमानता के कारण
(ख) क्षेत्रीय विविधताओं के कारण
(ग) सांस्कृतिक एकरूपता के कारण
(घ) कृषि में कमी के कारण
प्रश्न 2: ‘सतत विकास’ से लेखक का तात्पर्य किससे है? (1 अंक)
(क) केवल आर्थिक वृद्धि
(ख) केवल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन
(ग) सामाजिक समानता और पर्यावरण संतुलन
(घ) केवल तकनीकी विकास
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): विकास केवल आर्थिक वृद्धि नहीं है।
Reason (R): विकास में सामाजिक और नैतिक पहलुओं की कोई भूमिका नहीं होती।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: गद्यांश के अनुसार, विकास को अधूरा क्यों माना जाता है? (1 अंक)
(क) जब केवल सरकार ही प्रयास करे
(ख) जब आर्थिक वृद्धि से जीवन गुणवत्ता न सुधरे
(ग) जब नागरिक केवल कर्तव्यों पर ज़ोर दें
(घ) जब सब लोग केवल पर्यावरण की बात करें
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: विकास में नागरिकों की भागीदारी क्यों आवश्यक मानी गई है? (2 अंक)
प्रश्न 6: लेखक ने पर्यावरणीय विषयों को विकास से कैसे जोड़ा है? (2 अंक)
प्रश्न 7: लेखक ने किन समस्याओं को योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा बताया है? (2 अंक)
उत्तर कुंजी:
प्रश्न 1: (ख) क्षेत्रीय विविधताओं के कारण
प्रश्न 2: (ग) सामाजिक समानता और पर्यावरण संतुलन
प्रश्न 3: (ख) A सही है, परंतु R गलत है।
प्रश्न 4: (ख) जब आर्थिक वृद्धि से जीवन गुणवत्ता न सुधरे
प्रश्न 5: लोकतांत्रिक देश में नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि वे अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते और केवल अधिकारों की अपेक्षा करते हैं, तो विकास अधूरा रह जाता है। जनभागीदारी से योजनाओं का सही क्रियान्वयन होता है और समाज में संतुलन बना रहता है।
प्रश्न 6: लेखक के अनुसार, केवल आर्थिक वृद्धि से विकास नहीं हो सकता जब तक पर्यावरण का संतुलन न बना रहे। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण सतत विकास के लिए अनिवार्य है।
प्रश्न 7: योजनाओं के क्रियान्वयन में धीमी प्रशासनिक प्रक्रियाएँ, भ्रष्टाचार, और राजनीतिक स्वार्थ प्रमुख बाधाएँ हैं। ये कारण नीतियों को जमीन पर प्रभावी रूप से लागू नहीं होने देते।
- जलवायु परिवर्तन आज विश्व की सबसे गंभीर और बहुआयामी चुनौतियों में से एक बन चुका है। इसके प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है — चाहे वह कृषि, स्वास्थ्य, जल संसाधन, आजीविका या वैश्विक आर्थिक संरचना हो। अनेक वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पुष्टि हो चुकी है कि पृथ्वी का औसत तापमान निरंतर बढ़ रहा है और इसका मुख्य कारण मानवीय गतिविधियाँ हैं। जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोल और डीज़ल का अत्यधिक प्रयोग, वनों की अंधाधुंध कटाई, अनियंत्रित औद्योगीकरण और शहरीकरण जैसे कारक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। जलवायु वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि कार्बन उत्सर्जन पर शीघ्र नियंत्रण नहीं किया गया, तो आने वाले दशकों में पृथ्वी का तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इससे ध्रुवीय बर्फ पिघलेगी, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, और तटीय क्षेत्र डूब सकते हैं, जिससे लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो सकते हैं। साथ ही, बाढ़, सूखा, अत्यधिक वर्षा, हीट वेव और जलवायु असंतुलन जैसी घटनाएँ और भी अधिक सामान्य हो जाएँगी। इन परिवर्तनों का प्रभाव सबसे अधिक विकासशील देशों पर पड़ेगा, जहाँ संसाधनों की पहले ही कमी है। यह समस्या केवल तकनीकी समाधानों से नहीं सुलझ सकती। इसके लिए आवश्यक है कि जन-सामान्य की सोच और जीवनशैली में भी परिवर्तन लाया जाए। ऊर्जा की बचत, सौर और पवन ऊर्जा जैसी हरित ऊर्जा का प्रयोग, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, एकल उपयोग प्लास्टिक से बचाव, और उपभोग की आदतों में संयम — ये सभी ऐसे छोटे-छोटे प्रयास हैं जो सामूहिक रूप से बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारों, वैश्विक संस्थाओं और कॉर्पोरेट कंपनियों को भी पर्यावरणीय नीतियों को कठोर बनाना होगा और उनके पालन को अनिवार्य करना होगा। केवल घोषणाएँ पर्याप्त नहीं हैं; ज़मीन पर अमल और पारदर्शिता भी उतनी ही ज़रूरी है। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष को केवल वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं या पर्यावरण कार्यकर्ताओं की ज़िम्मेदारी मान लेना उचित नहीं है। यह प्रत्येक नागरिक की नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वह स्वयं भी पर्यावरण की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाए। हमारी दैनिक आदतें — जैसे बिजली-पानी की बचत, स्थानीय उत्पादों का प्रयोग, पुनर्चक्रण की आदतें, और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता — ही मिलकर भविष्य के स्वरूप को निर्धारित करेंगी।
प्रश्नपत्र:
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक प्रत्येक):
प्रश्न 1: वैज्ञानिकों के अनुसार यदि कार्बन उत्सर्जन न रुका तो तापमान कितना बढ़ सकता है? (1 अंक)
(क) 1 से 2 डिग्री सेल्सियस
(ख) 2 से 3 डिग्री सेल्सियस
(ग) 3 से 5 डिग्री सेल्सियस
(घ) 5 से 6 डिग्री सेल्सियस
प्रश्न 2: लेखक के अनुसार जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा? (1 अंक)
(क) विकसित देशों पर
(ख) शहरी लोगों पर
(ग) समुद्री जीवों पर
(घ) विकासशील देशों पर
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): केवल तकनीकी उपायों से जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
Reason (R): जन-सामान्य की जीवनशैली का जलवायु परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: गद्यांश के अनुसार कौन से उपाय पर्यावरणीय परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं? (1 अंक)
(क) निजी वाहन का अधिक उपयोग
(ख) प्लास्टिक की पैकिंग में वृद्धि
(ग) ऊर्जा की बचत और पुनर्चक्रण
(घ) औद्योगिक उत्सर्जन को बढ़ाना
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले प्रमुख खतरे क्या हैं? (2 अंक)
प्रश्न 6: लेखक ने किन व्यक्तिगत प्रयासों को जलवायु समाधान में उपयोगी बताया है? (2 अंक)
प्रश्न 7: जलवायु संकट को केवल वैज्ञानिकों की समस्या मानने को लेखक क्यों गलत मानता है? (2 अंक)
उत्तर कुंजी:
प्रश्न 1: (ख) 2 से 3 डिग्री सेल्सियस
प्रश्न 2: (घ) विकासशील देशों पर
प्रश्न 3: (घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: (ग) ऊर्जा की बचत और पुनर्चक्रण
प्रश्न 5: जलवायु परिवर्तन से समुद्र का स्तर बढ़ सकता है, जिससे तटीय क्षेत्र डूब सकते हैं और लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं। इसके अलावा, बाढ़, सूखा, हीट वेव, और फसलों की क्षति जैसी आपदाएँ बढ़ सकती हैं।
प्रश्न 6: लेखक ने ऊर्जा की बचत, हरित ऊर्जा का उपयोग, सार्वजनिक परिवहन का समर्थन, उपभोग में संयम, और पुनर्चक्रण जैसी आदतों को उपयोगी बताया है जो व्यक्ति स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक हैं।
प्रश्न 7: लेखक के अनुसार जलवायु संकट समाज के हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है। केवल वैज्ञानिकों या नीति-निर्माताओं पर निर्भर रहना समाधान नहीं है। नागरिकों की जीवनशैली और दैनिक आदतें भी इसका समाधान तय करती हैं।
- भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज भी मुख्यतः कृषि पर आधारित है और इसमें पशुपालन, कुटीर उद्योग, ग्रामीण हस्तशिल्प तथा अन्य लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालाँकि शहरीकरण और औद्योगीकरण की गति में तीव्रता आई है, लेकिन भारत की लगभग 60% से अधिक आबादी आज भी गाँवों में निवास करती है। इन गाँवों में संसाधनों की गंभीर कमी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता, परिवहन की कमजोर स्थिति, और बेरोज़गारी जैसी समस्याएँ प्रचलित हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए अनेक योजनाएँ आरंभ कीं जिनमें पंचवर्षीय योजनाएँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि प्रमुख हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण समाज को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना था। कुछ हद तक इन योजनाओं से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन कई समस्याएँ अब भी वैसी की वैसी बनी हुई हैं। ग्रामीण भारत आज भी मूलभूत ज़रूरतों जैसे शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण स्कूल और रोजगार के अवसरों के लिए संघर्ष करता दिखाई देता है। कृषि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वह अब भी मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। सिंचाई की सीमित सुविधा, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की धीमी प्रक्रिया, गुणवत्ता युक्त बीज और खाद की लागत, और कृषि उत्पादों को बाज़ार तक पहुँचाने में आने वाली बाधाएँ किसानों की स्थिति को जटिल बनाती हैं। इसके अलावा, फसल का उचित मूल्य न मिल पाने और बिचौलियों की भूमिका ने किसानों की आय को सीमित कर दिया है। केवल सरकारी प्रयासों से इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण समाज स्वयं आगे आए, सहकारी संस्थाओं को मज़बूत किया जाए, स्वरोज़गार और लघु उद्यमों को बढ़ावा मिले ताकि आर्थिक गतिविधियों में विविधता लाई जा सके। आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण तभी होगा जब ग्रामीण नागरिक शिक्षित, जागरूक और तकनीकी रूप से सशक्त होंगे। इसके लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना, महिलाओं को आर्थिक निर्णयों में भागीदार बनाना, और पारंपरिक कौशल को आधुनिक बाज़ार से जोड़ना आवश्यक है। केवल आर्थिक योजनाओं से टिकाऊ विकास संभव नहीं; सामाजिक चेतना, सामुदायिक एकजुटता और सहभागी दृष्टिकोण भी उतने ही आवश्यक हैं।
प्रश्नपत्र:
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक प्रत्येक):
प्रश्न 1: ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या मानी गई है? (1 अंक)
(क) पर्यावरणीय असंतुलन
(ख) मानसून पर निर्भर कृषि
(ग) शहरीकरण का प्रभाव
(घ) महिलाओं की भागीदारी
प्रश्न 2: पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था? (1 अंक)
(क) किसानों को ऋण देना
(ख) सहकारी संस्थाएँ बनाना
(ग) गाँवों को बुनियादी सुविधाएँ देना
(घ) शहरों में उद्योग लगाना
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): ग्रामीण भारत में बेरोज़गारी का प्रमुख कारण शिक्षा की कमी है।
Reason (R): गाँवों में तकनीकी प्रशिक्षण की उपलब्धता व्यापक है।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: गद्यांश के अनुसार, किसानों की आय सीमित क्यों रह जाती है? (1 अंक)
(क) वे फसल नहीं उगाते
(ख) उनकी शिक्षा कम होती है
(ग) फसल का मूल्य नहीं मिलता और बिचौलियों की भूमिका रहती है
(घ) वे शहरों में काम करने जाते हैं
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कौन-कौन से उपाय आवश्यक बताए गए हैं? (2 अंक)
प्रश्न 6: लेखक ने कृषि से जुड़ी समस्याओं को कैसे स्पष्ट किया है? (2 अंक)
प्रश्न 7: टिकाऊ ग्रामीण विकास के लिए किन सामाजिक कारकों को आवश्यक बताया गया है? (2 अंक)
उत्तर कुंजी:
प्रश्न 1: (ख) मानसून पर निर्भर कृषि
प्रश्न 2: (ग) गाँवों को बुनियादी सुविधाएँ देना
प्रश्न 3: (ख) A सही है, परंतु R गलत है।
प्रश्न 4: (ग) फसल का मूल्य नहीं मिलता और बिचौलियों की भूमिका रहती है
प्रश्न 5: ग्रामीण समाज को शिक्षित करना, सहकारिता को बढ़ावा देना, स्वरोज़गार और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना, तथा पारंपरिक कौशल को आधुनिक बाज़ार से जोड़ना आवश्यक उपाय बताए गए हैं।
प्रश्न 6: लेखक ने बताया है कि कृषि अब भी मानसून पर निर्भर है। सिंचाई की सुविधा कम है, बीज-खाद महंगे हैं, और बाज़ार तक पहुँच कठिन है। साथ ही किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।
प्रश्न 7: सामाजिक चेतना, सामुदायिक सहभागिता, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं की भागीदारी तथा तकनीकी सशक्तिकरण को टिकाऊ ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक माना गया है।
- जलवायु परिवर्तन आज के समय की सबसे गंभीर वैश्विक समस्याओं में से एक बन चुका है। यह केवल पर्यावरणीय असंतुलन तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। औद्योगिक क्रांति के बाद से वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों—जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड—की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई है। जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई और अनियंत्रित औद्योगीकरण ने इस संकट को और गहरा बना दिया है। इन कारणों से पृथ्वी का औसत तापमान निरंतर बढ़ रहा है, जिससे ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ तेजी से पिघल रही है, समुद्र-स्तर में वृद्धि हो रही है, और जलवायु असंतुलन की घटनाएँ बढ़ रही हैं। इससे जैव विविधता में भारी गिरावट आई है और अनेक प्रजातियाँ विलुप्ति की कगार पर पहुँच गई हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समान रूप से सभी देशों पर नहीं पड़ता। विकासशील और पिछड़े देश, जो इस संकट के लिए बहुत कम ज़िम्मेदार हैं, सबसे अधिक दुष्परिणाम झेल रहे हैं। भारत जैसे देशों में इसका सीधा प्रभाव कृषि पर पड़ा है। अनियमित वर्षा, असमय बाढ़ और लंबे सूखे की स्थितियों के कारण फसलें नष्ट होती हैं और खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। किसानों की आय पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन के चलते स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर देखा जा रहा है। गर्मी की लहरें, जलजनित बीमारियाँ, वायु प्रदूषण से उत्पन्न श्वसन रोग, और त्वचा संबंधी समस्याएँ आम होती जा रही हैं। बच्चों, बुज़ुर्गों और कमज़ोर वर्गों के लिए यह और भी घातक है। जलवायु संकट से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेरिस समझौते के माध्यम से देशों ने कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने की प्रतिबद्धता जताई है। ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे प्रयास विकासशील देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा—जैसे सौर और पवन ऊर्जा—के प्रयोग को बढ़ावा देना एक सकारात्मक कदम है। लेकिन ये प्रयास तब तक पूर्ण नहीं माने जा सकते जब तक आम नागरिक अपनी जीवनशैली में ठोस बदलाव न लाएँ। प्लास्टिक के कम प्रयोग, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, ऊर्जा की बचत, कचरे का पुनर्चक्रण और हरित पौधारोपण जैसे छोटे-छोटे व्यक्तिगत प्रयास मिलकर एक बड़े परिवर्तन की नींव रख सकते हैं। सरकारें नीतियाँ बना सकती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन और प्रभाव तभी सुनिश्चित हो सकता है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसमें भागीदार बने। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध यह संघर्ष अब केवल वैज्ञानिकों, सरकारों या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का दायित्व नहीं रह गया है। यह हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण की रक्षा को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाए।
प्रश्नपत्र:
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक प्रत्येक):
प्रश्न 1: गद्यांश के अनुसार, औद्योगिक क्रांति के बाद किस गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई? (1 अंक)
(क) ऑक्सीजन और हाइड्रोजन
(ख) नाइट्रोजन और अमोनिया
(ग) ग्रीनहाउस गैसें
(घ) सल्फर और क्लोरीन
प्रश्न 2: जलवायु परिवर्तन का भारत में मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा है? (1 अंक)
(क) खनन और व्यापार पर
(ख) ग्रामीण शिक्षा पर
(ग) कृषि और स्वास्थ्य पर
(घ) समुद्री यातायात पर
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता पर भी असर पड़ता है।
Reason (R): जलवायु परिवर्तन केवल मानव जीवन को प्रभावित करता है, पर्यावरण को नहीं।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: गद्यांश के अनुसार, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या आवश्यक है? (1 अंक)
(क) केवल सरकारी बजट बढ़ाना
(ख) व्यक्तिगत जीवनशैली में परिवर्तन
(ग) अधिक कारखाने लगाना
(घ) समुद्री क्षेत्र का विस्तार
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: जलवायु परिवर्तन के कारण किन प्राकृतिक और सामाजिक क्षेत्रों पर दुष्प्रभाव पड़ा है? (2 अंक)
प्रश्न 6: लेखक ने आम नागरिकों के किस व्यवहार को जलवायु समाधान के लिए आवश्यक बताया है? (2 अंक)
प्रश्न 7: पेरिस समझौते और ग्रीन क्लाइमेट फंड का उद्देश्य क्या है? (2 अंक)
उत्तर कुंजी:
प्रश्न 1: (ग) ग्रीनहाउस गैसें
प्रश्न 2: (ग) कृषि और स्वास्थ्य पर
प्रश्न 3: (ख) A सही है, परंतु R गलत है।
प्रश्न 4: (ख) व्यक्तिगत जीवनशैली में परिवर्तन
प्रश्न 5: जलवायु परिवर्तन से ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, समुद्र-स्तर बढ़ रहा है, जैव विविधता घट रही है और अनेक प्रजातियाँ संकट में हैं। सामाजिक रूप से यह कृषि, स्वास्थ्य और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।
प्रश्न 6: लेखक ने बताया है कि नागरिकों को प्लास्टिक कम उपयोग करना, ऊर्जा की बचत करना, सार्वजनिक परिवहन अपनाना और पौधारोपण जैसे व्यवहारों को अपनाना चाहिए। ये व्यवहार जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक हैं।
प्रश्न 7: पेरिस समझौते का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को सीमित करना है। ग्रीन क्लाइमेट फंड विकासशील देशों को जलवायु संकट से निपटने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- भारतीय लोकतंत्र की सफलता केवल एक उत्कृष्ट संवैधानिक ढाँचे का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे अनेक अन्य कारक भी कार्यरत हैं—जैसे जागरूक नागरिक, स्वतंत्र प्रेस, प्रभावी न्यायपालिका और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली। जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद लोकतंत्र को अपनाया, तो अनेक अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और विद्वानों ने संदेह व्यक्त किया कि क्या इतना विविधतापूर्ण और सामाजिक असमानताओं से ग्रस्त देश लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान कर पाएगा। परंतु भारत ने पिछले सात दशकों में यह सिद्ध किया है कि लोकतंत्र केवल उसकी राजनीतिक प्रणाली नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का अभिन्न हिस्सा है। लोकतंत्र केवल मताधिकार तक सीमित नहीं रहता, वह एक ऐसी जीवन पद्धति है जो नागरिकों से विवेक, उत्तरदायित्व और सहभागिता की अपेक्षा करता है। यदि नागरिक केवल अपने अधिकारों पर बल देते हैं परंतु कर्तव्यों से विमुख रहते हैं, तो लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। राष्ट्र की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतने ही जागरूक रहें जितना कि अधिकारों के प्रति। स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जो सरकार की नीतियों की समीक्षा करता है, जनमत का निर्माण करता है और नागरिकों को सूचनाएँ प्रदान करता है। मीडिया के इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के कारण वह सत्ता के प्रति एक उत्तरदायी दृष्टिकोण को स्थापित करता है। किंतु आज के युग में मीडिया की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। जब प्रेस व्यावसायिक लाभ, राजनीतिक दबाव या पूर्वग्रहों से संचालित होता है, तो वह अपने वास्तविक कर्तव्य से विमुख हो जाता है और लोकतांत्रिक चेतना को क्षति पहुँचती है। इसी प्रकार चुनाव प्रणाली लोकतंत्र की आत्मा है। यदि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त नहीं होते, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार ही डगमगा जाता है। आज जब चुनावों में धन, बल, झूठे प्रचार और सांप्रदायिक भावनाओं का प्रयोग किया जाता है, तब यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक मतदाता निडर होकर, विवेक के साथ, अपने मत का प्रयोग करे। लोकतंत्र को केवल सरकार द्वारा लागू की जाने वाली प्रणाली न मानकर, हर नागरिक को इसे अपने जीवन का नैतिक और सामाजिक मूल्य बनाना होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि लोकतंत्र की सच्ची शक्ति न केवल संविधान में, बल्कि जागरूक, उत्तरदायी और नैतिक नागरिकों में निहित होती है।
प्रश्नपत्र:
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक प्रत्येक):
प्रश्न 1: लेखक के अनुसार लोकतंत्र की सच्ची शक्ति कहाँ निहित है? (1 अंक)
(क) संसद में
(ख) संविधान में
(ग) नागरिकों में
(घ) न्यायपालिका में
प्रश्न 2: मीडिया को लोकतंत्र का कौन-सा स्तंभ कहा गया है? (1 अंक)
(क) तीसरा
(ख) पाँचवाँ
(ग) पहला
(घ) चौथा
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): लोकतंत्र में केवल अधिकारों की माँग करना पर्याप्त नहीं है।
Reason (R): क्योंकि लोकतंत्र उत्तरदायित्व और कर्तव्य की माँग करता है।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सबसे अधिक कौन-से तत्व कमजोर करते हैं? (1 अंक)
(क) स्वतंत्र मताधिकार
(ख) राजनीतिक विमर्श
(ग) झूठा प्रचार, धनबल और भय
(घ) न्यायिक समीक्षा
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: लेखक ने नागरिकों की भूमिका लोकतंत्र में कैसे स्पष्ट की है? (2 अंक)
प्रश्न 6: मीडिया की निष्पक्षता पर क्या प्रश्न उठाए गए हैं? (2 अंक)
प्रश्न 7: लेखक के अनुसार चुनावी प्रणाली की निष्पक्षता क्यों आवश्यक है? (2 अंक)
उत्तर कुंजी:
प्रश्न 1: (ग) नागरिकों में
प्रश्न 2: (घ) चौथा
प्रश्न 3: (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
प्रश्न 4: (ग) झूठा प्रचार, धनबल और भय
प्रश्न 5: लेखक के अनुसार नागरिक केवल मत डालने तक सीमित न रहें, बल्कि वे अपने कर्तव्यों को भी समझें। अधिकारों के साथ-साथ उत्तरदायित्व भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक हैं।
प्रश्न 6: लेखक ने संकेत दिया कि मीडिया कभी-कभी राजनीतिक प्रभाव या व्यावसायिक लाभ के चलते पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है, जिससे उसकी स्वतंत्रता और लोकतंत्र दोनों प्रभावित होते हैं।
प्रश्न 7: यदि चुनाव निष्पक्ष और भयमुक्त न हों, तो लोकतंत्र का आधार कमजोर पड़ता है। सही और विवेकपूर्ण मतदान ही लोकतंत्र को स्थायित्व देता है।
- भारत की ग्रामीण संस्कृति ने देश की आत्मा और पहचान को गहराई से सँजोए रखा है। शहरीकरण और आधुनिकता की तेज़ रफ्तार ने जहाँ नगरों को वैश्विक पहचान दी है, वहीं गाँवों की मूलभूत विशेषताएँ जैसे आत्मनिर्भरता, सामुदायिक सहयोग और प्रकृति के प्रति गहन श्रद्धा धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही हैं। भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, जहाँ जीवन भले ही सुविधाओं से वंचित हो, पर उसमें मानवता, परंपरा और श्रम की गरिमा जीवित है। किसान, जो इस व्यवस्था का केंद्रीय पात्र है, अपने परिश्रम से समस्त राष्ट्र को अन्न उपलब्ध कराता है, पर स्वयं आज कई संकटों से घिरा है। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी सामने आए—रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता घट गई, जल स्रोत प्रदूषित हो गए और पारंपरिक कृषि ज्ञान उपेक्षित हो गया। इसके साथ ही, ग्रामीण युवाओं में शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति तेज़ हुई है। उन्हें लगता है कि शहरी जीवन में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ और रोज़गार के अवसर उपलब्ध हैं। इस प्रवृत्ति ने ग्रामीण श्रम शक्ति को कम किया है और गाँवों की पारंपरिक कलाएँ तथा कौशल धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। यद्यपि सरकार ने मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि, स्वच्छ भारत मिशन जैसी अनेक योजनाएँ प्रारंभ की हैं जिनका उद्देश्य गाँवों को सशक्त बनाना है, लेकिन इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव उनके क्रियान्वयन की पारदर्शिता और स्थानीय प्रशासन की निष्ठा पर निर्भर करता है। गाँवों में आज भी शिक्षा का स्तर निम्न है, स्वास्थ्य सेवाएँ सीमित हैं और सामाजिक कुरीतियाँ जैसे लिंग भेद, जातिगत भेदभाव आदि विद्यमान हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि ग्रामीण समाज का भविष्य केवल आर्थिक विकास से सुनिश्चित नहीं हो सकता। यदि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली और उद्यमिता की भावना गाँवों तक पहुँचाई जाए, तो भारत का यह भाग पुनः आत्मनिर्भर, उन्नत और प्रेरणादायक बन सकता है। गाँवों की आत्मा उनकी संस्कृति और नैतिक मूल्यों में निहित है। जब तक हम इन मूल्यों को पुनर्जीवित नहीं करते, तब तक ग्रामीण भारत का वास्तविक पुनरुत्थान संभव नहीं होगा। इसलिए, आज आवश्यकता है एक समन्वित दृष्टिकोण की, जिसमें परंपरा और नवाचार दोनों को समान महत्व मिले।
प्रश्नपत्र:
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक प्रत्येक):
प्रश्न 1: गद्यांश के अनुसार, हरित क्रांति का कौन-सा नकारात्मक प्रभाव सामने आया है? (1 अंक)
(क) कृषि उत्पादों में कमी
(ख) रासायनिक खाद की अनुपलब्धता
(ग) मिट्टी की उर्वरता और जल स्रोतों को क्षति पहुँचना
(घ) किसानों का विदेशी पलायन
प्रश्न 2: ग्रामीण युवाओं के शहरों की ओर पलायन का मुख्य कारण क्या बताया गया है? (1 अंक)
(क) राजनीतिक अस्थिरता
(ख) करों में वृद्धि
(ग) बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की चाह
(घ) कृषि से मोहभंग
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): ग्रामीण भारत का पुनरुत्थान केवल आर्थिक प्रगति से संभव है।
Reason (R): सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य विकास के मार्ग में बाधक हैं।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: लेखक के अनुसार सरकार की योजनाएँ कब सफल हो सकती हैं? (1 अंक)
(क) जब उनमें केवल तकनीकी सहायता मिले
(ख) जब प्रशासन की पारदर्शिता और सक्रियता हो
(ग) जब गाँवों को शहर बना दिया जाए
(घ) जब किसानों को आयकर से मुक्त किया जाए
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: हरित क्रांति के दुष्परिणामों का ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? (2 अंक)
प्रश्न 6: लेखक ने गाँवों के सांस्कृतिक और नैतिक पक्ष को कैसे महत्वपूर्ण बताया है? (2 अंक)
प्रश्न 7: ग्रामीण भारत को पुनः आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन-से उपाय आवश्यक माने गए हैं? (2 अंक)
उत्तर कुंजी:
प्रश्न 1: (ग) मिट्टी की उर्वरता और जल स्रोतों को क्षति पहुँचना
प्रश्न 2: (ग) बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की चाह
प्रश्न 3: (घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: (ख) जब प्रशासन की पारदर्शिता और सक्रियता हो
प्रश्न 5: हरित क्रांति से कृषि उत्पादन बढ़ा, पर अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता घटी, जल स्रोत प्रदूषित हुए और पारंपरिक कृषि ज्ञान उपेक्षित हो गया। इससे ग्रामीण जीवन की पारिस्थितिकी गड़बड़ा गई।
प्रश्न 6: लेखक ने बताया कि गाँवों की आत्मा उनकी संस्कृति, सहकारिता और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता में है। केवल भौतिक संसाधनों से नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों से भी गाँव सशक्त बनते हैं।
प्रश्न 7: शिक्षा, तकनीक, वैज्ञानिक कृषि, नवाचार, पारदर्शी योजनाएँ और स्थानीय प्रशासन की सक्रियता आवश्यक उपाय बताए गए हैं जिससे गाँव आत्मनिर्भर और प्रेरणास्पद बन सकें।
- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वदेशी आंदोलन एक निर्णायक मोड़ के रूप में उभरा जिसने स्वतंत्रता के संघर्ष को केवल राजनीतिक मंच तक सीमित न रखकर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक चेतना से जोड़ दिया। इस आंदोलन की शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप हुई थी, परंतु इसकी जड़ें शीघ्र ही संपूर्ण भारत में फैल गईं। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य केवल विदेशी वस्त्रों और सामानों का बहिष्कार नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता की भावना को जन-जन में स्थापित करना था। यह आंदोलन भारतीय जनमानस को जागरूक बनाकर उन्हें अपने देशी उत्पादों, कारीगरों और संसाधनों के प्रति सम्मान देना सिखाता था। इस आंदोलन के माध्यम से भारतीय हस्तशिल्प, खादी, स्वदेशी विद्यालय और देसी शिक्षा पद्धतियों को पुनः प्रतिष्ठा मिली। यह आंदोलन एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण था, जिसने केवल ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं किया बल्कि भारत की आत्मा को पुनः पहचान दिलाई। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को केवल आर्थिक बहिष्कार की नीति नहीं, बल्कि जीवन-दर्शन की संज्ञा दी। उनके लिए स्वदेशी का अर्थ था – अपने देश के संसाधनों, जनशक्ति और मूल्यों में विश्वास रखना तथा उनके उपयोग को प्राथमिकता देना। चरखा चलाकर उन्होंने इसे आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक बना दिया। उन्होंने माना कि जब तक भारतवासी मानसिक रूप से पराधीन हैं और विदेशी वस्तुओं को श्रेष्ठ मानते हैं, तब तक स्वतंत्रता अधूरी है। स्वदेशी आंदोलन का गहरा संदेश यह था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि वह एक मानसिक, नैतिक और सांस्कृतिक स्थिति है। आज वैश्वीकरण के युग में, जहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ और वैश्विक बाजार हमारे जीवन में गहराई से प्रवेश कर चुके हैं, वहाँ स्वदेशी की भावना को बनाए रखना एक चुनौती है। उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, विज्ञापन आधारित मानसिकता और ब्रांड संस्कृति ने लोगों को देशी उत्पादों से दूर कर दिया है। परंतु भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए ‘वोकल फॉर लोकल’, ‘मेक इन इंडिया’ जैसे अभियानों ने इस भावना को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। आज स्वदेशी का अर्थ केवल भारतीय उत्पाद खरीदना नहीं, बल्कि भारतीयता को जीवन के हर क्षेत्र में अपनाना है। स्वदेशी आंदोलन हमें यह सिखाता है कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी आवश्यक है। यही आत्मबल किसी भी राष्ट्र की सच्ची शक्ति बनता है।
प्रश्नपत्र:
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक प्रत्येक):
प्रश्न 1: स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के विरोध में हुई थी? (1 अंक)
(क) जलियाँवाला बाग हत्याकांड
(ख) बंगाल विभाजन
(ग) चौरी-चौरा कांड
(घ) असहयोग आंदोलन
प्रश्न 2: महात्मा गांधी ने स्वदेशी को किस रूप में देखा? (1 अंक)
(क) आर्थिक प्रतिरोध
(ख) स्वतंत्रता की अंतिम अवस्था
(ग) जीवन का दर्शन
(घ) धार्मिक आंदोलन
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): गांधीजी ने चरखे को आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना।
Reason (R): चरखा भारत के परंपरागत हथियारों का उदाहरण था।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: वर्तमान में स्वदेशी भावना को पुनर्जीवित करने के लिए कौन-से अभियान चलाए गए हैं? (1 अंक)
(क) डिज़िटल इंडिया और आयुष्मान भारत
(ख) मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल
(ग) ग्रीन इंडिया और उज्ज्वला योजना
(घ) स्वच्छ भारत और सागरमाला
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय समाज पर कौन-कौन से सकारात्मक प्रभाव डाले? (2 अंक)
प्रश्न 6: वैश्वीकरण के युग में स्वदेशी भावना के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं? (2 अंक)
प्रश्न 7: लेखक के अनुसार आत्मनिर्भरता का वास्तविक अर्थ क्या है? (2 अंक)
उत्तर कुंजी:
प्रश्न 1: (ख) बंगाल विभाजन
प्रश्न 2: (ग) जीवन का दर्शन
प्रश्न 3: (ख) A सही है, परंतु R गलत है।
प्रश्न 4: (ख) मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल
प्रश्न 5: स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता, आत्मगौरव और राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहित किया। भारतीय उत्पादों, कारीगरों और हस्तशिल्प को सम्मान मिला तथा शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में नवचेतना आई।
प्रश्न 6: आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों, ब्रांड संस्कृति, उपभोक्तावाद और विज्ञापन संस्कृति ने लोगों को विदेशी वस्तुओं की ओर मोहित कर दिया है जिससे देशी उत्पादों की उपेक्षा हो रही है।
प्रश्न 7: लेखक के अनुसार आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना नहीं है, बल्कि मानसिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी अपने देश और उसकी शक्तियों पर विश्वास करना आत्मनिर्भरता का वास्तविक रूप है।
- मानव सभ्यता का विकास जितना तीव्र हुआ है, उतनी ही तीव्रता से उसकी समस्याएँ भी जटिल होती गई हैं। प्रारंभिक काल में जहाँ भोजन, वस्त्र और आश्रय ही मानव जीवन की मूल आवश्यकताएँ थीं, वहीं आज मानसिक शांति, भावनात्मक सुरक्षा, सामाजिक सामंजस्य और पर्यावरणीय संतुलन जैसी अपेक्षाएँ भी जीवन का अनिवार्य अंग बन चुकी हैं। तकनीकी प्रगति ने जीवन को सुविधाजनक और तेज़ अवश्य बना दिया है, किंतु उसने अनेक सामाजिक और पारिवारिक विकृतियाँ भी जन्म दी हैं। विशेष रूप से आधुनिक तकनीकों जैसे मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने युवाओं की सोच, जीवनशैली और संबंधों पर गहरा प्रभाव डाला है। यद्यपि ये माध्यम सूचना के तीव्र प्रसार के लिए उपयोगी हैं, परंतु इनके अत्यधिक प्रयोग ने युवाओं को आत्मकेंद्रित, अधीर और सामाजिक रूप से अलग-थलग कर दिया है। तुलना की प्रवृत्ति और बाहरी दिखावे की संस्कृति ने विशेष रूप से किशोरों में आत्म-सम्मान की भावना को क्षीण किया है। साथ ही, शहरीकरण और एकल परिवारों की संख्या में वृद्धि ने परिवार की पारंपरिक संरचना को कमजोर किया है। आज के समय में बुजुर्गों की उपेक्षा, माता-पिता और बच्चों के बीच संवाद की कमी, तथा बच्चों में व्यवहारिक समस्याएँ सामान्य रूप से देखी जाती हैं। यह स्पष्ट है कि तकनीकी प्रगति अपने आप में समस्या का समाधान नहीं है। समाधान भावनात्मक बौद्धिकता, पारिवारिक समर्थन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना में निहित है। आवश्यकता इस बात की है कि भौतिक सुख-सुविधाओं की दौड़ में हम आत्मिक और मानसिक शांति की अनदेखी न करें। शिक्षा का उद्देश्य केवल अकादमिक ज्ञान देना नहीं है, बल्कि यह भी सिखाना है कि जीवन को कैसे सजीव, संतुलित और सुसंस्कृत ढंग से जिया जाए। यदि आत्मानुशासन, सहानुभूति, आत्मनिरीक्षण, और संवाद जैसे मूल जीवन-मूल्य शिक्षा के केंद्र में आएँ, तो सामाजिक समरसता की दिशा में सार्थक कदम उठाया जा सकता है। आज के संदर्भ में एक ऐसे समाज की आवश्यकता है जहाँ व्यक्ति तकनीक का उपयोग करे, पर तकनीक उस पर हावी न हो; जहाँ भौतिक उपलब्धियों के साथ-साथ मानसिक संतुलन और मानवीय संवेदनाएँ भी जीवन का अभिन्न हिस्सा हों।
प्रश्नपत्र:
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक प्रत्येक):
प्रश्न 1: लेखक के अनुसार आधुनिक तकनीक ने मानव जीवन में किस प्रकार की जटिलताएँ उत्पन्न की हैं? (1 अंक)
(क) केवल आर्थिक असमानता बढ़ी है
(ख) पारिवारिक सहयोग में वृद्धि हुई है
(ग) सामाजिक अलगाव और मानसिक तनाव उत्पन्न हुए हैं
(घ) शिक्षा व्यवस्था सरल हो गई है
प्रश्न 2: शिक्षा का उद्देश्य लेखक के अनुसार क्या होना चाहिए? (1 अंक)
(क) नौकरी दिलाना
(ख) जीवन जीने की कला सिखाना
(ग) प्रतियोगी परीक्षा पास कराना
(घ) तकनीकी कौशल बढ़ाना
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): तकनीकी प्रगति से युवाओं में आत्मकेंद्रितता और अधैर्य की प्रवृत्ति बढ़ी है।
Reason (R): क्योंकि सोशल मीडिया ने संवाद को सरल बना दिया है।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: लेखक के अनुसार संतुलित समाज की रचना किन मूल्यों के आधार पर हो सकती है? (1 अंक)
(क) विज्ञापन और उपभोक्तावाद
(ख) आत्मानुशासन, सहानुभूति, आत्मनिरीक्षण
(ग) तकनीकी श्रेष्ठता और प्रतियोगिता
(घ) शहरीकरण और निजी स्वार्थ
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: लेखक ने तकनीकी प्रगति के किस प्रकार के प्रभावों की ओर संकेत किया है? (2 अंक)
प्रश्न 6: किशोरों में आत्म-सम्मान की कमी के क्या कारण बताए गए हैं? (2 अंक)
प्रश्न 7: शिक्षा को लेकर लेखक की क्या अपेक्षाएँ हैं? (2 अंक)
उत्तर कुंजी:
प्रश्न 1: (ग) सामाजिक अलगाव और मानसिक तनाव उत्पन्न हुए हैं
प्रश्न 2: (ख) जीवन जीने की कला सिखाना
प्रश्न 3: (ख) A सही है, परंतु R गलत है।
प्रश्न 4: (ख) आत्मानुशासन, सहानुभूति, आत्मनिरीक्षण
प्रश्न 5: लेखक ने बताया कि आधुनिक तकनीक के अत्यधिक प्रयोग से सामाजिक अलगाव, मानसिक तनाव, और पारिवारिक संवाद में कमी जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं, विशेषकर युवाओं में।
प्रश्न 6: किशोर दूसरों से निरंतर तुलना करते हैं और सोशल मीडिया के बाहरी दिखावे से प्रभावित होकर स्वयं को कमतर मानने लगते हैं, जिससे आत्म-सम्मान घटता है।
प्रश्न 7: शिक्षा केवल ज्ञान का हस्तांतरण नहीं, बल्कि जीवन जीने की समझ, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, संवाद और संतुलित दृष्टिकोण सिखाने वाली होनी चाहिए।
- भारतीय लोकतंत्र का आधार जनता की भागीदारी है, लेकिन विडंबना यह है कि आम जन केवल मतदान के समय ही सक्रिय दिखाई देते हैं। लोकतंत्र का तात्पर्य केवल मत देना या सरकार चुनना नहीं है, बल्कि शासन, निर्णय और नीति निर्माण में जनसहभागिता भी इसका मूल तत्व है। दुर्भाग्यवश, भारत में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो यह मानकर चलता है कि सरकार ही सब कुछ करेगी, और उनकी भूमिका केवल शिकायत करने तक सीमित है। लोकतंत्र तभी सशक्त भारतीय लोकतंत्र की सफलता का मूल आधार जनता की भागीदारी है, किंतु विडंबना यह है कि अधिकांश नागरिक लोकतंत्र को केवल मतदान तक सीमित समझते हैं। लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप केवल सरकार चुनना नहीं, बल्कि शासन की प्रक्रिया में निरंतर सहभागिता करना है। नीतियों के निर्माण, उनके क्रियान्वयन और निगरानी में जन भागीदारी लोकतंत्र की आत्मा है। दुर्भाग्यवश, देश का एक बड़ा हिस्सा यह मानकर चलता है कि सरकार ही सब कुछ करेगी, और उनकी भूमिका केवल शिकायत करने तक सीमित रह जाती है। जब तक नागरिक अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग नहीं होंगे, तब तक लोकतंत्र केवल एक ढांचा रह जाएगा, उसमें जीवन नहीं होगा। केवल सोशल मीडिया पर सक्रियता दिखाना या पांच वर्षों में एक बार मतदान करना पर्याप्त नहीं है। नागरिकों को अपने आस-पास के पर्यावरण, स्वच्छता, शिक्षा, जल संरक्षण, और प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी दिखानी चाहिए। इसके विपरीत, राजनैतिक दलों ने भी लोकतंत्र को ‘वोट बैंक’ की मानसिकता तक सीमित कर दिया है। चुनाव के समय आम जनता को लुभाने की कोशिश होती है, किंतु शेष समय न तो पारदर्शिता होती है और न ही सरकारें नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनी रहती हैं। मीडिया की भूमिका भी कुछ अवसरों पर आलोचना के घेरे में आती है, जब वह जनहित के मुद्दों को छोड़कर केवल सनसनी फैलाने वाले समाचारों पर केंद्रित हो जाता है। यद्यपि स्थिति निराशाजनक है, लेकिन पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। हाल के वर्षों में युवाओं की सक्रियता में वृद्धि हुई है। कई युवा न केवल राजनीति में रुचि ले रहे हैं, बल्कि स्वयंसेवी संस्थाओं, पर्यावरण अभियानों और शिक्षा से जुड़े सामाजिक कार्यों में भाग ले रहे हैं। यह जागरूकता और सक्रियता लोकतंत्र की परिपक्वता का संकेत है। नागरिक जब सचेत, संगठित और सक्रिय होते हैं, तब लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं, बल्कि एक जीवंत जनजीवन बन जाता है। ऐसे में आवश्यक है कि शिक्षा, संवाद और संवेदनशीलता को लोकतांत्रिक संस्कृति का अभिन्न अंग बनाया जाए, जिससे प्रत्येक नागरिक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार बन सके।
प्रश्नपत्र:
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक प्रत्येक):
प्रश्न 1: लेखक के अनुसार लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप क्या है? (1 अंक)
(क) केवल सरकार बदलना
(ख) जन भागीदारी और नीति निर्माण में सहभागिता
(ग) केवल मतदान
(घ) राजनैतिक दलों की आलोचना
प्रश्न 2: लेखक ने मीडिया की कौन-सी भूमिका को आलोचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया है? (1 अंक)
(क) शिक्षा को बढ़ावा देना
(ख) युवा पीढ़ी को प्रेरित करना
(ग) तथ्य छोड़कर सनसनी पर ध्यान देना
(घ) सूचना के प्रसार को मजबूत करना
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): लोकतंत्र में नागरिकों की केवल शिकायत करने की भूमिका होनी चाहिए।
Reason (R): क्योंकि सरकार ही सभी समस्याओं का समाधान करती है।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: हाल के वर्षों में कौन-सा परिवर्तन लोकतंत्र की परिपक्वता का संकेत माना गया है? (1 अंक)
(क) युवा राजनीति से दूरी बना रहे हैं
(ख) सोशल मीडिया पर व्यंग्य लेखन
(ग) युवा स्वयंसेवी कार्यों में भाग ले रहे हैं
(घ) केवल मतदान प्रतिशत में वृद्धि
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: लेखक के अनुसार भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? (2 अंक)
प्रश्न 6: लोकतंत्र को जीवंत और प्रभावी बनाने के लिए नागरिकों को क्या करना चाहिए? (2 अंक)
प्रश्न 7: लेखक ने युवाओं की भूमिका को लोकतंत्र के संदर्भ में किस रूप में देखा है? (2 अंक)
उत्तर कुंजी:
प्रश्न 1: (ख) जन भागीदारी और नीति निर्माण में सहभागिता
प्रश्न 2: (ग) तथ्य छोड़कर सनसनी पर ध्यान देना
प्रश्न 3: (घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: (ग) युवा स्वयंसेवी कार्यों में भाग ले रहे हैं
प्रश्न 5: लेखक के अनुसार लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि नागरिक केवल मतदान के समय सक्रिय होते हैं, और शासन में निरंतर भागीदारी नहीं निभाते।
प्रश्न 6: लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए, नीति-निर्माण, स्वच्छता, पर्यावरण आदि में भागीदारी दिखानी चाहिए।
प्रश्न 7: लेखक ने युवाओं को लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रतीक माना है क्योंकि वे अब राजनीति और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।
- आज का युग तकनीक और डिजिटल संचार का युग है जहाँ सूचना का प्रवाह अत्यधिक तीव्र हो चुका है। इंटरनेट, मोबाइल और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने हमारे संवाद, ज्ञान प्राप्ति और विचार-विनिमय के तरीकों में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। एक क्लिक पर सैकड़ों सूचनाएँ उपलब्ध हैं, लेकिन इन सूचनाओं की प्रामाणिकता और उपयोगिता की जाँच करना अधिकांश लोगों के लिए कठिन है। परिणामस्वरूप, अनेक बार अधूरी, भ्रामक या पूरी तरह झूठी जानकारियाँ समाज में भ्रम, भय और द्वेष का वातावरण बना देती हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी समाचार और अफवाहों के प्रसार की गति इतनी तेज होती है कि उसका प्रभाव व्यापक और त्वरित होता है। इस संकट की पृष्ठभूमि में ‘मीडिया साक्षरता’ का महत्व बढ़ गया है। इसका आशय केवल मीडिया चलाना भर नहीं, बल्कि सूचना के स्रोत की पहचान, उसके सत्यापन और विवेकपूर्ण उपयोग से है। दुर्भाग्यवश, विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में मीडिया साक्षरता को अभी भी पाठ्यक्रम का आवश्यक हिस्सा नहीं माना गया है। इसका परिणाम यह है कि युवा वर्ग—जो कि तकनीक के सबसे बड़े उपयोगकर्ता हैं—फर्जी खबरों और भ्रमजनक प्रचार के सबसे बड़े शिकार भी बन रहे हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि उन्हें प्रारंभिक स्तर से ही सिखाया जाए कि किसी भी सूचना पर आँख मूँदकर विश्वास न करें, बल्कि तथ्य-जाँच की प्रक्रिया अपनाएँ। सकारात्मक बात यह है कि कुछ गैर-सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थाएँ और डिजिटल मंच इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। वे कार्यशालाओं, वेबिनार और डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को यह सिखा रहे हैं कि कैसे वे सूचना की प्रामाणिकता परखें और अपने डिजिटल व्यवहार को जिम्मेदार बनाएँ। इस डिजिटल युग में जहाँ सूचना शक्ति है, वहीं वह उत्तरदायित्व की भी माँग करती है। यदि उपयोगकर्ता अपने विवेक, नैतिकता और सामाजिक चेतना के साथ तकनीकी साधनों का प्रयोग करें, तो यह माध्यम समाज को सशक्त बना सकता है। लेकिन यदि यही माध्यम अज्ञानता, जल्दबाजी या पूर्वग्रह से युक्त हो जाए, तो यह समाज को बाँटने और भ्रमित करने का उपकरण भी बन सकता है। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि तकनीक का उपयोग ज्ञान, विवेक और दायित्व-बोध के साथ किया जाए।
प्रश्नपत्र:
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक प्रत्येक):
प्रश्न 1: लेखक के अनुसार ‘मीडिया साक्षरता’ का आशय क्या है? (1 अंक)
(क) केवल समाचार पढ़ना आना
(ख) मीडिया चैनलों की संख्या जानना
(ग) सूचना के स्रोत और सत्यता की पहचान करना
(घ) केवल मोबाइल और इंटरनेट चलाना
प्रश्न 2: लेखक के अनुसार सोशल मीडिया पर फर्जी समाचार का मुख्य प्रभाव क्या है? (1 अंक)
(क) मनोरंजन बढ़ता है
(ख) समाज में भ्रम और भय फैलता है
(ग) शिक्षा व्यवस्था मजबूत होती है
(घ) तकनीकी ज्ञान बढ़ता है
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): डिजिटल माध्यम अत्यधिक सशक्त और संवेदनशील है।
Reason (R): क्योंकि इससे सूचनाओं का प्रचार बहुत धीमी गति से होता है।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: लेखक के अनुसार मीडिया साक्षरता का प्रशिक्षण किन माध्यमों से दिया जा रहा है? (1 अंक)
(क) केवल विद्यालयों में
(ख) टीवी चैनलों के विज्ञापनों द्वारा
(ग) वेबिनार, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से
(घ) सोशल मीडिया पोस्ट द्वारा
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: लेखक ने सूचना के तीव्र प्रवाह को लेकर किस समस्या की ओर ध्यान दिलाया है? (2 अंक)
प्रश्न 6: मीडिया साक्षरता की आवश्यकता को लेखक ने क्यों महत्वपूर्ण बताया है? (2 अंक)
प्रश्न 7: लेखक के अनुसार डिजिटल युग में सूचना का दुरुपयोग कैसे समाज को हानि पहुँचा सकता है? (2 अंक)
उत्तर कुंजी:
प्रश्न 1: (ग) सूचना के स्रोत और सत्यता की पहचान करना
प्रश्न 2: (ख) समाज में भ्रम और भय फैलता है
प्रश्न 3: (ख) A सही है, परंतु R गलत है।
प्रश्न 4: (ग) वेबिनार, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से
प्रश्न 5: लेखक के अनुसार सूचना के तीव्र प्रवाह के कारण अनेक बार फर्जी समाचार, अधूरी जानकारियाँ और अफवाहें समाज में भ्रम और भय फैलाती हैं।
प्रश्न 6: मीडिया साक्षरता आवश्यक है क्योंकि इसके माध्यम से लोग यह सीख सकते हैं कि किसी सूचना की सत्यता कैसे जाँची जाए और उसे विवेकपूर्ण ढंग से कैसे उपयोग में लाया जाए।
प्रश्न 7: यदि डिजिटल माध्यम का उपयोग अज्ञानता या पूर्वग्रह के साथ हो, तो यह समाज को भ्रमित करने, आपसी विभाजन बढ़ाने और वैमनस्य फैलाने का कारण बन सकता है।
- भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में राष्ट्रीय एकता की भावना अत्यंत आवश्यक और प्रासंगिक है। विभिन्न धर्मों, भाषाओं, वेशभूषाओं, पर्वों, परंपराओं और जीवन-शैलियों के होते हुए भी यदि भारत एक अखंड राष्ट्र के रूप में स्थापित है तो इसका श्रेय उस सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता को जाता है, जो हमारी आत्मा में गहराई से बसी हुई है। यह एकता केवल किसी राजनीतिक ढांचे या संविधान द्वारा नहीं लाई गई, बल्कि यह भारत के ऐतिहासिक संघर्षों, सांस्कृतिक समन्वय और जनमानस की सोच का परिणाम है। बाहरी आक्रमणों और विदेशी शासनों ने भारत को तोड़ने की कोशिश की, किंतु हर बार भारत की आत्मा ने इन आघातों को सहते हुए अपने मूल स्वरूप को बनाए रखा। स्वतंत्रता संग्राम इस एकता का प्रमाण है, जहाँ भिन्न-भिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और धर्मों के लोग एक उद्देश्य के लिए संगठित हुए थे। आज जब सामाजिक मीडिया, राजनीतिक ध्रुवीकरण और आर्थिक विषमता जैसे कारक समाज में अलगाव और टकराव को जन्म दे रहे हैं, तब यह आवश्यक हो गया है कि राष्ट्रीय एकता की भावना को सशक्त किया जाए। एकता का अर्थ विविधता की समाप्ति नहीं, बल्कि विविधता में सामंजस्य है। यही भारत की असली विशेषता है—‘एकता में अनेकता’। यह कार्य केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने व्यवहार, विचार और क्रियाओं में एकता और सहयोग का प्रदर्शन करे। विद्यालयों, महाविद्यालयों और सांस्कृतिक मंचों पर अंतर-राज्यीय मेलों, भाषायी आदान-प्रदान और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देना इस भावना को मजबूत कर सकता है। जब हम विविधताओं को विरोध नहीं, बल्कि समृद्धि के रूप में देखने लगेंगे, तब भारत की आंतरिक एकता और अधिक दृढ़ होगी। वैश्विक पटल पर सशक्त राष्ट्र बनने के लिए भारत को सबसे पहले अपने भीतर स्थिरता और समरसता को कायम रखना होगा।
प्रश्नपत्र:
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक प्रत्येक):
प्रश्न 1: लेखक के अनुसार भारत की एकता किस पर आधारित है? (1 अंक)
(क) केवल संविधान पर
(ख) समान धर्म और भाषा पर
(ग) सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक मूल्यों पर
(घ) आर्थिक समानता पर
प्रश्न 2: लेखक के अनुसार विविधता में एकता का क्या अर्थ है? (1 अंक)
(क) विविधता को समाप्त करना
(ख) केवल एक धर्म का पालन करना
(ग) विविधताओं के मध्य समरसता बनाए रखना
(घ) सांस्कृतिक पहचान को छोड़ना
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): आज के समय में भारत को राष्ट्रीय एकता की पहले से अधिक आवश्यकता है।
Reason (R): क्योंकि समाज में राजनीतिक विचारधारा और आर्थिक असमानता जैसे कारक विभाजन को जन्म दे रहे हैं।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: लेखक ने किन प्रयासों को राष्ट्रीय एकता की दिशा में सहायक बताया है? (1 अंक)
(क) केवल सैन्य शक्ति को बढ़ाना
(ख) सभी को एक ही भाषा सिखाना
(ग) सांस्कृतिक आयोजनों और अंतर-राज्यीय आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देना
(घ) अलग-अलग समुदायों को अलग क्षेत्रों में बसाना
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: लेखक के अनुसार भारत की सांस्कृतिक एकता किस प्रकार बनी रही, जबकि उस पर बार-बार बाहरी आक्रमण हुए? (2 अंक)
प्रश्न 6: ‘एकता में अनेकता’ की भावना को समाज में सशक्त करने के लिए लेखक ने क्या सुझाव दिए हैं? (2 अंक)
प्रश्न 7: लेखक के अनुसार राष्ट्रीय एकता केवल शासन की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? (2 अंक)
उत्तर कुंजी:
प्रश्न 1: (ग) सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक मूल्यों पर
प्रश्न 2: (ग) विविधताओं के मध्य समरसता बनाए रखना
प्रश्न 3: (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
प्रश्न 4: (ग) सांस्कृतिक आयोजनों और अंतर-राज्यीय आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देना
प्रश्न 5: भारत की सांस्कृतिक एकता इसलिए बनी रही क्योंकि उसने विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों को आत्मसात किया और अपनी मौलिक पहचान को जीवित रखा।
प्रश्न 6: लेखक ने सुझाव दिया है कि विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और मंचों पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान, भाषायी मेल और ऐतिहासिक समझ को प्रोत्साहित किया जाए।
प्रश्न 7: राष्ट्रीय एकता केवल शासन की जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि नागरिकों के व्यवहार, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी से ही इसका स्थायित्व संभव है।
- भारत में जल की महत्ता केवल एक भौतिक संसाधन के रूप में नहीं देखी जाती, बल्कि यह सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय परंपरा में नदियों को मातृस्वरूपा माना गया है—गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी जैसी नदियाँ केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि जनमानस की आस्था की धारा भी हैं। किंतु वर्तमान समय में यही जीवनदायिनी नदियाँ प्रदूषण का बोझ झेल रही हैं। नगरों का गंदा पानी, कारखानों का रासायनिक कचरा और प्लास्टिक अपशिष्ट अनियंत्रित रूप से इन जलधाराओं में प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे न केवल जल की गुणवत्ता घट रही है, बल्कि जल-जीवों का जीवन और जल पर आश्रित मनुष्यों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। भारत में जल संकट केवल प्रदूषण तक सीमित नहीं है। वर्षा का वितरण असमान है—कुछ क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त होते हैं तो कुछ सूखे से। मानसूनी वर्षा का अधिकांश जल बिना संचय के समुद्र में बह जाता है। वनों की कटाई, शहरीकरण, जल स्रोतों की उपेक्षा और भूजल के अति दोहन ने इस संकट को और भी गंभीर बना दिया है। सरकार ने ‘जल शक्ति अभियान’, ‘नमामि गंगे’, ‘अटल भूजल योजना’ जैसी परियोजनाओं के माध्यम से समाधान का प्रयास किया है, परंतु केवल सरकारी प्रयासों से परिवर्तन संभव नहीं। जब तक प्रत्येक नागरिक में जल के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भाव नहीं होगा, तब तक यह संकट बना रहेगा। हमें वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन देना होगा, पारंपरिक जल संरचनाओं का पुनरुद्धार करना होगा और जल का विवेकपूर्ण उपयोग सीखना होगा। जल संकट केवल वर्तमान नहीं, अपितु भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक गंभीर खतरा है। यदि हमने अभी कदम नहीं उठाए, तो भविष्य में जीवन का अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है।
प्रश्नपत्र:
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक प्रत्येक):
प्रश्न 1: लेखक के अनुसार भारत में नदियाँ केवल जल स्रोत नहीं हैं, बल्कि— (1 अंक)
(क) खेती का साधन हैं
(ख) आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आस्था की प्रतीक हैं
(ग) बिजली उत्पादन का स्रोत हैं
(घ) पर्यटन स्थल हैं
प्रश्न 2: लेखक के अनुसार वर्षा जल का एक बड़ा भाग क्यों व्यर्थ चला जाता है? (1 अंक)
(क) वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है
(ख) जल स्रोतों की कमी होती है
(ग) जल संचयन की व्यवस्था नहीं होती
(घ) नदियाँ सूख जाती हैं
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): भारत में जल संकट का एक कारण शहरीकरण और भूजल का अति दोहन है।
Reason (R): क्योंकि शहरीकरण जल संचयन को बढ़ावा देता है।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: लेखक के अनुसार जल संकट से निपटने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? (1 अंक)
(क) बड़े बाँधों का निर्माण
(ख) जल पर कर लगाना
(ग) जनभागीदारी और जल के प्रति जिम्मेदारी
(घ) जल का निजीकरण
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: लेखक के अनुसार नदियाँ किस प्रकार भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई हैं? (2 अंक)
प्रश्न 6: जल प्रदूषण के मुख्य कारणों को लेखक ने किस प्रकार वर्णित किया है? (2 अंक)
प्रश्न 7: लेखक के अनुसार जल संकट के समाधान के लिए क्या-क्या उपाय आवश्यक हैं? (2 अंक)
उत्तर कुंजी:
प्रश्न 1: (ख) आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आस्था की प्रतीक हैं
प्रश्न 2: (ग) जल संचयन की व्यवस्था नहीं होती
प्रश्न 3: (ख) A सही है, परंतु R गलत है।
प्रश्न 4: (ग) जनभागीदारी और जल के प्रति जिम्मेदारी
प्रश्न 5: लेखक के अनुसार भारतीय परंपरा में नदियों को मातृस्वरूपा माना गया है और वे केवल जल की स्रोत नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आस्था की प्रतीक हैं।
प्रश्न 6: लेखक के अनुसार नदियों में नगरों का सीवेज, औद्योगिक रसायन, प्लास्टिक और अपशिष्ट जल का अनियंत्रित बहाव जल प्रदूषण के मुख्य कारण हैं।
प्रश्न 7: जल संकट से निपटने के लिए लेखक ने वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्स्थापन, जल की मितव्ययता से खपत और जनभागीदारी जैसे उपाय आवश्यक बताए हैं।
- भारतीय लोककला भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का जीवंत प्रमाण है। यह कला उन समुदायों की देन है जिन्होंने औपचारिक शिक्षा से दूर रहकर भी अपनी जीवनशैली, आस्था, अनुभवों और पर्यावरणीय संबंधों को रंगों व आकृतियों में ढाला। चाहे वह मध्य प्रदेश की भील चित्रकला हो या राजस्थान की फड़ पेंटिंग, बंगाल का पटचित्र हो या बिहार की मधुबनी — प्रत्येक कला शैली अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है और उस क्षेत्र के लोगों की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन गई है। लोककलाएँ मुख्यतः मौखिक परंपरा और पारिवारिक प्रशिक्षण द्वारा पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्थानांतरित होती रही हैं। इन चित्रकलाओं में प्रयुक्त रंग पूर्णतः प्राकृतिक होते हैं — जैसे फूलों से प्राप्त पीला रंग, पत्तियों से निकाला गया हरा, कोयले से बना काला, और मिट्टी से तैयार लाल। चित्रों में देवी-देवताओं, लोकपर्वों, ग्रामीण जीवन, पशुपालन, कृषि और प्रकृति के विविध रूपों को दर्शाया जाता है। इन कलाओं की सहजता, प्रतीकात्मकता और रंग संयोजन उन्हें विशेष बनाते हैं। आज तकनीक और डिजिटलीकरण ने लोककलाओं को नया मंच दिया है — ऑनलाइन प्रदर्शनियाँ, ई-कॉमर्स मंचों पर बिक्री और डिज़िटल संग्रहालयों ने इनकी पहुँच वैश्विक स्तर पर बढ़ाई है। किंतु इन सबके बावजूद लोककलाओं का भविष्य संकटग्रस्त है। पारंपरिक कलाकारों की नई पीढ़ी इस क्षेत्र में रुचि नहीं ले रही क्योंकि इसे आर्थिक रूप से स्थायी विकल्प नहीं माना जाता। अनेक लोककलाएँ लुप्त होने की स्थिति में पहुँच चुकी हैं। सरकार व गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संरक्षण हेतु योजनाएँ बनाई गई हैं — जैसे कलाकारों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, और विद्यालयी पाठ्यक्रम में लोककला की शिक्षा। किंतु जब तक समाज स्वयं इन कलाओं को अपनाकर इन्हें जीवित नहीं रखता, तब तक संरक्षण के ये प्रयास एकांगी रहेंगे। लोककला केवल चित्र नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि है जिसे पहचानने और सहेजने की आवश्यकता है।
प्रश्नपत्र:
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक प्रत्येक):
प्रश्न 1: लोककलाएँ मुख्यतः किस माध्यम से अगली पीढ़ियों तक पहुँची हैं? (1 अंक)
(क) संस्थागत पाठ्यक्रम के द्वारा
(ख) ऑनलाइन पाठ्यक्रम द्वारा
(ग) मौखिक परंपरा और पारिवारिक प्रशिक्षण द्वारा
(घ) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा
प्रश्न 2: लेखक के अनुसार लोककलाओं में प्रयुक्त रंग— (1 अंक)
(क) रासायनिक होते हैं
(ख) यांत्रिक तकनीक से बनाए जाते हैं
(ग) प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं
(घ) आधुनिक स्याही से तैयार होते हैं
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): आधुनिक समय में तकनीक और डिजिटलीकरण ने लोककलाओं को समाप्त कर दिया है।
Reason (R): क्योंकि अब लोग केवल डिजिटल कला में रुचि लेते हैं।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: लेखक के अनुसार लोककलाओं के संरक्षण का सबसे बड़ा आधार क्या है? (1 अंक)
(क) केवल सरकारी योजनाएँ
(ख) अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ
(ग) स्कूली प्रतियोगिताएँ
(घ) समाज द्वारा इन्हें महत्व देना
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: लेखक ने किन-किन लोककला शैलियों का उल्लेख किया है, और वे किस प्रकार सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हैं? (2 अंक)
प्रश्न 6: लोककलाओं के भविष्य को लेकर लेखक की क्या चिंता है? (2 अंक)
प्रश्न 7: लेखक के अनुसार लोककलाओं को संरक्षण देने हेतु किन प्रयासों का उल्लेख किया गया है? (2 अंक)
उत्तर कुंजी:
प्रश्न 1: (ग) मौखिक परंपरा और पारिवारिक प्रशिक्षण द्वारा
प्रश्न 2: (ग) प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं
प्रश्न 3: (घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: (घ) समाज द्वारा इन्हें महत्व देना
प्रश्न 5: लेखक ने भील चित्रकला, फड़ पेंटिंग, पटचित्र और मधुबनी जैसे लोककला शैलियों का उल्लेख किया है। ये कलाएँ क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान की प्रतीक हैं और वहाँ की जनसंस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं।
प्रश्न 6: लेखक की चिंता यह है कि पारंपरिक कलाकारों की नई पीढ़ी इस क्षेत्र में नहीं आ रही क्योंकि यह आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं माना जाता, जिससे कई लोककलाएँ लुप्त होने के कगार पर हैं।
प्रश्न 7: लोककलाओं के संरक्षण हेतु सरकार और गैर-सरकारी संस्थाएँ कलाकारों को प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, और स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने जैसे प्रयास कर रही हैं, लेकिन समाज की स्वैच्छिक सहभागिता आवश्यक है।
- भारतीय लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में गिना जाता है, जिसकी नींव जन-भागीदारी और उत्तरदायित्व पर आधारित है। परंतु लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें नागरिकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। जब तक आम नागरिक अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप साकार नहीं हो सकता। भारत में अनेक नागरिक केवल मतदान को ही लोकतांत्रिक सहभागिता मानते हैं, जबकि वास्तविक लोकतंत्र का मतलब है कि लोग शासन की प्रक्रिया में सतत भाग लें, नीति निर्माण पर प्रश्न उठाएँ, निर्णयों की समीक्षा करें और अपने विचार व्यक्त करें। एक जागरूक नागरिक सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की मांग करता है। परंतु अफसोस की बात यह है कि आज भी बहुत से लोग सरकारी नीतियों और योजनाओं की आलोचना तो करते हैं, परन्तु स्वयं उसमें सक्रिय भागीदारी नहीं निभाते। लोकतांत्रिक मूल्य तभी पनप सकते हैं जब शिक्षा व्यवस्था में नागरिक शास्त्र और नैतिक मूल्यों को उचित स्थान मिले। विद्यालय और महाविद्यालय केवल अंक या डिग्री देने के स्थान नहीं होने चाहिए, बल्कि वे चरित्र निर्माण और सामाजिक चेतना के केंद्र बनने चाहिएँ। छात्रों में तर्कशीलता, सहिष्णुता और संवाद कौशल विकसित करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए ताकि वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। इसके अतिरिक्त मीडिया और जनसंचार के साधनों की भी भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। उन्हें केवल सनसनी फैलाने की बजाय जनता को सूचित, शिक्षित और जागरूक करने का दायित्व निभाना चाहिए। जब हर स्तर पर नागरिक चेतना जागृत होगी, तभी लोकतंत्र सशक्त और सार्थक बन सकेगा।
प्रश्नपत्र:
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक प्रत्येक):
प्रश्न 1: लेखक के अनुसार लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप कब साकार हो सकता है? (1 अंक)
(क) जब चुनाव निष्पक्ष हों
(ख) जब सरकार जवाबदेह हो
(ग) जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक हों
(घ) जब न्यायपालिका स्वतंत्र हो
प्रश्न 2: विद्यालय और महाविद्यालय किस प्रकार की भूमिका निभाने चाहिएँ? (1 अंक)
(क) प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी केंद्र
(ख) केवल डिग्री प्रदान करने के स्थान
(ग) रोजगार प्राप्ति के साधन
(घ) चरित्र निर्माण और सामाजिक चेतना के केंद्र
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): लोकतंत्र में केवल मतदान करना ही पर्याप्त है।
Reason (R): क्योंकि यही नागरिकों की मुख्य जिम्मेदारी है।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: लेखक के अनुसार मीडिया को किस भूमिका का निर्वहन करना चाहिए? (1 अंक)
(क) केवल मनोरंजन प्रदान करना
(ख) राजनीतिक दलों का समर्थन करना
(ग) जनता को सूचित, शिक्षित और जागरूक करना
(घ) सामाजिक माध्यमों पर सक्रिय रहना
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: लेखक ने लोकतंत्र की सतत प्रक्रिया में नागरिक की क्या भूमिका बताई है? (2 अंक)
प्रश्न 6: लेखक के अनुसार एक जागरूक नागरिक की विशेषताएँ क्या होनी चाहिएँ? (2 अंक)
प्रश्न 7: लोकतंत्र को सशक्त बनाने में शिक्षा व्यवस्था की भूमिका क्या हो सकती है? (2 अंक)
उत्तर कुंजी:
प्रश्न 1: (ग) जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक हों
प्रश्न 2: (घ) चरित्र निर्माण और सामाजिक चेतना के केंद्र
प्रश्न 3: (घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: (ग) जनता को सूचित, शिक्षित और जागरूक करना
प्रश्न 5: लेखक के अनुसार लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों को शासन प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, नीतियों पर प्रश्न उठाने चाहिए और निर्णयों की समीक्षा करनी चाहिए।
प्रश्न 6: एक जागरूक नागरिक सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की माँग करता है, स्वयं निर्णय प्रक्रिया में भाग लेता है और केवल आलोचना तक सीमित नहीं रहता।
प्रश्न 7: शिक्षा व्यवस्था यदि नागरिक शास्त्र और नैतिक मूल्यों को महत्व दे तो वह लोकतंत्र को सशक्त कर सकती है। विद्यालयों को सामाजिक चेतना और संवाद-कौशल का केंद्र बनना चाहिए।
- भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण का विशेष स्थान रहा है। वैदिक काल से ही प्रकृति को देवी-देवताओं के रूप में पूजा गया है—पृथ्वी को ‘भूमि देवी’, नदियों को ‘गंगा माँ’, वृक्षों को ‘वृक्ष देवता’, और वायु को ‘वायु देव’ की संज्ञा दी गई है। यह भाव न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक था, बल्कि उसमें वैज्ञानिक चेतना भी निहित थी। परंतु जैसे-जैसे आधुनिकता बढ़ती गई, वैसे-वैसे यह भावनात्मक संबंध टूटता गया और प्रकृति का दोहन बढ़ता चला गया। आज जब हम जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों के पिघलने, जैव विविधता के क्षय और प्रदूषण की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब हमें अपने पूर्वजों की उन परंपराओं की ओर लौटने की आवश्यकता है, जिनमें प्रकृति के साथ सहअस्तित्व की भावना थी। लेकिन यह केवल सांस्कृतिक लौटाव से नहीं होगा; इसके लिए आधुनिक विज्ञान और तकनीक के सहयोग से एक संतुलित विकास नीति अपनानी होगी, जिसमें पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक प्रगति साथ-साथ चलें। विकास के नाम पर अंधाधुंध औद्योगीकरण, शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों की बेतरतीब खपत ने मानवीय जीवन के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अब आवश्यकता है एक ऐसी शिक्षा की जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाकर प्रत्येक व्यक्ति को उसके संरक्षण की दिशा में प्रेरित करे। इसके लिए विद्यालयों में ‘पर्यावरण शिक्षा’ को केवल एक विषय की तरह नहीं, बल्कि जीवन पद्धति के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। विकास का मतलब केवल ऊँची इमारतें, चौड़ी सड़कें या विदेशी निवेश नहीं है, बल्कि वह प्रक्रिया है जो वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और उपयोगी हो। अतः जनसाधारण को भी यह समझने की आवश्यकता है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से ही यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
प्रश्नपत्र:
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक प्रत्येक):
प्रश्न 1: वैदिक काल में पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण कैसा था? (1 अंक)
(क) केवल धार्मिक
(ख) केवल वैज्ञानिक
(ग) धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों
(घ) केवल सांस्कृतिक
प्रश्न 2: लेखक के अनुसार शिक्षा में किस बात पर विशेष बल दिया जाना चाहिए? (1 अंक)
(क) तकनीकी कौशल
(ख) विदेशी निवेश
(ग) पर्यावरण संरक्षण को जीवन पद्धति के रूप में पढ़ाना
(घ) प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): पर्यावरणीय संकटों का हल केवल परंपराओं में लौटने से संभव है।
Reason (R): क्योंकि परंपराएँ आधुनिक विज्ञान से अधिक प्रभावी हैं।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: लेखक के अनुसार विकास की सच्ची परिभाषा क्या है? (1 अंक)
(क) ऊँची इमारतों और चौड़ी सड़कों का निर्माण
(ख) केवल आर्थिक वृद्धि
(ग) वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रखने वाली प्रक्रिया
(घ) विदेशी निवेश को आकर्षित करना
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: लेखक ने आधुनिकता के बढ़ने के साथ किस प्रकार के परिवर्तन का उल्लेख किया है? (2 अंक)
प्रश्न 6: पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव आवश्यक बताए गए हैं? (2 अंक)
प्रश्न 7: लेखक ने आम नागरिकों की किस जिम्मेदारी पर बल दिया है? (2 अंक)
उत्तर कुंजी:
प्रश्न 1: (ग) धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों
प्रश्न 2: (ग) पर्यावरण संरक्षण को जीवन पद्धति के रूप में पढ़ाना
प्रश्न 3: (ख) A सही है, परंतु R गलत है।
प्रश्न 4: (ग) वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रखने वाली प्रक्रिया
प्रश्न 5: लेखक के अनुसार आधुनिकता के बढ़ने के साथ प्रकृति से भावनात्मक संबंध टूटते गए और इसका दोहन बढ़ गया, जिससे पर्यावरण संकट उत्पन्न हुआ।
प्रश्न 6: शिक्षा प्रणाली में ‘पर्यावरण शिक्षा’ को केवल विषय के रूप में नहीं, बल्कि जीवन शैली के रूप में अपनाने की आवश्यकता है ताकि छात्र संवेदनशील और जिम्मेदार बनें।
प्रश्न 7: लेखक ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है।
- भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की लगभग 60% जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। कृषि केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक संरचना का अभिन्न अंग रही है। किसान का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है – कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि, कभी फसल का उचित मूल्य न मिलना – इन सभी समस्याओं के बीच भी वह अन्नदाता बना रहता है। आधुनिक समय में कृषि क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए हैं। हरित क्रांति, उन्नत बीज, सिंचाई की आधुनिक विधियाँ और यंत्रीकरण ने उत्पादकता में वृद्धि की है। लेकिन इसके बावजूद भी छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति उतनी नहीं सुधरी है जितनी अपेक्षित थी। किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती कर्ज का बोझ है। कई बार कर्ज लेकर बीज और उर्वरक खरीदे जाते हैं, परंतु यदि मौसम प्रतिकूल हो जाए या बाजार मूल्य घट जाए, तो किसान कर्ज चुकाने में असफल हो जाता है। सरकार ने किसानों की सहायता के लिए अनेक योजनाएँ चलाई हैं – जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना आदि। इन योजनाओं से कुछ राहत मिली है, परंतु जमीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन अभी भी चुनौतीपूर्ण है। किसान आज भी साहूकारों के चंगुल में फँसे हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रख पाते। आज आवश्यकता है कि किसानों को केवल आर्थिक नहीं, बल्कि तकनीकी, शैक्षणिक और बाजार संबंधी सहायता भी दी जाए। कृषि को केवल पारंपरिक नहीं, बल्कि आधुनिक उद्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। जब तक किसानों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जाएगा, तब तक भारत की समृद्धि अधूरी ही रहेगी।
प्रश्नपत्र:
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक प्रत्येक):
प्रश्न 1: भारत की लगभग कितनी जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है? (1 अंक)
(क) 40%
(ख) 50%
(ग) 60%
(घ) 70%
प्रश्न 2: किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या बताई गई है? (1 अंक)
(क) सिंचाई का अभाव
(ख) कर्ज का बोझ
(ग) तकनीकी जानकारी की कमी
(घ) खाद की अनुपलब्धता
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): आधुनिक तकनीकों ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाया है।
Reason (R): हरित क्रांति और यंत्रीकरण के कारण कृषि पिछड़ गई है।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: लेखक के अनुसार किसानों की आत्मनिर्भरता से क्या लाभ होगा? (1 अंक)
(क) कृषि समाप्त हो जाएगी
(ख) सरकार की सहायता की आवश्यकता नहीं रहेगी
(ग) भारत की समृद्धि संभव होगी
(घ) किसान केवल परंपरागत खेती करेगा
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: लेखक ने किसानों के जीवन को कठिन क्यों बताया है? (2 अंक)
प्रश्न 6: किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई गई हैं और उनका प्रभाव कैसा रहा है? (2 अंक)
प्रश्न 7: लेखक के अनुसार कृषि को किस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और क्यों? (2 अंक)
उत्तर कुंजी:
प्रश्न 1: (ग) 60%
प्रश्न 2: (ख) कर्ज का बोझ
प्रश्न 3: (ख) A सही है, परंतु R गलत है।
प्रश्न 4: (ग) भारत की समृद्धि संभव होगी
प्रश्न 5: लेखक ने बताया कि किसान का जीवन सूखा, अतिवृष्टि, फसल के मूल्य में गिरावट जैसी समस्याओं से भरा होता है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी वह देश को अन्न देता है, इसलिए उसका जीवन कठिन माना गया है।
प्रश्न 6: सरकार ने ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’, ‘फसल बीमा योजना’ आदि लागू की हैं। इनसे कुछ किसानों को लाभ मिला है, परंतु जमीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन धीमा और सीमित रहा है।
प्रश्न 7: लेखक के अनुसार कृषि को आधुनिक उद्यम के रूप में देखा जाना चाहिए, ताकि किसान तकनीकी, शैक्षणिक और विपणन सहायता लेकर आत्मनिर्भर बन सके और देश की समृद्धि में योगदान दे सके।
- आज के समय में सामाजिक मीडिया ने लोगों के जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब आदि मंचों के माध्यम से लोग एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं, विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, तथा अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित भी करते हैं। लेकिन जहाँ एक ओर यह प्लेटफॉर्म लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, वहीं दूसरी ओर इसके कई नकारात्मक पहलू भी सामने आए हैं। सबसे पहली चिंता निजता (Privacy) की है। सोशल मीडिया पर डाले गए व्यक्तिगत चित्र, वीडियो या सूचनाएँ कभी-कभी गलत हाथों में पहुँच जाती हैं, जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका गंभीर प्रभाव देखा गया है। निरंतर तुलना की भावना, ‘लाइक्स’ की संख्या से आत्म-मूल्यांकन, ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग जैसे व्यवहार आज आम हो गए हैं। किशोरों और युवाओं में सोशल मीडिया की लत भी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। पढ़ाई, नींद और पारिवारिक समय की कीमत पर घंटों स्क्रीन के सामने बिताना अब सामान्य हो गया है। इसका असर न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है – जैसे आंखों की रोशनी पर प्रभाव, थकान, मोटापा, और तनाव। इसके बावजूद, यदि सोशल मीडिया का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, तो यह एक सशक्त उपकरण सिद्ध हो सकता है। ऑनलाइन शिक्षा, जागरूकता अभियान, आपातकालीन सूचना प्रसारण, व्यवसाय का प्रचार आदि क्षेत्रों में यह बहुत सहायक रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि उपयोगकर्ता डिजिटल साक्षरता को अपनाएँ, गोपनीयता की सुरक्षा करें और अपने समय का संतुलित प्रबंधन करें।
प्रश्नपत्र:
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक प्रत्येक):
प्रश्न 1: सामाजिक मीडिया का सबसे पहला नकारात्मक प्रभाव क्या बताया गया है?
(क) मनोरंजन का अभाव
(ख) समय की बर्बादी
(ग) निजता का संकट
(घ) रोजगार में गिरावट
प्रश्न 2: निम्न में से कौन-सा शारीरिक प्रभाव सोशल मीडिया की लत से संबंधित नहीं है?
(क) थकान
(ख) मोटापा
(ग) तेज़ स्मृति
(घ) आँखों की समस्या
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): सोशल मीडिया आज के समय में युवाओं के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। (1 अंक)
Reason (R): इसके माध्यम से वे ऑनलाइन शिक्षा और व्यवसाय को बढ़ावा दे सकते हैं।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: सोशल मीडिया की विवेकपूर्ण उपयोगिता का एक सकारात्मक उदाहरण क्या हो सकता है?
(क) ट्रोलिंग बढ़ाना
(ख) अनियमित नींद लेना
(ग) ऑनलाइन शिक्षा
(घ) निजता साझा करना
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: सोशल मीडिया के मानसिक प्रभावों पर लेखक ने क्या टिप्पणी की है? (2 अंक)
प्रश्न 6: किशोरों में सोशल मीडिया की लत किस प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न कर रही है? (2 अंक)
प्रश्न 7: लेखक ने डिजिटल साक्षरता के बारे में क्या सुझाव दिया है? (2 अंक)
उत्तर कुंजी:
प्रश्न 1: (ग) निजता का संकट
प्रश्न 2: (ग) तेज़ स्मृति
प्रश्न 3: (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
प्रश्न 4: (ग) ऑनलाइन शिक्षा
प्रश्न 5: लेखक के अनुसार सोशल मीडिया पर तुलना की भावना, ट्रोलिंग, और साइबर बुलिंग जैसी गतिविधियाँ मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, जिससे तनाव और आत्म-मूल्यांकन की समस्या उत्पन्न होती है।
प्रश्न 6: किशोरों में सोशल मीडिया की लत से पढ़ाई में ध्यान की कमी, पारिवारिक समय की उपेक्षा, नींद की कमी और शारीरिक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
प्रश्न 7: लेखक का सुझाव है कि उपयोगकर्ताओं को डिजिटल साक्षरता अपनाकर, अपने डेटा की गोपनीयता सुरक्षित रखनी चाहिए और सोशल मीडिया पर बिताए गए समय का संतुलित प्रबंधन करना चाहिए।
- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भी शुरुआत थी। अंग्रेजों के शोषणकारी शासन के खिलाफ जो चिंगारी फैली, वह देश की आत्मा को झकझोरने वाली थी। 1857 का विद्रोह इसका पहला संगठित रूप था, जिसके बाद देशभर में अनेक क्रांतिकारियों, समाज-सुधारकों और नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए अपने-अपने ढंग से संघर्ष किया। महात्मा गांधी ने जब 1915 में भारत में कदम रखा, तब स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ मिला। उन्होंने ‘सत्याग्रह’ और ‘अहिंसा’ जैसे सिद्धांतों को अपनाकर जनांदोलन को जनसाधारण तक पहुँचा दिया। गाँधीजी के नेतृत्व में हुए असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। इस आंदोलन में केवल पुरुष नहीं, बल्कि महिलाएँ, छात्र, किसान, मजदूर, व्यापारी – सभी वर्गों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली जैसी महिलाएँ स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बन गईं। संघर्ष केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था। समाज के पिछड़े वर्गों को समान अधिकार दिलाने, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार देने, छुआछूत मिटाने जैसी अनेक सामाजिक सुधार की माँगें भी इसमें समाहित थीं। इस संग्राम ने भारतीयों को अपनी पहचान, आत्मगौरव और एकता का अनुभव कराया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब यह केवल एक भौगोलिक स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि यह भारतीय आत्मा की मुक्ति थी। परंतु स्वतंत्रता के साथ ही विभाजन की त्रासदी और उसके परिणाम भी जुड़े, जिसने देश के लिए एक नया संघर्ष आरंभ किया।
प्रश्नपत्र
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक):
प्रश्न 1: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है? (1 अंक)
(क) केवल राजनीतिक आंदोलन
(ख) सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन
(ग) सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण
(घ) औद्योगिक विकास की प्रक्रिया
प्रश्न 2: गाँधीजी के नेतृत्व में किस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी? (1 अंक)
(क) खिलाफत आंदोलन
(ख) नमक सत्याग्रह
(ग) चंपारण आंदोलन
(घ) किसानों का विद्रोह
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): स्वतंत्रता संग्राम केवल पुरुषों तक सीमित था।
Reason (R): महिलाएँ उस समय शिक्षा और राजनीति से दूर रहती थीं।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ किस प्रकार की समस्या ने जन्म लिया? (1 अंक)
(क) आर्थिक मंदी
(ख) औद्योगिक क्रांति
(ग) विभाजन की त्रासदी
(घ) तकनीकी विकास का संकट
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: स्वतंत्रता संग्राम में गाँधीजी द्वारा अपनाए गए दो प्रमुख सिद्धांत कौन-से थे? (2 अंक)
प्रश्न 6: इस गद्यांश के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की क्या भूमिका रही? (2 अंक)
प्रश्न 7: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सामाजिक सुधारों की क्या माँगें उठाई गई थीं? (2 अंक)
उत्तरकुंजी
प्रश्न 1: (ग) सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण
प्रश्न 2: (ख) नमक सत्याग्रह
प्रश्न 3: (घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: (ग) विभाजन की त्रासदी
प्रश्न 5: गाँधीजी ने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया, जिससे जनांदोलन शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावशाली बना।
प्रश्न 6: महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाई। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और अरुणा आसफ अली जैसी महिलाओं ने आंदोलन को प्रेरणा दी।
प्रश्न 7: संग्राम के दौरान स्त्रियों की शिक्षा, छुआछूत का उन्मूलन और पिछड़े वर्गों को समान अधिकार देने जैसी सामाजिक माँगें उठीं।
- जल ही जीवन है – यह कथन केवल एक नारा नहीं, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का मूल आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। मानव शरीर का लगभग 70% भाग जल से बना है, वहीं वनस्पति, जीव-जंतु तथा पर्यावरण की संपूर्ण क्रियाविधियाँ जल पर ही निर्भर करती हैं। किंतु आज जल संकट एक वैश्विक समस्या बन गया है। जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित शहरीकरण, औद्योगिक अपशिष्ट तथा जल संसाधनों का अति दोहन इस संकट के मुख्य कारण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी लोग कई किलोमीटर दूर से जल लाकर अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर तेजी से गिर रहा है। जल का असमान वितरण भी इस संकट को और गंभीर बनाता है। कहीं बाढ़ से त्राहि-त्राहि मच जाती है, तो कहीं सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका मुख्य कारण है – जल संचयन और संरक्षण की उपेक्षा। भारत जैसे देश में, जहाँ मानसून पर कृषि निर्भर है, जल संरक्षण का महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है। यदि वर्षा जल को एकत्र कर पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाए, तो यह संकट काफी हद तक कम हो सकता है। छतों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली, तालाबों और कुंओं का पुनरुद्धार, नदियों की सफाई तथा वृक्षारोपण इसके कुछ कारगर उपाय हैं। सरकार ने ‘जल शक्ति अभियान’, ‘नमामि गंगे’, ‘अमृत योजना’ जैसी कई पहलें की हैं, लेकिन इनका प्रभाव तभी पड़ेगा जब आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझें। जल का विवेकपूर्ण उपयोग, रिसाव को रोकना, और बच्चों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना आवश्यक है। आज आवश्यकता है कि हम जल को केवल संसाधन नहीं, बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह देखें। यदि अभी भी हम सचेत नहीं हुए, तो आने वाली पीढ़ियों को जल के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।
प्रश्नपत्र
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक):
प्रश्न 1: वर्तमान में जल संकट का मुख्य कारण क्या है? (1 अंक)
(क) समुद्र का खारा पानी
(ख) वर्षा की अधिकता
(ग) जल संसाधनों का अति दोहन
(घ) अधिक जनसंख्या का विदेशों में पलायन
प्रश्न 2: ‘नमामि गंगे’ योजना का संबंध किससे है? (1 अंक)
(क) वर्षा जल संचयन से
(ख) जल का पुनर्चक्रण
(ग) नदियों की सफाई से
(घ) कुओं की खुदाई से
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): भारत में जल संकट की एक बड़ी वजह जल संचयन की उपेक्षा है।
Reason (R): वर्षा जल को संरक्षित करना और दोबारा उपयोग करना असंभव है।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: जल संकट से निपटने के लिए निम्न में से कौन-सा उपाय गद्यांश में उल्लिखित नहीं है? (1 अंक)
(क) वृक्षारोपण
(ख) वर्षा जल संचयन
(ग) नदियों की सफाई
(घ) समुद्र जल का खारा करना
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: भारत में जल संकट के प्रमुख कारण कौन-कौन से हैं? (2 अंक)
प्रश्न 6: वर्षा जल संचयन के कौन-कौन से उपाय इस गद्यांश में बताए गए हैं? (2 अंक)
प्रश्न 7: आम नागरिक जल संरक्षण में कैसे भाग ले सकते हैं? (2 अंक)
उत्तरकुंजी
प्रश्न 1: (ग) जल संसाधनों का अति दोहन
प्रश्न 2: (ग) नदियों की सफाई से
प्रश्न 3: (ख) A सही है, परंतु R गलत है।
प्रश्न 4: (घ) समुद्र जल का खारा करना
प्रश्न 5: जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित शहरीकरण, औद्योगिक अपशिष्ट और जल संसाधनों का अति दोहन भारत में जल संकट के प्रमुख कारण हैं।
प्रश्न 6: वर्षा जल को छतों पर संग्रहित करना, तालाबों और कुंओं का पुनरुद्धार करना, तथा नदियों की सफाई करना वर्षा जल संचयन के कुछ उपाय हैं।
प्रश्न 7: नागरिक जल का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं, रिसाव को रोक सकते हैं, बच्चों को जागरूक बना सकते हैं और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने में योगदान दे सकते हैं।
- भारतीय समाज में परिवार एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण संस्था रही है। पारंपरिक संयुक्त परिवार व्यवस्था ने न केवल सामाजिक सुरक्षा प्रदान की, बल्कि नैतिक मूल्यों, सांस्कृतिक परंपराओं और सहयोग की भावना को भी बनाए रखा। एक ही छत के नीचे तीन-चार पीढ़ियों का साथ रहना, बुज़ुर्गों का मार्गदर्शन और बच्चों का सामूहिक लालन-पालन – ये सभी बातें भारतीय परिवार की विशेषताएँ रही हैं। लेकिन बदलते समय और आधुनिक जीवनशैली के कारण अब परिवार की संरचना में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। अब एकल परिवार (nuclear family) का प्रचलन बढ़ गया है, जहाँ माता-पिता और बच्चे ही रहते हैं। इसके कई कारण हैं – जैसे नौकरी के लिए स्थानांतरण, निजी स्वतंत्रता की चाह, शहरीकरण और जीवन की तेज़ गति। एकल परिवार जहाँ निजी निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है, वहीं इसमें सामाजिक सहयोग, भावनात्मक सुरक्षा और बुज़ुर्गों से ज्ञान का आदान-प्रदान कम हो जाता है। आजकल वृद्धजन अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, वहीं युवा तनाव, अवसाद और अव्यवस्थित जीवन शैली से जूझ रहे हैं। यह आवश्यक है कि हम आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखें। एकल परिवार हों या संयुक्त, उनमें परस्पर सम्मान, संवाद और जिम्मेदारी का भाव बना रहना चाहिए। परिवार केवल खून का संबंध नहीं, बल्कि एक भावनात्मक बंधन है, जिसे विश्वास और सहयोग से सींचा जाता है।
प्रश्नपत्र
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक):
प्रश्न 1: पारंपरिक संयुक्त परिवार की कौन-सी विशेषता नहीं है? (1 अंक)
(क) सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा
(ख) व्यक्तिगत स्वतंत्रता
(ग) सामाजिक सुरक्षा
(घ) सहयोग की भावना
प्रश्न 2: एकल परिवार का कौन-सा लाभ गद्यांश में बताया गया है? (1 अंक)
(क) सभी सदस्यों की स्थायी आमदनी
(ख) स्वतंत्र निर्णय लेने की सुविधा
(ग) जीवनशैली में अनुशासन
(घ) पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): वृद्धजन आज अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं।
Reason (R): एकल परिवारों में बुज़ुर्गों की उपस्थिति अधिक हो गई है।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: निम्न में से किस तत्व को परिवार का आधार नहीं माना गया है? (1 अंक)
(क) संवाद
(ख) विश्वास
(ग) संपत्ति
(घ) सहयोग
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: आजकल एकल परिवारों का प्रचलन किन कारणों से बढ़ा है? (2 अंक)
प्रश्न 6: गद्यांश के अनुसार पारंपरिक संयुक्त परिवार समाज को क्या लाभ प्रदान करते थे? (2 अंक)
प्रश्न 7: एक आदर्श परिवार के लिए किन मूल्यों को बनाए रखना आवश्यक है? (2 अंक)
उत्तरकुंजी
प्रश्न 1: (ख) व्यक्तिगत स्वतंत्रता
प्रश्न 2: (ख) स्वतंत्र निर्णय लेने की सुविधा
प्रश्न 3: (ख) A सही है, परंतु R गलत है।
प्रश्न 4: (ग) संपत्ति
प्रश्न 5: नौकरी में स्थानांतरण, निजी स्वतंत्रता की चाह, शहरीकरण और तेज जीवन शैली के कारण एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ा है।
प्रश्न 6: संयुक्त परिवार सामाजिक सुरक्षा, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक परंपराएँ और सहयोग की भावना प्रदान करते थे।
प्रश्न 7: परस्पर सम्मान, संवाद, और पारिवारिक जिम्मेदारी जैसे मूल्य आदर्श परिवार के लिए आवश्यक हैं।
- आज की दुनिया में तकनीकी विकास की गति अत्यंत तीव्र हो गई है। कंप्यूटर, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में हो रहे नवाचारों ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, कृषि और मनोरंजन – हर जगह तकनीकी हस्तक्षेप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस प्रगति के सकारात्मक पहलू अनेक हैं – सूचना तक शीघ्र पहुँच, दूर-दराज़ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ, ऑनलाइन शिक्षा, समय की बचत, और उत्पादन में तेजी। लेकिन तकनीक के अंधाधुंध प्रयोग ने कई नई चुनौतियाँ भी खड़ी कर दी हैं। सबसे पहली चिंता है – बेरोजगारी की। मशीनें और ऑटोमेशन मानव श्रमिकों की जगह ले रहे हैं, जिससे परंपरागत नौकरियाँ घट रही हैं। दूसरी चिंता है – डिजिटल असमानता। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में अभी भी पर्याप्त तकनीकी संसाधनों की कमी है, जिससे वहाँ के लोग मुख्यधारा से पीछे छूट रहे हैं। साथ ही, साइबर अपराध, डेटा चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं। इन सबके बावजूद, तकनीक को रोका नहीं जा सकता। इसका उत्तरदायी और नैतिक उपयोग ही एकमात्र उपाय है। हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी होगी जो छात्रों को केवल डिग्री नहीं, बल्कि कौशल, नवाचार और समस्या-समाधान की क्षमता प्रदान करें। इसके साथ-साथ डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा को भी महत्व देना आवश्यक है।
प्रश्नपत्र
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक):
प्रश्न 1: तकनीकी प्रगति के किस क्षेत्र का उल्लेख गद्यांश में नहीं किया गया है? (1 अंक)
(क) कृषि
(ख) स्वास्थ्य
(ग) पर्यटन
(घ) संचार
प्रश्न 2: डिजिटल असमानता का प्रमुख कारण क्या बताया गया है? (1 अंक)
(क) बेरोजगारी
(ख) संसाधनों की असमान उपलब्धता
(ग) शिक्षा की कमी
(घ) डेटा चोरी
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): तकनीक के बढ़ते प्रयोग से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है।
Reason (R): मशीनें और ऑटोमेशन कई परंपरागत नौकरियों का स्थान ले रही हैं।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: गद्यांश के अनुसार, तकनीकी चुनौतियों से निपटने का सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? (1 अंक)
(क) तकनीक का त्याग
(ख) शिक्षा प्रणाली में सुधार
(ग) मशीनों का बहिष्कार
(घ) केवल शहरी क्षेत्रों में विकास
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: तकनीकी विकास ने मानव जीवन के किन क्षेत्रों को प्रभावित किया है और इसके क्या लाभ हैं? (2 अंक)
प्रश्न 6: गद्यांश के अनुसार, तकनीक से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ कौन-कौन सी हैं और उनका समाधान क्या बताया गया है? (2 अंक)
प्रश्न 7: शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन आवश्यक हैं ताकि तकनीकी युग की चुनौतियों का सामना किया जा सके? (2 अंक)
उत्तरकुंजी
प्रश्न 1: (ग) पर्यटन
प्रश्न 2: (ख) संसाधनों की असमान उपलब्धता
प्रश्न 3: (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
प्रश्न 4: (ख) शिक्षा प्रणाली में सुधार
प्रश्न 5: तकनीकी विकास ने शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन, कृषि और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इससे सूचना की शीघ्र प्राप्ति, समय की बचत, उत्पादन में वृद्धि और दूरदराज़ क्षेत्रों तक सेवाओं की पहुँच संभव हुई है।
प्रश्न 6: बेरोजगारी, डिजिटल असमानता और साइबर अपराध प्रमुख चुनौतियाँ हैं। समाधान के रूप में तकनीक का नैतिक उपयोग, डिजिटल साक्षरता और सुरक्षित उपयोग का सुझाव दिया गया है।
प्रश्न 7: शिक्षा प्रणाली में केवल डिग्री नहीं, बल्कि नवाचार, कौशल और समस्या-समाधान क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। साथ ही, डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा को भी शिक्षा का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
- भारतीय ग्रामीण जीवन देश की आत्मा का प्रतीक है। भारत की एक बड़ी जनसंख्या गाँवों में निवास करती है और उनकी आजीविका मुख्यतः कृषि पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्र जहाँ एक ओर परंपराओं, संस्कृति और सामूहिकता को संजोए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और मूलभूत सुविधाओं की कमी से भी जूझ रहे हैं। गाँवों में जीवन सरल जरूर है, लेकिन वहाँ सुविधाओं का अभाव जीवन को कठिन बना देता है। आज भी बहुत-से गाँवों में पक्की सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पीने का स्वच्छ जल और बिजली जैसी बुनियादी चीजें पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं। इसके कारण ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हो रही है। सरकार द्वारा कई योजनाएँ – जैसे ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’, ‘स्वच्छ भारत मिशन’, ‘संपूर्ण शिक्षा अभियान’ आदि चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारना है। परंतु इन योजनाओं का प्रभाव तभी पड़ता है जब उन्हें जमीनी स्तर पर ईमानदारी से लागू किया जाए और लोगों को इनके प्रति जागरूक किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे बड़ी शक्ति उनका सामाजिक ताना-बाना है, जहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक-दूसरे की मदद करते हैं और सामूहिक निर्णय लेते हैं। यदि इस सामाजिक एकता को सशक्त बनाया जाए और युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, तो ग्रामीण भारत भी आत्मनिर्भर बन सकता है।
प्रश्नपत्र
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक):
प्रश्न 1: ग्रामीण जनसंख्या मुख्यतः किस पर निर्भर है? (1 अंक)
(क) उद्योग पर
(ख) कृषि पर
(ग) व्यापार पर
(घ) पर्यटन पर
प्रश्न 2: ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन का प्रमुख कारण क्या है? (1 अंक)
(क) सांस्कृतिक विविधता
(ख) मौसम परिवर्तन
(ग) सुविधाओं की कमी
(घ) अधिक जनसंख्या
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी शक्ति उनका सामाजिक ताना-बाना है।
Reason (R): ग्रामीण लोग एक-दूसरे से अलग-थलग रहना पसंद करते हैं।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ का उद्देश्य क्या है? (1 अंक)
(क) शहरीकरण को बढ़ावा देना
(ख) किसानों को रोजगार देना
(ग) गाँवों को सड़कों से जोड़ना
(घ) जल-प्रदूषण रोकना
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: ग्रामीण जीवन की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं, और उनका नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? (2 अंक)
प्रश्न 6: सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु शुरू की गई योजनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। (2 अंक)
प्रश्न 7: ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किन उपायों को अपनाया जाना चाहिए? (2 अंक)
उत्तरकुंजी
प्रश्न 1: (ख) कृषि पर
प्रश्न 2: (ग) सुविधाओं की कमी
प्रश्न 3: (ख) A सही है, परंतु R गलत है।
प्रश्न 4: (ग) गाँवों को सड़कों से जोड़ना
प्रश्न 5: ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव प्रमुख समस्याएँ हैं। इनका नागरिकों पर प्रभाव यह होता है कि वे पलायन करते हैं, शिक्षा से वंचित रहते हैं और उनका जीवन स्तर निम्न बना रहता है।
प्रश्न 6: सरकार द्वारा ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’, ‘स्वच्छ भारत मिशन’ और ‘संपूर्ण शिक्षा अभियान’ जैसी योजनाएँ चलाई गई हैं जिनका उद्देश्य गाँवों को सड़कों से जोड़ना, स्वच्छता बढ़ाना और शिक्षा का स्तर सुधारना है। इन योजनाओं से ग्रामीण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है।
प्रश्न 7: ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करना, युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा देना, योजनाओं का ईमानदार क्रियान्वयन और ग्रामीण जनता को योजनाओं के प्रति जागरूक बनाना आवश्यक है। इससे उनकी क्षमता और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।
- प्रकृति केवल देखने की वस्तु नहीं है, वह मानव जीवन की आधारशिला है। वनों की हरियाली, नदियों की कलकल, पर्वतों की विशालता और आकाश की व्यापकता – ये सभी जीवन को ऊर्जा प्रदान करते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश, आधुनिक मानव ने अपने लोभ और सुविधा के लिए प्रकृति का दोहन करना प्रारंभ कर दिया है। वनों की अंधाधुंध कटाई, जल स्रोतों का प्रदूषण, औद्योगीकरण और प्लास्टिक जैसी अपघटनीय वस्तुओं का अत्यधिक उपयोग पृथ्वी को विनाश की ओर ले जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा, जैव विविधता में गिरावट – ये सब प्रकृति से असंतुलन के संकेत हैं। वैज्ञानिकों ने चेताया है कि यदि यह स्थिति जारी रही तो पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ सकता है। वनस्पतियाँ और जीव-जंतु विलुप्त हो सकते हैं, फसलें प्रभावित होंगी और जल संकट गंभीर रूप ले सकता है। हालाँकि इस समस्या का समाधान हमारे ही हाथ में है। यदि हम सतर्क हो जाएँ और जीवनशैली में छोटे-छोटे परिवर्तन लाएँ, तो पृथ्वी को पुनः संतुलित किया जा सकता है। वृक्षारोपण करना, प्लास्टिक का प्रयोग कम करना, जल-संरक्षण करना, अक्षय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना – ये कुछ ऐसे कदम हैं जो प्रकृति की रक्षा में सहायक हो सकते हैं। आज का विद्यार्थी वर्ग, जो देश का भविष्य है, इस परिवर्तन का अग्रदूत बन सकता है। उन्हें पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से प्रकृति के महत्व को समझाया जाना चाहिए और व्यवहार में लागू करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। जब हर व्यक्ति अपने स्तर पर सजग होगा, तभी यह धरती हरी-भरी और सुरक्षित रह पाएगी।
प्रश्नपत्र
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक):
प्रश्न 1: आधुनिक मानव ने किस कारण प्रकृति का दोहन प्रारंभ किया? (1 अंक)
(क) उत्सुकता
(ख) सुविधा और लोभ
(ग) ज्ञान की कमी
(घ) विज्ञान के प्रभाव
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन-सी अपघटनीय वस्तु है? (1 अंक)
(क) कागज
(ख) कपड़ा
(ग) प्लास्टिक
(घ) लकड़ी
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): तापमान में वृद्धि जलवायु परिवर्तन का संकेत है।
Reason (R): औद्योगिक क्रियाकलाप और वनों की कटाई इसके प्रमुख कारण हैं।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: विद्यार्थियों की पर्यावरण सुरक्षा में क्या भूमिका हो सकती है? (1 अंक)
(क) केवल पौधारोपण करना
(ख) पर्यावरणीय शिक्षा को परीक्षा तक सीमित रखना
(ग) केवल व्याख्यान सुनना
(घ) व्यवहार में परिवर्तन लाना और जागरूकता फैलाना
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: जलवायु असंतुलन के मुख्य लक्षण क्या हैं और ये मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? (2 अंक)
प्रश्न 6: प्रकृति की रक्षा के लिए आम व्यक्ति को अपने जीवन में कौन-कौन से छोटे परिवर्तन लाने चाहिए? (2 अंक)
प्रश्न 7: विद्यार्थी वर्ग को किस प्रकार पर्यावरणीय संरक्षण का अग्रदूत बनाया जा सकता है? (2 अंक)
उत्तरकुंजी
प्रश्न 1: (ख) सुविधा और लोभ
प्रश्न 2: (ग) प्लास्टिक
प्रश्न 3: (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
प्रश्न 4: (घ) व्यवहार में परिवर्तन लाना और जागरूकता फैलाना
प्रश्न 5: जलवायु असंतुलन के लक्षणों में तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा, ग्लेशियरों का पिघलना और जैव विविधता की हानि शामिल हैं। ये लक्षण मानव जीवन को फसल उत्पादन में कमी, जल संकट, स्वास्थ्य समस्याओं और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में प्रभावित करते हैं।
प्रश्न 6: आम व्यक्ति को प्लास्टिक का प्रयोग कम करना, वृक्षारोपण करना, जल और ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करना, सार्वजनिक परिवहन अपनाना तथा अपने घर और कार्यस्थल पर स्वच्छता बनाए रखना जैसे छोटे-छोटे परिवर्तन लाने चाहिए।
प्रश्न 7: विद्यार्थियों को व्यवहारिक परियोजनाओं, पर्यावरणीय क्लबों, वृक्षारोपण अभियानों, ऊर्जा संरक्षण योजनाओं तथा पाठ्यक्रमों में पर्यावरण से जुड़े विषयों के माध्यम से प्रेरित किया जा सकता है ताकि वे स्वयं जागरूक बनें और दूसरों को भी प्रेरित करें।
- भारत एक युवा देश है। यहाँ की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यह तथ्य अपने-आप में देश की प्रगति और शक्ति का संकेत है, लेकिन केवल संख्या बल से कुछ नहीं होता, यदि इस युवा शक्ति को दिशा, अवसर और उपयुक्त संसाधन न मिलें तो यह शक्ति निष्क्रिय या विनाशकारी भी बन सकती है। आज के युवाओं के सामने कई प्रकार की चुनौतियाँ हैं – बेरोजगारी, मानसिक तनाव, नशे की लत, सामाजिक दबाव और मार्गदर्शन की कमी। दूसरी ओर, यह पीढ़ी तकनीकी रूप से दक्ष, नवीन सोच से परिपूर्ण और सामाजिक बदलाव की इच्छुक भी है। आवश्यकता है कि इन गुणों को पहचान कर उन्हें सही दिशा दी जाए। शिक्षा प्रणाली में केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य, करियर काउंसलिंग और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी अत्यंत आवश्यक है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘स्किल इंडिया’, ‘स्टार्ट-अप इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’ जैसे अभियान तभी सफल हो सकते हैं जब युवा जागरूक, प्रशिक्षित और आत्मनिर्भर बनें। युवाओं को भी चाहिए कि वे अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएँ। देश को केवल शिकायतों की नहीं, समाधान खोजने वाली सोच की ज़रूरत है। यदि हर युवा अपने भीतर की संभावनाओं को पहचान ले और समाज हित में उसे उपयोग करे, तो भारत न केवल एक विकसित देश बन सकता है, बल्कि वैश्विक नेतृत्व में भी अग्रणी भूमिका निभा सकता है।
प्रश्नपत्र
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक):
प्रश्न 1: भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है? (1 अंक)
(क) 45%
(ख) 55%
(ग) 65%
(घ) 75%
प्रश्न 2: निम्न में से कौन-सी योजना युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है? (1 अंक)
(क) स्वच्छ भारत
(ख) स्किल इंडिया
(ग) प्रधानमंत्री आवास
(घ) जल जीवन मिशन
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): भारत के युवाओं में नवाचार की क्षमता और तकनीकी दक्षता है।
Reason (R): युवा वर्ग आज भी केवल पारंपरिक सोच में बंधा हुआ है।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: युवाओं को देश के विकास में क्या भूमिका निभानी चाहिए? (1 अंक)
(क) केवल शिकायत करना
(ख) नशे की ओर झुकाव
(ग) समाधान आधारित सोच अपनाना
(घ) तकनीक से दूर रहना
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: आज के युवाओं को किन-किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है? (2 अंक)
प्रश्न 6: शिक्षा व्यवस्था में कौन-से सुधार आवश्यक हैं ताकि युवा अधिक सक्षम बनें? (2 अंक)
प्रश्न 7: यदि युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएँ तो भारत को क्या लाभ हो सकता है? (2 अंक)
उत्तरकुंजी
प्रश्न 1: (ग) 65%
प्रश्न 2: (ख) स्किल इंडिया
प्रश्न 3: (ख) A सही है, परंतु R गलत है।
प्रश्न 4: (ग) समाधान आधारित सोच अपनाना
प्रश्न 5: आज के युवाओं को बेरोजगारी, मानसिक तनाव, नशे की लत, सामाजिक दबाव और उचित मार्गदर्शन की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के कारण उनकी ऊर्जा गलत दिशा में जा सकती है।
प्रश्न 6: शिक्षा व्यवस्था में किताबी ज्ञान के स्थान पर व्यावसायिक और कौशल आधारित प्रशिक्षण, करियर काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और नैतिक मूल्यों की शिक्षा को शामिल करना आवश्यक है।
प्रश्न 7: यदि युवा सकारात्मक दिशा में कार्य करें, तो वे नए उद्यम शुरू कर सकते हैं, देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकते हैं और भारत को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं।
- भारत में शहरीकरण की गति तीव्र होती जा रही है, और इसके साथ ही शहरी जीवन की चुनौतियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। गाँवों से शहरों की ओर पलायन, बढ़ती जनसंख्या, सीमित संसाधन, और अव्यवस्थित विकास ने शहरों को जटिल समस्याओं का केंद्र बना दिया है। सबसे पहली समस्या आवास की है—प्रत्येक व्यक्ति को रहने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सुलभ स्थान की आवश्यकता होती है, परंतु महानगरों में झुग्गी-झोपड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो न केवल जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त, यातायात जाम, प्रदूषण, पानी की कमी, और ठोस कचरे का निष्प्रभावी प्रबंधन शहरी जीवन को और कठिन बना देते हैं। वायु और ध्वनि प्रदूषण से लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी ओर, शहरी जीवन की तेज़ गति और प्रतिस्पर्धा के कारण तनाव, अकेलापन और अवसाद जैसी मानसिक समस्याएँ बढ़ रही हैं। लोग सुविधाएँ तो प्राप्त कर रहे हैं, परंतु उनमें आपसी संवाद और मानवीय संबंधों की गहराई घटती जा रही है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण की कमी भी शहरी जीवन की एक गंभीर चुनौती है। हालाँकि सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना, शहरी विकास मिशन, और किफायती आवास योजना जैसी कई पहलें की गई हैं, लेकिन उनका प्रभाव तभी पड़ेगा जब योजनाओं को धरातल पर ईमानदारी से लागू किया जाए और जनता की सहभागिता सुनिश्चित हो। इसके साथ ही यह आवश्यक है कि शहरी जीवन में मूलभूत ढाँचे के विकास के साथ-साथ सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाए। शहरों को केवल इमारतों और सड़कों से नहीं, बल्कि स्वस्थ, सुरक्षित और समावेशी समुदायों से परिभाषित किया जाना चाहिए।
प्रश्नपत्र
1. बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक):
प्रश्न 1: शहरी जीवन की सबसे प्रमुख समस्या क्या बताई गई है? (1 अंक)
(क) शिक्षा की कमी
(ख) आवास की समस्या
(ग) इंटरनेट की कमी
(घ) मनोरंजन की कमी
प्रश्न 2: शहरी जीवन में मानसिक समस्याओं के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? (1 अंक)
(क) खराब जलवायु
(ख) प्रदूषित भोजन
(ग) तेज़ गति और प्रतिस्पर्धा
(घ) तकनीकी विकास
प्रश्न 3: Assertion-Reasoning (1 अंक)
Assertion (A): शहरों में झुग्गियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
Reason (R): क्योंकि महानगरों में सभी को मुफ्त मकान उपलब्ध कराया जाता है।
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, परंतु R गलत है।
(ग) A गलत है, परंतु R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
प्रश्न 4: निम्न में से कौन-सी योजना शहरी जीवन से संबंधित नहीं है? (1 अंक)
(क) स्मार्ट सिटी मिशन
(ख) प्रधानमंत्री आवास योजना
(ग) नमामि गंगे
(घ) अटल शहरी विकास योजना
2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक):
प्रश्न 5: शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण किस प्रकार जीवन को प्रभावित कर रहा है? (2 अंक)
प्रश्न 6: शहरी जीवन में आपसी संवाद और मानवीय संबंध किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं? (2 अंक)
प्रश्न 7: शहरों में बच्चों और बुजुर्गों की समस्याओं को किस रूप में देखा जा सकता है? (2 अंक)
उत्तर कुंजी
1. बहुविकल्पीय उत्तर:
- (ख)
- (ग)
- (ख)
- (ग)
2. दीर्घ उत्तरीय उत्तर:
5. शहरी क्षेत्रों में वायु और ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे श्वसन रोग, हृदय संबंधी समस्याएँ और मानसिक तनाव उत्पन्न होते हैं। यातायात और औद्योगिक धुएँ से पर्यावरण विषैला हो जाता है, जो जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।
- शहरी जीवन की तेज़ गति, अत्यधिक कार्यभार और प्रतिस्पर्धा के कारण लोग एक-दूसरे से कटने लगे हैं। परिवारों में बातचीत कम होती है और व्यक्तिगत रिश्तों में दूरी बढ़ रही है, जिससे समाज में अलगाव और अवसाद की भावना बढ़ रही है।
- शहरों में बच्चों के लिए खेलने की सुरक्षित जगह और बुजुर्गों के लिए सामूहिक गतिविधियों की कमी होती है। अकेलेपन के कारण दोनों वर्गों में मानसिक और शारीरिक समस्याएँ बढ़ती हैं। सुरक्षा, सुविधाएँ और देखभाल की कमी उनकी कठिनाइयों को बढ़ा देती है।