कक्षा – 09 अपठित गद्यांश (Unseen Prose Passages)
‘अपठित’ यह शब्द ‘अ’ उपसर्ग, ‘पठ्’ धातु और ‘इत’ प्रत्यय से मिलकर बना है। ‘अपठित’ शब्द का अर्थ है- जो कभी पढ़ा न गया हो। अर्थात अपठित गद्याश वे गद्यांश हैं जिनको छात्रों ने पहले कभी अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ा नहीं है। अपठित गद्यांश देकर उस पर भाव-बांध संबंधी प्रश्न पूछे जाते है। इन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को उसी गद्यांश के आधार पर देने होते हैं। उत्तर देते समय यह कोशिश होनी चाहिए कि उत्तर में गद्यांश के वाक्यों को जैसा का तैसा न उतारा जाए बल्कि उसमें कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए।
(Download 09 Hindi A & B papers in word format – Click Here)
अपठित गद्यांश का उद्देश्य
मूल्यांकन हेतु अपठित गद्यांश दिए जाने का उद्देश्य है- छात्रों के भाषा-बोध का पता लगाना। अर्थात यह जानना कि छात्र उस गद्द्याश की भाषा को समझते हैं या नहीं। साथ ही इससे उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का भी पता चल जाता है।
अपठित गद्यांश हल करते समय ध्यान देने योग्य बाते-
• दिए गए गद्यांश का एक-दो बार मौन वाचन करें तथा उसे समझने का प्रयास करें।
• तदुपरांत प्रश्नों को अलग-अलग पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के संभावित उत्तर को गद्यांश में रेखांकित करें। जब प्रश्नों के उत्तर लिखना प्रारंभ करें तो लेखक द्वारा कही गई बात को सरल एवं स्पष्ट भाषा में छोटे-छोटे वाक्यों में व्यक्त करें।
• यदि शीर्षक देना हो, तो किसी रफ़ कागज पर सोचकर दो-तीन शीर्षक लिख लें। फिर उनमें से जो सबसे अधिक उपयुक्त लगे उसे उत्तर के रूप में लिखें। यदि प्रश्नों का प्रारूप बहुविकल्पीय है तो सारे विकल्पों को ध्यान से पढ़कर सर्वाधिक उचित विकल्प पर निशान लगाइए।
कक्षा 09 अपठित गद्यांश के उदाहरण (बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय
अपठित गद्यांश
- हर बड़ा साहित्यकार साहित्य और विशेषकर शब्द की गरिमा और मर्यादा पर लड़ने-मरने को तैयार रहता है। बच्चन जी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने अपने संपूर्ण लेखन में शब्दों के चयन, अभिव्यक्ति की स्पष्टता और भावों की गंभीरता को विशेष स्थान दिया। वे मानते थे कि शब्द केवल माध्यम नहीं होते, बल्कि संवेदना के वाहक होते हैं। बच्चन जी ने जितना आदर अपने साहित्य का किया, उतना ही उन्होंने भारत तथा विदेशों के साहित्य का भी सम्मान किया। उनके लिए भाषा मात्र संवाद का उपकरण नहीं थी, बल्कि यह संस्कृति की आत्मा थी। यही कारण था कि उन्होंने अनुवाद करते समय भाषा की गरिमा बनाए रखने पर विशेष बल दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी का अनुवाद यदि बाजारू स्तर की हिंदी में किया जाए तो वह हिंदी के साथ अन्याय होगा। उनके अनुसार शब्दों की शक्ति केवल अर्थ को व्यक्त करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे समाज के सोचने और अनुभव करने के ढंग को भी निर्धारित करते हैं। उनका दृष्टिकोण यह था कि अनुवाद का उद्देश्य मूल भाव और गरिमा को बनाए रखते हुए अर्थ का संवेदनशील स्थानांतरण होना चाहिए। बच्चन जी यह भी कहते थे कि जब हिंदी अंग्रेजी के स्तर तक उठने की कोशिश करती है, तो उसे कठिन और क्लिष्ट कहा जाता है और जब वह अधिक सरलता की ओर झुकती है, तो उसे अपरिपक्व करार दे दिया जाता है। उनके लिए यह विडंबना चिंताजनक थी। उन्होंने अपने गद्य और पद्य दोनों में ही एक सुंदर, सुगठित, स्पष्ट और भावपूर्ण हिंदी का प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया कि आवश्यकता के अनुसार संस्कृतनिष्ठ होते हुए भी हिंदी लोकप्रिय, ग्राह्य और लोकरंजक बन सकती है। वे यह भी मानते थे कि भाषा केवल साहित्य की नहीं, बल्कि सोचने और अनुभव करने की शक्ति होती है। भाषा समाज की चेतना का निर्माण करती है और उसकी अभिव्यक्ति को स्वर देती है। इसी सोच के साथ उन्होंने शब्दों की दुनिया को एक नई दृष्टि दी और साहित्य की दुनिया में शब्द की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया।
प्रश्नावली:
प्रश्न 1: निम्न कथनों में से किनके आधार पर बच्चन जी के भाषा-सम्बंधी दृष्टिकोण को समझा जा सकता है? (1 अंक)
(1) उन्होंने भाषा को संवाद का उपकरण मात्र माना।
(2) वे अनुवाद में मूल भावों की गरिमा बनाए रखने के पक्ष में थे।
(3) वे शब्दों को संवेदना का वाहक मानते थे।
(4) वे अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद को सरल बनाने के पक्षधर थे।
विकल्प:
(क) केवल 2 और 3
(ख) केवल 1 और 4
(ग) केवल 2 और 4
(घ) केवल 3
प्रश्न 2: बच्चन जी ने हिंदी भाषा के संदर्भ में कौन-सी विडंबना बताई है? (1 अंक)
(क) हिंदी सरल हो जाए तो क्लिष्ट मानी जाती है
(ख) हिंदी कठिन हो जाए तो अंग्रेजी कहलाती है
(ग) कठिन हिंदी को सराहा जाता है
(घ) अंग्रेजी को ही मानक भाषा समझा जाता है
प्रश्न 3: Assertion (A) और Reason (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। (1 अंक)
Assertion (A): बच्चन जी ने हिंदी भाषा को भावपूर्ण और ग्राह्य बनाने का प्रयास किया।
Reason (R): वे मानते थे कि भाषा केवल संवाद की विधा नहीं, बल्कि सोचने और अनुभव करने की शक्ति भी होती है।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है परंतु R गलत है।
(घ) A गलत है परंतु R सही है।
प्रश्न 4: बच्चन जी का अनुवाद के प्रति दृष्टिकोण क्या था और उन्होंने हिंदी की गरिमा बनाए रखने के लिए कौन-से प्रयास किए? (2 अंक)
प्रश्न 5: बच्चन जी ने हिंदी भाषा को ग्राह्य और लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय अपनाए और वे भाषा को किस दृष्टि से देखते थे? (2 अंक)
उत्तरकुंजी:
प्रश्न 1: (क) केवल 2 और 3
प्रश्न 2: (क) हिंदी सरल हो जाए तो क्लिष्ट मानी जाती है
प्रश्न 3: (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
प्रश्न 4 (उत्तर): बच्चन जी का मानना था कि अनुवाद करते समय मूल भावों और भाषा की गरिमा को बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने बाजारू हिंदी के विरोध में उच्चकोटि की हिंदी का प्रयोग किया, जिससे अनुवाद भी सम्मानजनक बना रहे।
प्रश्न 5 (उत्तर): बच्चन जी ने अपने गद्य और पद्य दोनों में स्पष्ट, भावपूर्ण और संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग किया। वे भाषा को केवल साहित्य की नहीं, बल्कि सोचने और अनुभव करने की शक्ति मानते थे।
- संसार में अमरता उन्हें ही प्राप्त होती है जो अपने पीछे ऐसे विचार, मूल्य और कर्म छोड़ जाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं जहाँ किसी महान व्यक्तित्व ने साधारण जीवन जीते हुए भी असाधारण कार्य किए और मानवता के लिए आदर्श बन गए। प्रायः यह देखा गया है कि ऐसे महान व्यक्तित्वों का जन्म संपन्न परिवारों में नहीं, बल्कि मध्यम या गरीब वर्गों में होता है। विपरीत परिस्थितियाँ उनके भीतर विनय, सहनशीलता, कष्ट-सहिष्णुता, साहस, और उदारता जैसे गुणों का विकास करती हैं। यही चारित्रिक गुण उन्हें अहंकारहीन और सादा जीवन जीने योग्य बनाते हैं। सादगी केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि विचारों में भी होनी चाहिए। विचारों की ऊँचाई और जीवन की सरलता एक आदर्श संतुलन है जो किसी भी व्यक्ति को महान बना सकती है। सादा जीवन जीने के लिए दो बातें अत्यंत आवश्यक हैं—एक, कठिन परिस्थितियों में धैर्य न छोड़ना, और दो, अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना। आज के उपभोक्तावादी युग में व्यक्ति जितना अधिक भौतिक सुखों की ओर आकर्षित हो रहा है, उतना ही वह सादगी और आत्म-संयम से दूर होता जा रहा है। जबकि सच्चा आत्मसम्मान तभी टिकता है जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को विवेकपूर्वक सीमित रखे और कभी आत्मगौरव को ठेस न पहुँचने दे। विचारशील व्यक्ति जानता है कि बाहरी दिखावा क्षणिक है, जबकि चरित्र की सादगी स्थायी प्रभाव छोड़ती है। इसलिए जीवन की सच्ची गरिमा सादगी और उच्च विचारों में है, जो मनुष्य को आंतरिक रूप से शक्तिशाली और समाज के लिए अनुकरणीय बनाती है।
प्रश्नावली:
प्रश्न 1: निम्न कथनों में से किनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विपरीत परिस्थितियाँ महानता की ओर ले जाती हैं? (1 अंक)
(1) विपरीत परिस्थितियाँ विनय और सहनशीलता का विकास करती हैं।
(2) वे व्यक्ति को विलासिता की ओर ले जाती हैं।
(3) साधारण जीवन में असाधारण कर्म जन्म लेते हैं।
(4) सादगी और चरित्र में संबंध होता है।
विकल्प:
(क) केवल 1 और 2
(ख) केवल 1 और 3
(ग) केवल 2 और 4
(घ) केवल 3 और 4
प्रश्न 2: लेखक के अनुसार सच्चा आत्मसम्मान किस स्थिति में टिकता है? (1 अंक)
(क) जब व्यक्ति दिखावे से दूर रहता है
(ख) जब भौतिक वस्तुएँ पर्याप्त हों
(ग) जब आत्मगौरव को ठेस न पहुँचे और आवश्यकताएँ सीमित हों
(घ) जब व्यक्ति समाज में प्रसिद्ध हो जाए
प्रश्न 3: Assertion (A) और Reason (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। (1 अंक)
Assertion (A): सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति समाज के लिए अनुकरणीय बनता है। (1 अंक)
Reason (R): क्योंकि वह आंतरिक रूप से शक्तिशाली होता है और दिखावे से दूर रहता है।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है परंतु R गलत है।
(घ) A गलत है परंतु R सही है।
प्रश्न 4: लेखक के अनुसार महानता और सादगी के बीच क्या संबंध है? (2 अंक)
प्रश्न 5: आज के उपभोक्तावादी युग में व्यक्ति सादगी से क्यों दूर होता जा रहा है और इसका क्या प्रभाव है? (2 अंक)
उत्तरकुंजी:
प्रश्न 1: (ख) केवल 1 और 3
प्रश्न 2: (ग) जब आत्मगौरव को ठेस न पहुँचे और आवश्यकताएँ सीमित हों
प्रश्न 3: (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
प्रश्न 4 (उत्तर): लेखक के अनुसार सादगी और महानता एक-दूसरे के पूरक हैं। सादा जीवन व्यक्ति के अंदर विनय, सहनशीलता और चारित्रिक ऊँचाई लाता है, जो उसे महान बनाता है।
प्रश्न 5 (उत्तर): आज व्यक्ति भौतिक सुखों के आकर्षण में सादगी और आत्म-संयम से दूर होता जा रहा है। इसका परिणाम यह होता है कि वह आंतरिक रूप से कमजोर हो जाता है और आत्मसम्मान खो बैठता है।
- मैं सोचता हूँ स्त्रियों के पास एक महान शक्ति सोई हुई है। दुनिया की आधी से बड़ी ताकत उनके पास है। आधी तो इसलिए कहता हूँ कि दुनिया में स्त्रियाँ आधी तो हैं ही। आधी से बड़ी इसलिए कि बच्चे उनकी छाया में पलते हैं। अतः वे जैसा चाहें वैसा उनके व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती हैं। पुरुष के हाथ में चाहे जितनी ताकत हो, लेकिन वह एक दिन स्त्री की गोद में होता है, वहीं से वह अपनी यात्रा शुरू करता है। स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संस्कृति, एक भावना, और एक विचार की संवाहिका है। जहाँ भी प्रेम, करुणा और दया है, वहाँ स्त्री मौजूद है। वही अपने कोमल स्वभाव से घर, समाज और देश को एकता और स्नेह से बाँधती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्त्री के पास आधी से भी बड़ी ताकत है और वह पाँच हजार वर्षों से बिलकुल सोई हुई है। यह शक्ति यदि जाग जाए तो सामाजिक क्रांति संभव है। नारी की शक्ति का कोई उपयोग नहीं हो सका है, क्योंकि सदियों तक उसे सीमित भूमिकाओं तक बाँध दिया गया। लेकिन अब समय बदल रहा है। स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। अब उन्हें यह समझना होगा कि उन्हें पुरुषों की नकल नहीं करनी है, बल्कि अपनी विशिष्टता और गरिमा बनाए रखते हुए आगे बढ़ना है। नारी यदि अपनी शक्ति को पहचान ले तो न केवल वह अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकती है, बल्कि पूरे समाज का नव निर्माण कर सकती है।
प्रश्नावली:
प्रश्न 1: स्त्रियों की शक्ति के संदर्भ में लेखक निम्न में से किन विचारों को प्रस्तुत करता है? (1 अंक)
(1) स्त्री एक विचार और भावना की संवाहिका है।
(2) स्त्री समाज को विभाजित करती है।
(3) स्त्री शिक्षा प्राप्त कर रही है और आत्मनिर्भर बन रही है।
(4) स्त्री का कोई प्रभाव नहीं रहा है।
विकल्प:
(क) केवल 1 और 3
(ख) केवल 2 और 4
(ग) केवल 1 और 2
(घ) केवल 3 और 4
प्रश्न 2: लेखक के अनुसार स्त्री की जाग्रत शक्ति समाज के लिए क्यों आवश्यक है? (1 अंक)
(क) क्योंकि वह पुरुषों की जगह ले सकती है
(ख) क्योंकि वह समाज में क्रांति ला सकती है
(ग) क्योंकि वह परंपरा को तोड़ सकती है
(घ) क्योंकि वह घर छोड़ सकती है
प्रश्न 3: Assertion (A) और Reason (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। (1 अंक)
Assertion (A): स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संस्कृति और भावना की संवाहिका है। (1 अंक)
Reason (R): वह प्रेम, करुणा और दया के माध्यम से समाज को बाँधती है।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है परंतु R गलत है।
(घ) A गलत है परंतु R सही है।
प्रश्न 4: लेखक ने स्त्री को ‘आधी से बड़ी शक्ति’ क्यों कहा है? इसका क्या तात्पर्य है? (2 अंक)
प्रश्न 5: लेखक ने नारी को पुरुष की नकल करने के बजाय किस मार्ग पर चलने की सलाह दी है? (2 अंक)
उत्तरकुंजी:
प्रश्न 1: (क) केवल 1 और 3
प्रश्न 2: (ख) क्योंकि वह समाज में क्रांति ला सकती है
प्रश्न 3: (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
प्रश्न 4 (उत्तर): लेखक ने स्त्री को ‘आधी से बड़ी शक्ति’ इसलिए कहा है क्योंकि स्त्री की भूमिका केवल संख्यात्मक नहीं है, बल्कि वह बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण और समाज में स्नेह और एकता लाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
प्रश्न 5 (उत्तर): लेखक ने नारी को पुरुषों की नकल करने के बजाय अपनी विशिष्टता, गरिमा और कोमलता के साथ आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़ने की सलाह दी है ताकि वह समाज में प्रेरणा का स्रोत बन सके।
- तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका उत्तर केवल तुम ही दे सकते हो। कोई अन्य व्यक्ति—even तुम्हारा सबसे प्रिय और विश्वासपात्र मित्र—तुम्हारे जीवन के निर्णायक क्षणों का उत्तरदायित्व नहीं उठा सकता। मनुष्य को चाहिए कि वह अनुभवियों की बातों को ध्यान से सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करे, लेकिन अन्ततः निर्णय उसका स्वयं का हो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे अपने कार्य ही हमारे भविष्य के निर्माता होते हैं। दूसरों की राय भले ही मददगार हो सकती है, लेकिन जब तक हम अपने मन से निर्णय नहीं लेते, तब तक हम सच्ची प्रगति नहीं कर सकते। स्वतंत्र विचार और स्वविवेक के बिना जीवन में ठोस दिशा नहीं मिलती। हमें आत्मनिर्भरता और आत्ममूल्यांकन की आदत डालनी चाहिए। वह व्यक्ति जो सदा दूसरों की बातों पर चलता है, वह स्वयं कभी नेतृत्व नहीं कर सकता। वह केवल अनुकरण कर सकता है। लेखक कहता है कि जिसकी दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊँचा नहीं उठता। यहाँ नीची दृष्टि प्रतीक है–दृढ़ता, आत्मबल और दूरदृष्टि के अभाव की। यदि हम सिर्फ पैरों के नीचे की ज़मीन देखते रहेंगे, तो कभी नहीं जान पाएँगे कि रास्ता हमें कहाँ ले जा रहा है। जीवन में सच्ची स्वतंत्रता केवल बाहर की नहीं, मन की भी होनी चाहिए। लेकिन यह स्वतंत्रता उद्दंडता या कठोरता नहीं होनी चाहिए। व्यवहार में कोमलता और उद्देश्य में ऊँचाई होनी चाहिए। संयम, विनम्रता और उच्च लक्ष्य – यही वो गुण हैं जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। मन कभी निष्क्रिय न हो; विचारों में सजीवता होनी चाहिए। लेखक कहता है कि जिस व्यक्ति का लक्ष्य जितना ऊँचा होता है, उसकी उपलब्धियाँ भी उतनी ही ऊँची होती हैं। यह केवल सिद्धांत नहीं, अनुभवजन्य सत्य है। मनुष्य को स्वयं सोचने, निर्णय लेने, और दिशा चुनने का साहस करना चाहिए, क्योंकि यही गुण उसे आत्मनिर्भर, विवेकशील और सम्मानजनक बनाते हैं।
प्रश्नावली:
प्रश्न 1: लेखक के अनुसार निम्न में से किन तथ्यों से आत्मनिर्भरता का महत्व स्पष्ट होता है? (1 अंक)
(1) अपने निर्णय स्वयं लेना चाहिए
(2) दूसरों की राय कभी माननी ही नहीं चाहिए
(3) जीवन की दिशा स्वतंत्र विचार से तय होती है
(4) सच्ची प्रगति दूसरों के सहारे से होती है
विकल्प:
(क) केवल 1 और 3
(ख) केवल 2 और 4
(ग) केवल 1 और 4
(घ) केवल 2 और 3
प्रश्न 2: लेखक के अनुसार ‘नीची दृष्टि’ का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? (1 अंक)
(क) शारीरिक कमजोरी का प्रतीक
(ख) आत्मबल, दूरदृष्टि और दृढ़ता का अभाव
(ग) दूसरों से तुलना करना
(घ) विनम्रता और अनुशासन
प्रश्न 3: Assertion (A) और Reason (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। (1 अंक)
Assertion (A): व्यक्ति को आत्मनिर्भर और विवेकशील बनना चाहिए। (1 अंक)
Reason (R): क्योंकि यही गुण उसे निर्णय लेने और समाज में सम्मान पाने योग्य बनाते हैं।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है परंतु R गलत है।
(घ) A गलत है परंतु R सही है।
प्रश्न 4: लेखक के अनुसार ‘सच्ची स्वतंत्रता’ किसे कहा गया है और वह जीवन में कैसे दिशा प्रदान करती है? (2 अंक)
प्रश्न 5: लेखक ने व्यक्ति को दूसरों की नकल न कर स्वयं निर्णय लेने पर क्यों बल दिया है? (2 अंक)
उत्तरकुंजी:
प्रश्न 1: (क) केवल 1 और 3
प्रश्न 2: (ख) आत्मबल, दूरदृष्टि और दृढ़ता का अभाव
प्रश्न 3: (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
प्रश्न 4 (उत्तर): लेखक के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं, बल्कि मन की होनी चाहिए। जब व्यक्ति अपने विचारों से निर्णय लेता है तो उसे जीवन में ठोस दिशा और लक्ष्य प्राप्त होता है।
प्रश्न 5 (उत्तर): लेखक के अनुसार जो व्यक्ति सदैव दूसरों की बातों पर चलता है, वह नेतृत्व नहीं कर सकता। आत्मनिर्भर निर्णय व्यक्ति को विवेकशील और समाज में सम्मानजनक बनाते हैं।
- एक अंग्रेज डॉक्टर का कहना है कि किसी नगर में दवाई से लदे हुए बीस गधे ले जाने से अधिक लाभकारी एक हँसोड़ आदमी को ले जाना है। यह कथन मजाक प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसमें छिपा हुआ संदेश अत्यंत गंभीर और वैज्ञानिक है। हँसी न केवल मानसिक तनाव को कम करती है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी वरदान समान है। यह शरीर और मन दोनों को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है, रक्त का संचार सुचारु करती है और शरीर से पसीना निकालकर विषैले तत्वों को बाहर करती है। डॉक्टर ह्यूड का कहना है कि हँसी जीवन की सबसे मीठी और सस्ती औषधि है। आनंद से अधिक मूल्यवान वस्तु मनुष्य के पास कुछ नहीं है। जब कोई व्यक्ति जी भरकर हँसता है, तो उसकी भावनाओं में सकारात्मकता आती है और वह दूसरों के प्रति सहिष्णु हो जाता है। कारलाइल जैसे चिंतक भी मानते थे कि जो व्यक्ति हृदय से हँसता है, वह कभी बुरा नहीं होता। हँसी न केवल खुद के लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी फायदेमंद है। यदि आप अपने मित्र को हँसाते हैं, तो वह अधिक प्रसन्न होता है; अपने शत्रु को हँसाइए, तो वह आपसे कम घृणा करेगा; एक अनजान को हँसाइए, तो वह आप पर विश्वास करेगा। यही नहीं, अगर आप किसी निराश व्यक्ति को हँसाते हैं, तो उसकी आशा पुनः जाग सकती है। उदास व्यक्ति को हँसाकर उसका दुख हल्का किया जा सकता है। हँसी के प्रभाव से एक वृद्ध भी अपने को युवा महसूस कर सकता है और एक बच्चा ज्यादा प्रसन्न, चंचल और स्वस्थ बन सकता है। मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक दोनों मानते हैं कि हँसी मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद और अकेलेपन की दवा है। समाज में आज जितना तनाव है, उतना ही अधिक हमें हँसी जैसे स्वाभाविक उपचार की आवश्यकता है। हँसी आत्मीयता और मानवीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाती है। इसलिए हँसी को केवल मजाक का साधन न समझें, यह जीवन की शक्ति है, ऊर्जा है और सबसे आसान औषधि है जिसे कोई भी खर्च किए बिना दूसरों को दे सकता है।
प्रश्नावली:
प्रश्न 1: गद्यांश के अनुसार हँसी से संबंधित कौन-कौन-से लाभ होते हैं? (1 अंक)
(1) यह मन और शरीर दोनों को प्रसन्न करती है।
(2) यह केवल मनोरंजन का साधन है।
(3) यह रक्त संचार को सुधारती है।
(4) यह व्यक्ति को स्वार्थी बना देती है।
विकल्प:
(क) केवल 1 और 3
(ख) केवल 1 और 2
(ग) केवल 2 और 4
(घ) केवल 3 और 4
प्रश्न 2: लेखक के अनुसार किसी निराश व्यक्ति को हँसाना क्यों लाभकारी होता है? (1 अंक)
(क) क्योंकि वह अधिक चुप रहता है
(ख) क्योंकि उसकी आशा पुनः जाग सकती है
(ग) क्योंकि वह दुश्मन बन जाता है
(घ) क्योंकि वह ज्यादा खर्च करता है
प्रश्न 3: Assertion (A) और Reason (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। (1 अंक)
Assertion (A): हँसी मानसिक तनाव और चिंता की प्राकृतिक दवा है। (1 अंक)
Reason (R): क्योंकि हँसी शरीर में विषैले तत्वों को बाहर निकालती है और सकारात्मक ऊर्जा देती है।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है परंतु R गलत है।
(घ) A गलत है परंतु R सही है।
प्रश्न 4: डॉक्टर ह्यूड के अनुसार हँसी को “मीठी और सस्ती औषधि” क्यों कहा गया है? (2 अंक)
प्रश्न 5: लेखक के अनुसार हँसी सामाजिक संबंधों और दूसरों के व्यवहार पर क्या प्रभाव डालती है? (2 अंक)
उत्तरकुंजी:
प्रश्न 1: (क) केवल 1 और 3
प्रश्न 2: (ख) क्योंकि उसकी आशा पुनः जाग सकती है
प्रश्न 3: (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
प्रश्न 4 (उत्तर): डॉक्टर ह्यूड के अनुसार हँसी न केवल आनंद प्रदान करती है बल्कि मानसिक तनाव, चिंता और शारीरिक विषाक्तता को भी दूर करती है। यह बिना किसी खर्च के उपलब्ध होती है, इसलिए यह मीठी और सस्ती औषधि है।
प्रश्न 5 (उत्तर): लेखक के अनुसार हँसी दूसरों के प्रति सहिष्णुता, विश्वास और आत्मीयता उत्पन्न करती है। यह मित्रता को मजबूत करती है, शत्रुता को कम करती है और सामाजिक संबंधों को मधुर बनाती है।
- कहने को भारत एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और स्वशासी राष्ट्र है जहाँ ‘भारतीयकरण’ की बात की जाती है और संस्कृति के संरक्षण का दावा किया जाता है। लेकिन जब व्यवहारिक पक्ष को देखा जाता है तो स्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है। देश में आस्थावानता की अपेक्षा आस्थाहीनता तेजी से बढ़ रही है। मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों में भीड़ अवश्य बढ़ी है, लेकिन यह भीड़ प्रायः सामाजिक दिखावे, कर्मकांड या प्रचार माध्यमों के प्रभाव से प्रेरित प्रतीत होती है। टीवी चैनलों द्वारा मेलों और पर्वों का अत्यधिक कवरेज भी इसी भ्रम को और गहरा करता है कि देश में आस्था मजबूत हो रही है। परंतु सच्चाई यह है कि यह सब सतही है—बाहरी दिखावा, भीड़ का प्रभाव, या मनोवैज्ञानिक दबाव। आस्था का अर्थ केवल धार्मिक स्थलों पर जाना नहीं, बल्कि उसे आचरण में उतारना है। गांधीजी को लेकर बनी ‘लगे रहो मुन्ना भाई’ जैसी फिल्मों में उनके सिद्धांतों को हास्य व नाटकीयता के रूप में प्रस्तुत किया गया। इससे दर्शकों को कुछ पल का मनोरंजन अवश्य मिला, परंतु जीवन में परिवर्तन लाने जैसा कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। गांधी को यदि हम केवल ‘गांधीगिरी’ तक सीमित कर दें, तो यह उनके जीवन-मूल्यों और विचारों के साथ अन्याय होगा। वास्तविक श्रद्धा और आस्था तभी संभव है जब हम उनके विचारों जैसे सत्य, अहिंसा, संयम, सादगी, कर्तव्यनिष्ठा और आत्मानुशासन को अपने जीवन में अपनाएँ। अफसोस की बात है कि आज 2 अक्टूबर या 30 जनवरी जैसे दिनों पर औपचारिक भाषण और आयोजनों तक ही सब सीमित रह गया है। हम उनके आदर्शों के प्रति संकल्प लेते हैं, मगर व्यवहार में उनका कोई अंश नहीं दिखता। केवल प्रतीकों और आडंबरों से समाज नहीं बदलता। सच्ची आस्था वह है जो विचारों में गहराई और कर्मों में ईमानदारी लाए। अन्यथा यह दिखावटी संस्कृति समाज को खोखला बना रही है।
प्रश्नावली:
प्रश्न 1: लेखक के अनुसार भारत में आस्था की स्थिति को किस प्रकार समझा जा सकता है? (1 अंक)
(1) धार्मिक स्थलों में बढ़ती भीड़ से आस्था बढ़ रही है।
(2) टीवी और मीडिया आस्था के प्रचार में योगदान दे रहे हैं।
(3) वास्तविक आस्था आचरण में उतरती है, न कि केवल उपस्थिति से।
(4) संस्कृति का संरक्षण केवल सरकार का कार्य है।
विकल्प:
(क) केवल 1 और 2
(ख) केवल 3 और 4
(ग) केवल 2 और 4
(घ) केवल 2 और 3
प्रश्न 2: लेखक के अनुसार ‘गांधीगिरी’ को केवल हास्य तक सीमित कर देना क्यों अनुचित है? (1 अंक)
(क) क्योंकि यह राजनीतिक उपयोग है
(ख) क्योंकि यह फिल्मों का हिस्सा है
(ग) क्योंकि यह गांधीजी के सिद्धांतों की गहराई को नजरअंदाज़ करता है
(घ) क्योंकि यह मीडिया की चाल है
प्रश्न 3: Assertion (A) और Reason (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। (1 अंक)
Assertion (A): सच्ची आस्था कर्मों की ईमानदारी में दिखाई देती है। (1 अंक)
Reason (R): क्योंकि केवल प्रतीकों और आयोजनों से समाज नहीं बदलता।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है परंतु R गलत है।
(घ) A गलत है परंतु R सही है।
प्रश्न 4: लेखक के अनुसार धार्मिक स्थलों की भीड़ को आस्था का प्रमाण क्यों नहीं माना जा सकता? (2 अंक)
प्रश्न 5: गांधीजी के विचारों को व्यवहार में लाना क्यों आवश्यक है, और लेखक इसे क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? (2 अंक)
उत्तरकुंजी:
प्रश्न 1: (घ) केवल 2 और 3
प्रश्न 2: (ग) क्योंकि यह गांधीजी के सिद्धांतों की गहराई को नजरअंदाज़ करता है
प्रश्न 3: (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
प्रश्न 4 (उत्तर): धार्मिक स्थलों की भीड़ केवल सामाजिक दबाव, प्रचार या दिखावे का परिणाम हो सकती है। वास्तविक आस्था तभी मानी जा सकती है जब वह जीवन और व्यवहार में झलके।
प्रश्न 5 (उत्तर): लेखक के अनुसार गांधीजी के विचार जैसे सत्य, अहिंसा, सादगी और कर्तव्यनिष्ठा समाज को नैतिक आधार देते हैं। इन्हें अपनाने से व्यक्ति और समाज दोनों में सच्चा परिवर्तन संभव है।
- व्यक्ति से अगली इकाई परिवार की होती है। जब दो व्यक्ति, पति-पत्नी के रूप में जीवनयात्रा आरंभ करते हैं, और उसमें माता-पिता तथा बच्चे शामिल होते हैं, तब मिलकर एक सामाजिक इकाई का निर्माण होता है जिसे हम परिवार कहते हैं। परिवार केवल कुछ व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि वह संस्था है जो समाज और राष्ट्र की संरचना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब परिवार सुखी और संतुलित होता है, तभी समाज और राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित होती है। ‘परिवार कल्याण’ शब्द का अर्थ केवल आर्थिक उन्नति नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक संतुलन से भी है। परिवार को सीमित रखने का भाव केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व भी है। यदि एक परिवार के सदस्य सीमित संख्या में हों, तो उपलब्ध संसाधनों का समुचित वितरण हो सकता है, जिससे परिवार में आर्थिक बोझ कम पड़ता है और प्रत्येक सदस्य को बेहतर जीवन-स्तर प्राप्त होता है। दुर्भाग्यवश, आज हमारे देश में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वह न केवल संसाधनों पर दबाव बना रही है, बल्कि परिवारों की स्थिरता और खुशहाली को भी प्रभावित कर रही है। जब एक कमाई करने वाले व्यक्ति को बड़ी संख्या में आश्रितों का पालन करना पड़ता है, तो उसकी आय पर्याप्त नहीं रहती, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और मूलभूत सुविधाओं में कमी आती है। अतः परिवार कल्याण का विचार केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक हित से जुड़ा है। हमें यह समझना चाहिए कि छोटे परिवार का अर्थ केवल कम सदस्य नहीं, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाला जीवन है। इसके लिए समाज में व्यापक जनजागृति आवश्यक है। लोगों को यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि अनियंत्रित जनसंख्या से किस प्रकार उनके बच्चे अशिक्षा, कुपोषण और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। यदि प्रत्येक नागरिक इस बात को समझे कि परिवार की गुणवत्ता उसकी मात्रा से अधिक महत्त्वपूर्ण है, तो न केवल उसका परिवार बल्कि पूरा देश सशक्त हो सकेगा।
प्रश्नावली:
प्रश्न 1: लेखक के अनुसार सीमित परिवार के क्या लाभ हैं? (1 अंक)
(1) उच्च जीवन-स्तर
(2) कम शिक्षा व्यय
(3) सामाजिक सम्मान
(4) कम आर्थिक बोझ
विकल्प:
(क) केवल 1 और 4
(ख) केवल 2 और 3
(ग) केवल 1 और 3
(घ) केवल 2 और 4
प्रश्न 2: लेखक ने परिवार को किस रूप में परिभाषित किया है? (1 अंक)
(क) केवल पति-पत्नी का समूह
(ख) सीमित बच्चों वाला संगठन
(ग) समाज की इकाई और नैतिक संस्था
(घ) आर्थिक संस्था
प्रश्न 3: Assertion (A) और Reason (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। (1 अंक)
Assertion (A): परिवार की गुणवत्ता उसकी मात्रा से अधिक महत्त्वपूर्ण है। (1 अंक)
Reason (R): क्योंकि सीमित परिवार ही समाज की स्थिरता और संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है परंतु R गलत है।
(घ) A गलत है परंतु R सही है।
प्रश्न 4: लेखक के अनुसार परिवार कल्याण को केवल सरकारी योजना मानना क्यों गलत है? (2 अंक)
प्रश्न 5: अनियंत्रित जनसंख्या का परिवार और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? (2 अंक)
उत्तरकुंजी:
प्रश्न 1: (क) केवल 1 और 4
प्रश्न 2: (ग) समाज की इकाई और नैतिक संस्था
प्रश्न 3: (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
प्रश्न 4 (उत्तर): लेखक के अनुसार परिवार कल्याण को केवल सरकारी योजना मानना गलत है क्योंकि यह एक सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व है जो प्रत्येक व्यक्ति को परिवार, समाज और राष्ट्र के हित में निभाना चाहिए।
प्रश्न 5 (उत्तर): अनियंत्रित जनसंख्या से परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएँ प्रभावित होती हैं। यह समाज की स्थिरता और समग्र विकास में बाधा बनता है।
- मनुष्य अपने जन्म के साथ ही अहंकार का एक अदृश्य परंतु गहन बोझ लेकर आता है, जो उसकी सोच और दृष्टिकोण को इतना प्रभावित करता है कि वह स्वयं की बजाय दूसरों की बुराइयों की ओर अधिक सजग रहता है। आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया उसके लिए कठिन और असहज होती है, इस कारण वह परनिंदा और दोषदर्शन में ही आनंद अनुभव करता है। वह दूसरों की तरक्की या सफलता को सहजता से नहीं ले पाता। जैसे ही कोई व्यक्ति उसकी तुलना में आगे बढ़ता है, उसकी ईर्ष्या जाग्रत हो जाती है। यह ईर्ष्या उसके व्यवहार में नकारात्मकता लाती है। वह दूसरे के गुणों को जान-बूझकर अनदेखा करता है और केवल उनके दोषों या कमजोरियों को उजागर करता है। धीरे-धीरे यह प्रवृत्ति आदत में बदल जाती है और फिर उसका जीवन इसी में उलझा रह जाता है। हमारे शास्त्रों में परनिंदा को पाप कहा गया है, और यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों की आलोचना में संलग्न रहता है, वह अंततः स्वयं ही अपनी शांति, संतुलन और स्वास्थ्य को नष्ट करता है। ईर्ष्या की अग्नि सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वह जन्मती है। यही कारण है कि आत्मनिरीक्षण, आत्मशुद्धि और दूसरों की अच्छाइयों को सम्मान देना, व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य हैं। दुर्भाग्यवश, सामान्य व्यक्ति दूसरों की ओर अंगुली उठाते हुए यह भूल जाता है कि स्वयं के भीतर भी सुधार की आवश्यकता है। यह भी एक प्रकार का पलायन है – जहाँ वह अपने दोषों से बचकर दूसरों के दोषों को बड़ा करके अपने आत्म-सम्मान का झूठा निर्माण करता है। लेकिन यह भावना उसे कभी स्थायी संतोष नहीं देती। उल्टे उसके भीतर असंतोष, कटुता और अवसाद की जड़ें गहराती जाती हैं। जो व्यक्ति साहसपूर्वक अपनी कमियों को स्वीकार करता है, वही सही अर्थों में विकास की दिशा में बढ़ता है। इसलिए आवश्यक है कि हम ईर्ष्या, परनिंदा और अहंकार जैसे दुष्प्रवृत्तियों से दूर रहकर आत्मनिरीक्षण का मार्ग अपनाएँ और दूसरों के गुणों को भी खुले मन से स्वीकार करना सीखें।
प्रश्नावली:
प्रश्न 1: लेखक के अनुसार ईर्ष्या किस प्रकार का प्रभाव डालती है? (1 अंक)
(1) दूसरों को नुकसान पहुँचाती है
(2) स्वयं को पहले जलाती है
(3) समाज को आगे बढ़ाती है
(4) व्यक्ति को साहसी बनाती है
विकल्प:
(क) केवल 1 और 2
(ख) केवल 2
(ग) केवल 3 और 4
(घ) केवल 1 और 3
प्रश्न 2: आत्मनिरीक्षण न करने वाला व्यक्ति क्या करता है? (1 अंक)
(क) अपनी कमियों पर ध्यान देता है
(ख) दूसरों की अच्छाइयों को बढ़ाता है
(ग) दूसरों के दोषों को बढ़ा-चढ़ाकर देखता है
(घ) आत्म-विकास करता है
प्रश्न 3: Assertion (A) और Reason (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। (1 अंक)
Assertion (A): जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार करता है, वही सही विकास करता है। (1 अंक)
Reason (R): क्योंकि आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति में संतुलन और सकारात्मकता आती है।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है परंतु R गलत है।
(घ) A गलत है परंतु R सही है।
प्रश्न 4: परनिंदा को लेखक ने किस प्रकार का व्यवहार बताया है और उसका क्या परिणाम होता है? (2 अंक)
प्रश्न 5: लेखक के अनुसार आत्म-सम्मान का झूठा निर्माण व्यक्ति को किस मानसिक स्थिति की ओर ले जाता है? (2 अंक)
उत्तरकुंजी:
प्रश्न 1: (ख) केवल 2
प्रश्न 2: (ग) दूसरों के दोषों को बढ़ा-चढ़ाकर देखता है
प्रश्न 3: (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
प्रश्न 4 (उत्तर): लेखक के अनुसार परनिंदा एक पाप है और यह प्रवृत्ति व्यक्ति की शांति, संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देती है। यह दूसरों को नहीं, बल्कि स्वयं को ही सबसे अधिक हानि पहुँचाती है।
प्रश्न 5 (उत्तर): लेखक के अनुसार झूठे आत्म-सम्मान के कारण व्यक्ति में असंतोष, कटुता और अवसाद की भावना गहराती है, जिससे वह आंतरिक रूप से कमजोर और दुखी हो जाता है।
- मानव जीवन में कुछ महान कर दिखाने की जो आकांक्षा जन्म लेती है, उसे ही महत्वाकांक्षा कहा जाता है। यह महत्वाकांक्षा मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उसे आलस्य और जड़ता से बाहर निकालती है और उसे उपलब्धियों की ओर ले जाती है। किंतु यही महत्वाकांक्षा जब दूसरों से आगे निकलने की प्रतियोगिता में बदल जाती है तो वह प्रतिद्वंद्विता का रूप ले लेती है। यह प्रतिस्पर्धा एक ओर तो समाज में प्रगति और नवीनता को जन्म देती है, वहीं दूसरी ओर दूसरों को पीछे छोड़ने की निष्ठुर प्रवृत्ति को भी जन्म देती है। मनुष्य जब अपने जीवन में ऊँचाइयाँ छूना चाहता है, तो वह अनजाने में दूसरों से आगे निकलने और उनकी स्थिति को कमतर करने की भावना को भी पोषित करता है। यह भावना ही महत्वाकांक्षा को शक्ति देती है लेकिन साथ ही दूसरों के प्रति कठोरता और सहानुभूति की कमी भी लाती है। यदि इस प्रवृत्ति का विश्लेषण सहृदय होकर किया जाए तो स्पष्ट होता है कि यह एक प्रकार की निर्ममता है, एक ऐसी मानसिकता जो केवल स्वयं के लक्ष्य को सर्वोपरि मानती है और बाकी सबको गौण। परंतु यह भी सत्य है कि जब तक मनुष्य में यह तीव्र आकांक्षा और कठोर आत्मसंकल्प नहीं होता, वह किसी भी महान उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि कभी-कभी निष्ठुरता भी सफलता के मार्ग की अनिवार्य शर्त बन जाती है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम पूरी तरह से संवेदनहीन हो जाएँ। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी महत्वाकांक्षा को सकारात्मक दिशा दें, ताकि वह केवल स्वहित नहीं बल्कि समष्टिगत हित की ओर भी अग्रसर हो। यदि हम बिना दूसरों को गिराए अपने प्रयासों से आगे बढ़ें तो यह वास्तविक महानता होगी। मनुष्य के लिए यह एक चुनौती है कि वह महत्वाकांक्षा की ऊर्जा को स्वार्थ की आग में न झोंके, बल्कि सेवा, सृजन और सहयोग की भावना के साथ उसे उपयोग में लाए। तभी वह उस महानता को पा सकेगा जो केवल ऊँचाई नहीं, बल्कि ऊँचाई के साथ गरिमा और उदारता की भी प्रतीक हो।
प्रश्नावली:
प्रश्न 1: लेखक के अनुसार महत्वाकांक्षा कब प्रतिद्वंद्विता में बदल जाती है? (1 अंक)
(1) जब व्यक्ति सहयोग की भावना से कार्य करता है
(2) जब वह दूसरों से आगे निकलने की तीव्र इच्छा रखता है
(3) जब उसमें सेवा की भावना होती है
(4) जब वह लक्ष्य भूलकर भटक जाता है
विकल्प:
(क) केवल 1 और 3
(ख) केवल 2
(ग) केवल 3 और 4
(घ) केवल 2 और 4
प्रश्न 2: लेखक के अनुसार सच्ची महानता किसमें निहित है? (1 अंक)
(क) दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने में
(ख) केवल स्वहित की पूर्ति में
(ग) बिना दूसरों को हानि पहुँचाए आगे बढ़ने में
(घ) निष्ठुरता और ईर्ष्या में
प्रश्न 3: Assertion (A) और Reason (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। (1 अंक)
Assertion (A): व्यक्ति की महत्वाकांक्षा उसे कार्यशील और सफल बनाती है। (1 अंक)
Reason (R): क्योंकि यह भावना उसे आलस्य और निष्क्रियता से मुक्त करती है।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है परंतु R गलत है।
(घ) A गलत है परंतु R सही है।
प्रश्न 4: लेखक ने महत्वाकांक्षा के किन दोनों पक्षों को प्रस्तुत किया है? स्पष्ट कीजिए। (2 अंक)
प्रश्न 5: लेखक के अनुसार हम महत्वाकांक्षा की ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग कैसे कर सकते हैं? (2 अंक)
उत्तरकुंजी:
प्रश्न 1: (ख) केवल 2
प्रश्न 2: (ग) बिना दूसरों को हानि पहुँचाए आगे बढ़ने में
प्रश्न 3: (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
प्रश्न 4 (उत्तर): लेखक ने महत्वाकांक्षा के दो पक्ष बताए हैं—एक ओर यह व्यक्ति को प्रगति और उपलब्धि की ओर ले जाती है, वहीं दूसरी ओर यह दूसरों को पीछे छोड़ने की निष्ठुर प्रवृत्ति को जन्म देती है।
प्रश्न 5 (उत्तर): लेखक के अनुसार हम अपनी महत्वाकांक्षा की ऊर्जा को सेवा, सृजन और सहयोग की भावना के साथ प्रयोग करके उसे सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं, जिससे समाज और व्यक्ति दोनों लाभान्वित हो सकें।
- यह एक सर्वविदित तथ्य है कि मानवीय गुणों का अधिकतम विकास विपरीत परिस्थितियों में ही होता है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक के जीवन में इस सत्य के उदाहरण सहज ही मिल जाते हैं। जब मनुष्य कठिनाइयों, संघर्षों और विफलताओं से जूझता है, तब उसके भीतर की आत्मशक्ति जाग्रत होती है। कष्ट और पीड़ा जहाँ एक ओर उसकी अंतःवृत्तियों का परिशोधन करते हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें ऐसी मानसिक दृढ़ता उत्पन्न करते हैं जो उसे जीवन की हर परीक्षा में सफल होने की शक्ति प्रदान करती है। जैसे अग्नि में तपकर सोना खरा होता है, वैसे ही कठिनाइयों से जूझकर मनुष्य खरा और सशक्त बनता है। जब मनुष्य बार-बार आपत्तियों से टकराता है, तो उनमें जूझने की शक्ति का विकास होता है। धीरे-धीरे यही कठिनाइयाँ उसके लिए सामान्य प्रतीत होने लगती हैं। उसके भीतर विपत्तियों से डरने की बजाय उनसे लड़कर आगे बढ़ने की भावना जागती है। इस मानसिक बल के साथ-साथ शारीरिक बल की आवश्यकता भी जीवन में उतनी ही महत्त्वपूर्ण है। लेखक का मानना है कि जैसे मानसिक दृढ़ता कष्टों से आती है, वैसे ही शारीरिक दृढ़ता श्रम से आती है। निरंतर श्रम करने वाला व्यक्ति न केवल बलिष्ठ होता है बल्कि उसका शरीर भी लोहे जैसा कठोर और सहनशील बन जाता है। शारीरिक श्रम व्यक्ति में सहनशक्ति और कार्यनिष्ठा के गुण विकसित करता है। इसी प्रकार मानसिक संघर्ष, आत्मबल, आत्मसंयम और लक्ष्य-निर्धारण जैसे चारित्रिक गुणों को जन्म देता है। प्रसिद्ध शायर की यह पंक्ति – “मुश्किलें इतनी पड़ीं मुझ पर कि आसाँ हो गईं” – इसी सच्चाई की गूंज है। वह बताता है कि जब कठिनाइयाँ जीवन में बार-बार आती हैं, तो मनुष्य उन्हें झेलने का आदी हो जाता है और फिर वे कठिनाइयाँ कठिन नहीं लगतीं। अंततः कहा जा सकता है कि कष्ट और परिश्रम दोनों ही व्यक्ति को जीवन की कठोर सच्चाइयों के सामने दृढ़ बनाते हैं और वह जीवन की चुनौतियों से घबराने की बजाय उनका डटकर सामना करना सीखता है।
प्रश्नावली:
प्रश्न 1: लेखक के अनुसार कठिनाइयाँ व्यक्ति में किस प्रकार की भावना उत्पन्न करती हैं? (1 अंक)
(1) डर और असहायता
(2) पलायन और क्रोध
(3) लड़कर आगे बढ़ने की भावना
(4) सफलता का अहंकार
विकल्प:
(क) केवल 1 और 2
(ख) केवल 3
(ग) केवल 2 और 3
(घ) केवल 3 और 4
प्रश्न 2: “मानसिक बल” और “शारीरिक बल” के संबंध में लेखक का क्या मत है? (1 अंक)
(क) दोनों जीवन में समान रूप से आवश्यक हैं
(ख) केवल मानसिक बल की आवश्यकता है
(ग) केवल शारीरिक बल से सफलता मिलती है
(घ) मानसिक बल कठिनाइयों से नहीं आता
प्रश्न 3: Assertion (A) और Reason (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। (1 अंक)
Assertion (A): परिश्रम से व्यक्ति की शारीरिक सहनशक्ति बढ़ती है। (1 अंक)
Reason (R): क्योंकि निरंतर श्रम करने से शरीर लोहे जैसा कठोर बनता है।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है परंतु R गलत है।
(घ) A गलत है परंतु R सही है।
प्रश्न 4: लेखक ने किस प्रकार यह सिद्ध किया है कि कष्ट और पीड़ा व्यक्ति को जीवन के प्रति सशक्त बनाते हैं? (2 अंक)
प्रश्न 5: “मुश्किलें इतनी पड़ीं मुझ पर कि आसाँ हो गईं” – इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? (2 अंक)
उत्तरकुंजी:
प्रश्न 1: (ख) केवल 3
प्रश्न 2: (क) दोनों जीवन में समान रूप से आवश्यक हैं
प्रश्न 3: (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
प्रश्न 4 (उत्तर): लेखक के अनुसार जब व्यक्ति बार-बार कठिनाइयों का सामना करता है तो उसके भीतर आत्मबल और साहस का विकास होता है। वह विपत्तियों से डरने की बजाय उनका सामना करना सीखता है, जिससे उसका चरित्र और सोच मजबूत बनती है।
प्रश्न 5 (उत्तर): इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह संदेश देता है कि जब जीवन में बार-बार कठिनाइयाँ आती हैं, तो व्यक्ति उन्हें झेलने का अभ्यास कर लेता है और वे कठिनाइयाँ उसे उतनी कठिन नहीं प्रतीत होतीं, जितनी पहले होती थीं।
- हमारे भारत का किसान इस अर्थ में सच्चा देशभक्त है कि वह न केवल अपने परिवार का बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र का भरण-पोषण करता है। वह दिन-रात खेतों में मेहनत कर अन्न उपजाता है जिससे देश की खाद्य सुरक्षा बनी रहती है। विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रगति ने कृषि के क्षेत्र को भी नया रूप प्रदान किया है। आज हमारे कृषि वैज्ञानिक बेहतर किस्म के बीजों, रासायनिक खादों और अधिक उत्पादन देने वाली तकनीकों के विकास में सतत प्रयासरत हैं। इस वैज्ञानिक योगदान का सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है, जिससे वे कम समय में अधिक मात्रा में उत्पादन कर पा रहे हैं। आधुनिक यंत्रों और औजारों की सहायता से अब खेती एक परंपरागत कार्य न रहकर एक संगठित और लाभकारी उद्योग का स्वरूप ले चुकी है। सरकार ने भी कृषि को प्राथमिकता देते हुए अनेक योजनाएँ चलाई हैं जिनके अंतर्गत किसानों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण, बीज, खाद और मशीनों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, समर्थन मूल्य योजना तथा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार भी किया गया है। भारत जैसे विशाल और कृषि-प्रधान देश में यह आवश्यक है कि कृषि कार्य को आधुनिक तकनीकों और योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो और किसानों की आमदनी बढ़े। आज का किसान बदलते परिवेश के साथ कदम मिलाकर चल रहा है। वह वैज्ञानिकों और सरकार के सहयोग से अपनी खेती को आधुनिक रूप देने में सफल हो रहा है। यही कारण है कि अब कृषि को केवल एक परंपरा न मानकर उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है। जब किसान सक्षम होगा, तो न केवल वह स्वयं समृद्ध होगा, बल्कि देश की आर्थिक रीढ़ भी और मजबूत बनेगी। इस प्रकार आधुनिक कृषि, तकनीक और सरकारी योजनाओं के मेल से आज का भारतीय किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और भारत की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
प्रश्नावली:
प्रश्न 1: भारतीय किसान को सच्चा देशभक्त क्यों कहा गया है? (1 अंक)
(1) क्योंकि वह परंपराओं को निभाता है
(2) क्योंकि वह विज्ञान का उपयोग करता है
(3) क्योंकि वह राष्ट्र का भरण-पोषण करता है
(4) क्योंकि वह आधुनिक मशीनें चलाता है
विकल्प:
(क) केवल 1
(ख) केवल 2 और 4
(ग) केवल 3
(घ) केवल 1 और 3
प्रश्न 2: सरकार द्वारा किसानों को किस प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है? (1 अंक)
(क) सस्ते ऋण
(ख) मुफ्त शिक्षा
(ग) समर्थन मूल्य योजना
(घ) सिंचाई सुविधाएँ
प्रश्न 3: Assertion (A) और Reason (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। (1 अंक)
Assertion (A): आज का भारतीय किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। (1 अंक)
Reason (R): क्योंकि वह वैज्ञानिकों और सरकार के सहयोग से आधुनिक खेती कर रहा है।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है परंतु R गलत है।
(घ) A गलत है परंतु R सही है।
प्रश्न 4: आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से खेती में कौन-से दो परिवर्तन आए हैं? स्पष्ट कीजिए। (2 अंक)
प्रश्न 5: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कौन-कौन-सी योजनाएँ कार्यरत हैं? संक्षेप में लिखिए। (2 अंक)
उत्तरकुंजी:
प्रश्न 1: (ग) केवल 3
प्रश्न 2: (ख) मुफ्त शिक्षा
प्रश्न 3: (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
प्रश्न 4 (उत्तर): आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से अब खेती परंपरागत कार्य न रहकर संगठित और लाभकारी उद्योग बन गई है। किसान अब कम समय में अधिक उत्पादन कर पा रहे हैं।
प्रश्न 5 (उत्तर): किसानों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण, बीज, खाद और यंत्र उपलब्ध कराना; समर्थन मूल्य योजना लागू करना; प्रशिक्षण कार्यक्रम और सिंचाई सुविधाएँ बढ़ाना—ये सभी योजनाएँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रही हैं।
- यह संसार एक महान शिक्षालय है जहाँ प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक दृश्य और प्रत्येक अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। एक दिन मैं तेज़ धूप में खुले मैदान से होकर गुजर रहा था। चारों ओर विशाल वृक्ष अपनी हरीतिमा के साथ खड़े थे। धूप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि शरीर तपने लगा, लेकिन ये वृक्ष बिना किसी चिंता के शांति से खड़े थे। मैं सोचने लगा—जब ऊपर से इतनी तीव्र धूप पड़ रही है, तब भी ये वृक्ष इतने हरे-भरे और ताजे कैसे दिख रहे हैं? तभी मेरे मन में यह विचार कौंधा कि इन वृक्षों की जड़ें बहुत गहराई तक पृथ्वी के भीतर जाती हैं, जहाँ से उन्हें निरंतर जल प्राप्त होता रहता है। ऊपर से सूर्य की तपिश और भीतर से जड़ों को मिलने वाला जल—इन्हीं दोनों के संतुलन से ये वृक्ष जीवन और हरियाली से भरपूर हैं। मुझे लगा कि यही तो जीवन का रहस्य है। यदि मनुष्य भी भीतर से भक्ति, श्रद्धा, आत्मिक स्थिरता और आस्था से पोषित हो तथा बाहर से कठोर परिश्रम, संघर्ष और तपश्चर्या को सहने का सामर्थ्य रखे, तो उसका जीवन भी वृक्षों की भाँति फलदायक और हरा-भरा हो सकता है। परंतु समस्या यह है कि हम परिश्रम को ज्ञान की दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि उसे एक बोझ मानकर केवल दुःख समझते हैं। यही कारण है कि मनुष्य जीवन में आरोग्य, शांति और आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है। वृक्षों से प्रेरणा लेकर यदि हम भी भीतर की गहराई में उतरकर संयम, विवेक और आस्था का स्रोत खोज लें, तो जीवन की तपती धूप भी हमें झुलसा नहीं सकेगी। यही संतुलन बाहरी संघर्ष और भीतरी शांति का सामंजस्य है, जो मानव जीवन को सार्थक बनाता है।
प्रश्नावली:
प्रश्न 1: वृक्ष तीव्र धूप में भी हरे-भरे क्यों रहते हैं? (1 अंक)
(1) क्योंकि उनकी शाखाएँ बड़ी होती हैं
(2) क्योंकि उनकी जड़ें गहराई में जल प्राप्त करती हैं
(3) क्योंकि वे छाया में रहते हैं
(4) क्योंकि वे सूर्य की ऊर्जा से ताकत पाते हैं
विकल्प:
(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) केवल 2 और 4
(घ) केवल 1 और 3
प्रश्न 2: लेखक के अनुसार मनुष्य क्यों आत्मिक शांति से वंचित रह जाता है? (1 अंक)
(क) क्योंकि वह परिश्रम से भागता है
(ख) क्योंकि वह आस्था में विश्वास नहीं करता
(ग) क्योंकि वह केवल सफलता चाहता है
(घ) क्योंकि वह परिश्रम को दुःख समझता है
प्रश्न 3: Assertion (A) और Reason (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। (1 अंक)
Assertion (A): मनुष्य यदि भीतर से श्रद्धा और संयम से पोषित हो तो उसका जीवन भी वृक्षों की भाँति फलदायक हो सकता है। (1 अंक)
Reason (R): क्योंकि संयम और आस्था मनुष्य को बाहरी संघर्ष झेलने की शक्ति प्रदान करते हैं।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है परंतु R गलत है।
(घ) A गलत है परंतु R सही है।
प्रश्न 4: लेखक ने वृक्षों के माध्यम से जीवन का कौन-सा रहस्य स्पष्ट किया है? संक्षेप में लिखिए। (2 अंक)
प्रश्न 5: जीवन में बाहरी संघर्ष और भीतरी शांति के सामंजस्य का क्या महत्व है? उत्तर दीजिए। (2 अंक)
उत्तरकुंजी:
प्रश्न 1: (ख) केवल 2
प्रश्न 2: (घ) क्योंकि वह परिश्रम को दुःख समझता है
प्रश्न 3: (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
प्रश्न 4 (उत्तर): लेखक ने बताया है कि वृक्ष धूप सहने के बावजूद हरे-भरे रहते हैं क्योंकि उनकी जड़ें गहराई में जल लेती हैं। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी तभी फलदायक होता है जब वह भीतर से संयम और आस्था से पोषित हो।
प्रश्न 5 (उत्तर): बाहरी संघर्ष और भीतरी शांति का सामंजस्य जीवन को संतुलित और सार्थक बनाता है। इससे व्यक्ति तनावों को झेलने में सक्षम होता है और आंतरिक रूप से सशक्त बना रहता है।
- हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस युग में भक्ति की भावना से ओतप्रोत साहित्य की अत्यंत समृद्ध परंपरा विकसित हुई। इस युग के कवियों में महाकवि सूरदास, तुलसीदास और कबीर प्रमुख हैं। इनकी कविताएँ आज भी जनमानस के कंठहार बनी हुई हैं। जहाँ सूरदास ने श्रीकृष्ण को केंद्र बनाकर सगुण भक्ति की अभिव्यक्ति की, वहीं तुलसीदास ने श्रीराम को अपना आराध्य माना। कबीर निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, जिनकी रचनाओं में सामाजिक विकृतियों पर तीखा प्रहार मिलता है। परंतु भक्तिकाल के कवियों में सूरदास का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। उनकी रचनाओं में जो सरसता, माधुर्य, कोमल भावनाएँ और काव्यात्मक लालित्य है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। उनकी कविताएँ अलौकिक रस की अनुभूति कराती हैं, विशेषकर बालकृष्ण की लीलाओं का चित्रण भाव-विभोर कर देता है। सूरदास का जन्म 1478 ई. के आसपास माना जाता है। कुछ मतों के अनुसार उनका जन्म रुनकता (मथुरा-आगरा मार्ग) में हुआ था, जबकि अन्य के अनुसार दिल्ली के समीप स्थित गाँव ‘सीही’ को उनका जन्मस्थान माना जाता है। वे सारस्वत ब्राह्मण थे और उनके पिता का नाम रामदास था। ‘साहित्य लहरी’ के एक पद से ज्ञात होता है कि वे ब्रह्मभट्ट और चंदबरदाई के वंशज थे। सूरदास जन्म से ही नेत्रहीन थे, किंतु उनकी काव्य-दृष्टि अत्यंत प्रखर थी। उनके गीतों से प्रभावित होकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उन्हें दीक्षा दी और ‘सूरसागर’ की रचना का प्रेरणास्रोत भी वही बने। ‘सूरसागर’ के अतिरिक्त ‘साहित्य लहरी’ और ‘सूरसारावली’ भी उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने जब ‘अष्टछाप’ नामक गायक-कवियों का समूह गठित किया, तो उसमें सूरदास का स्थान सर्वोपरि था। सूरदास ने जिस माधुर्य और भाव-गहराई से श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओं, वात्सल्य और श्रृंगार को प्रस्तुत किया, वह उन्हें भक्तिकाल का अद्वितीय रचनाकार बनाता है।
प्रश्नावली
प्रश्न 1: सूरदास को भक्तिकाल का अद्वितीय रचनाकार क्यों माना जाता है? (1 अंक)
(क) क्योंकि वे अष्टछाप में शामिल थे
(ख) क्योंकि वे नेत्रहीन होने के बावजूद प्रभावशाली कवि थे
(ग) क्योंकि उन्होंने श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओं को अत्यंत माधुर्य से चित्रित किया
(घ) क्योंकि उनका जन्म रुनकता में हुआ था
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? (1 अंक)
(क) सूरदास ने सगुण भक्ति पर आधारित काव्य लिखा
(ख) तुलसीदास निर्गुण भक्ति के कवि थे
(ग) कबीर ने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया
(घ) ‘साहित्य लहरी’ सूरदास का ग्रंथ है
प्रश्न 3: Assertion (A) और Reason (R) को पढ़कर उत्तर चुनिए: (1 अंक)
Assertion (A): सूरदास का स्थान अष्टछाप में सर्वोपरि था। (1 अंक)
Reason (R): क्योंकि उन्होंने ‘सूरसागर’ नामक ग्रंथ की रचना की थी।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है परंतु R गलत है।
(घ) A गलत है परंतु R सही है।
प्रश्न 4: सूरदास की रचनाओं की कौन-सी विशेषताएँ उन्हें अन्य कवियों से विशिष्ट बनाती हैं? स्पष्ट कीजिए। (2 अंक)
प्रश्न 5: सूरदास के जीवन और साहित्यिक योगदान के संदर्भ में ‘सूरसागर’ और अष्टछाप का क्या महत्व है? (2 अंक)
उत्तरकुंजी:
प्रश्न 1: (ग) क्योंकि उन्होंने श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओं को अत्यंत माधुर्य से चित्रित किया
प्रश्न 2: (ख) तुलसीदास निर्गुण भक्ति के कवि थे
प्रश्न 3: (ख) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है
प्रश्न 4 (उत्तर): सूरदास की रचनाओं में कोमल भावनाओं, रसपूर्ण वर्णन और बालकृष्ण की लीलाओं का चित्रण अत्यंत सरस रूप में हुआ है। उनकी काव्य-शैली में माधुर्य और भाव-गंभीरता है, जो उन्हें अन्य कवियों से अलग करती है।
प्रश्न 5 (उत्तर): ‘सूरसागर’ सूरदास की प्रसिद्ध काव्यकृति है जिसमें श्रीकृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण है। ‘अष्टछाप’ में उनका सर्वोपरि स्थान उन्हें गायक-कवि रूप में प्रतिष्ठित करता है और उनके योगदान को उच्चतम स्तर पर स्थापित करता है।
- आत्मनिर्भरता का अर्थ है—अपने कार्यों में दूसरों पर निर्भर न रहकर स्वयं के बलबूते पर उन्हें संपन्न करना। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही वास्तव में आत्मविश्वास से भरपूर होता है। वह अपने कार्यों के लिए किसी अन्य की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि स्वयं आगे बढ़कर जिम्मेदारियाँ निभाता है। राष्ट्रीय स्तर पर आत्मनिर्भरता का तात्पर्य यह है कि कोई राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहरी देशों पर निर्भर न रहकर अपने संसाधनों के सहारे उन्हें पूरा करे। आत्मनिर्भरता स्वावलंबन की आधारशिला है और स्वावलंबन जीवन में सफलता प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। यह न केवल व्यक्तित्व विकास का, बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति का भी मूल मंत्र है। आत्मनिर्भरता का महत्व हमें प्रकृति में अनेक उदाहरणों से स्पष्ट होता है। जब एक शिशु छोटा होता है तो वह पूर्णतः अपनी माता पर निर्भर रहता है, किंतु जैसे-जैसे वह बड़ा होता है, वह स्वयं खाना, चलना और खेलना सीखता है, और यह आत्मनिर्भरता उसे आनंद देती है। यह स्वावलंबन का ही प्रतीक है। इसी प्रकार पेड़-पौधे भी बिना किसी सहारे के सूर्य से प्रकाश, धरती से जल और खनिज लेकर स्वयं बढ़ते हैं। पशु-पक्षी भी अपना भोजन स्वयं ढूंढ़ते हैं। चींटी जैसा छोटा जीव भी स्वावलंबन की महत्ता को समझता है और अपने भोजन के लिए सतत परिश्रम करता है। आत्मनिर्भरता केवल एक गुण नहीं, बल्कि जीवन जीने की श्रेष्ठ पद्धति है। यह जीवन को कर्मशील, स्वाभिमानी और दृढ़ बनाती है। आत्मनिर्भरता से ही व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता आती है और वह जीवन की कठिनाइयों से बिना डरे जूझ पाता है। यह गुण उसे कभी निराश नहीं होने देता। आत्मनिर्भर व्यक्ति समाज में उदाहरण बनता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में आत्मनिर्भरता को अपनाएँ और अपने आत्मविश्वास को जाग्रत करके उसे दृढ़ बनाएं, ताकि हम व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकें।
प्रश्नावली
प्रश्न 1: आत्मनिर्भरता से व्यक्ति में कौन-सा गुण विकसित होता है? (1 अंक)
(क) ईर्ष्या
(ख) आत्मविश्वास
(ग) निर्भरता
(घ) कठोरता
प्रश्न 2: निम्न में से कौन-सी बात आत्मनिर्भरता के लक्षणों में नहीं आती है? (1 अंक)
(क) कठिनाइयों से जूझने की क्षमता
(ख) स्वाभिमान और कर्मशीलता
(ग) दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करना
(घ) स्वयं निर्णय लेने की शक्ति
प्रश्न 3: Assertion (A) और Reason (R) को पढ़कर उत्तर चुनिए: (1 अंक)
Assertion (A): आत्मनिर्भर व्यक्ति समाज में दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। (1 अंक)
Reason (R): क्योंकि आत्मनिर्भरता व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से डरने से रोकती है।
विकल्प:
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है परंतु R गलत है।
(घ) A गलत है परंतु R सही है।
प्रश्न 4: प्रकृति से आत्मनिर्भरता के कौन-कौन से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं? स्पष्ट कीजिए। (2 अंक)
प्रश्न 5: आत्मनिर्भरता का समाज और राष्ट्र के स्तर पर क्या महत्व है? स्पष्ट कीजिए। (2 अंक)
उत्तरकुंजी:
प्रश्न 1: (ख) आत्मविश्वास
प्रश्न 2: (ग) दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करना
प्रश्न 3: (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
प्रश्न 4 (उत्तर): प्रकृति में शिशु धीरे-धीरे स्वयं चलना, खाना और खेलना सीखता है; पेड़-पौधे अपने संसाधनों से बढ़ते हैं; पशु-पक्षी और चींटी जैसे जीव अपना भोजन स्वयं ढूंढते हैं। ये सभी आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं।
प्रश्न 5 (उत्तर): यदि राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा तो वह बाहरी सहायता के बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा। यह समाज की उन्नति, संसाधनों के सही उपयोग और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है।
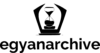
Thanks for your help
Welcome sir.
Very Good Bestest I can’t find any information missing in this
Thanks
Keep it up
Exactly it should be practiced
आपके शुभ शब्दों और हमारी साइट पर आने के लिए हार्दिक धन्यवाद। यह जानकर खुशी हुई कि आपको हमारी सामग्री उपयोगी और पूर्ण लगी। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए प्रेरणा है। यदि भविष्य में भी आपको किसी प्रकार की और जानकारी या सहायता की आवश्यकता लगे तो निःसंकोच हमें बताइए।