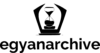कक्षा – 11 अपठित गद्यांश (Unseen Prose Passages)
‘अपठित’ यह शब्द ‘अ’ उपसर्ग, ‘पठ्’ धातु और ‘इत’ प्रत्यय से मिलकर बना है। ‘अपठित’ शब्द का अर्थ है- जो कभी पढ़ा न गया हो। अर्थात अपठित गद्याश वे गद्यांश हैं जिनको छात्रों ने पहले कभी अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ा नहीं है। अपठित गद्यांश देकर उस पर भाव-बांध संबंधी प्रश्न पूछे जाते है। इन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को उसी गद्यांश के आधार पर देने होते हैं। उत्तर देते समय यह कोशिश होनी चाहिए कि उत्तर में गद्यांश के वाक्यों को जैसा का तैसा न उतारा जाए बल्कि उसमें कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए।
(Download 11 Hindi A & B papers in word format – Click Here)
अपठित गद्यांश का उद्देश्य
मूल्यांकन हेतु अपठित गद्यांश दिए जाने का उद्देश्य है- छात्रों के भाषा-बोध का पता लगाना। अर्थात यह जानना कि छात्र उस गद्द्याश की भाषा को समझते हैं या नहीं। साथ ही इससे उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का भी पता चल जाता है।
अपठित गद्यांश हल करते समय ध्यान देने योग्य बाते-
• दिए गए गद्यांश का एक-दो बार मौन वाचन करें तथा उसे समझने का प्रयास करें।
• तदुपरांत प्रश्नों को अलग-अलग पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के संभावित उत्तर को गद्यांश में रेखांकित करें। जब प्रश्नों के उत्तर लिखना प्रारंभ करें तो लेखक द्वारा कही गई बात को सरल एवं स्पष्ट भाषा में छोटे-छोटे वाक्यों में व्यक्त करें।
• यदि शीर्षक देना हो, तो किसी रफ़ कागज पर सोचकर दो-तीन शीर्षक लिख लें। फिर उनमें से जो सबसे अधिक उपयुक्त लगे उसे उत्तर के रूप में लिखें। यदि प्रश्नों का प्रारूप बहुविकल्पीय है तो सारे विकल्पों को ध्यान से पढ़कर सर्वाधिक उचित विकल्प पर निशान लगाइए।
कक्षा 11 अपठित गद्यांश के उदाहरण (नए पाठ्यक्रम विनिर्देशन के अनुसार)
अपठित गद्यांश
- पर्यावरण का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल हमें जीवन के लिए आवश्यक वायु, जल और भूमि प्रदान करता है, बल्कि समस्त जैविक और अजैविक घटकों के बीच एक संतुलन भी बनाए रखता है। आधुनिक सभ्यता की बढ़ती आवश्यकताओं ने पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, उद्योगों की स्थापना और वाहनों की वृद्धि से प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। यह प्रदूषण न केवल मनुष्य के लिए बल्कि सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक है। आज स्थिति यह है कि वायु में विषैले गैसों की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जल स्रोत विषाक्त हो रहे हैं, और भूमि में भी रासायनिक अपशिष्ट मिलकर उसकी उर्वरता को कम कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, अनेक बीमारियाँ जन्म ले रही हैं और प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति भी बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। सरकार और विभिन्न संस्थाएँ इस दिशा में अनेक कदम उठा रही हैं। वृक्षारोपण, प्लास्टिक पर रोक, स्वच्छता अभियान, पुनर्चक्रण जैसी गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं, किंतु जब तक प्रत्येक नागरिक पर्यावरण संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा, तब तक कोई भी योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। पर्यावरण की रक्षा केवल एक नीति नहीं, बल्कि जीवन शैली बननी चाहिए। यदि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य चाहिए, तो हमें आज ही से पर्यावरण के प्रति सजग होना पड़ेगा।
प्रश्न –
(i) आधुनिक जीवनशैली ने पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित किया है? (1)
(क) शुद्ध किया है।
(ख) संतुलन बढ़ाया है।
(ग) स्वच्छ बनाया है।
(घ) प्रदूषित किया है।
(ii) कथन (A): प्लास्टिक पर रोक पर्यावरण रक्षा की दिशा में उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण कदम है। (1)
कारण (R): प्लास्टिक नष्ट न होने वाली सामग्री है जो भूमि व जल को प्रदूषित करती है।
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) पर्यावरण संरक्षण की सबसे आवश्यक शर्त क्या है? (1)
(क) अधिक उद्योग लगाना।
(ख) केवल सरकार पर निर्भर रहना।
(ग) प्रत्येक नागरिक की भागीदारी।
(घ) केवल योजना बनाना।
(iv) प्रदूषण के मुख्य कारणों में क्या सम्मिलित नहीं है? (1)
(क) वनों की कटाई
(ख) उद्योगों की स्थापना
(ग) पशुपालन
(घ) वाहनों की वृद्धि
(v) ‘पर्यावरण की रक्षा केवल एक नीति नहीं, बल्कि जीवन शैली बननी चाहिए’ – इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) प्रदूषण के बढ़ने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? दो बिंदुओं में उत्तर दीजिए। (2)
(vii) सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए दो प्रयासों का उल्लेख कीजिए। (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (घ) प्रदूषित किया है।
(ii) – (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(iii) – (ग) प्रत्येक नागरिक की भागीदारी।
(iv) – (ग) पशुपालन
(v) – इस कथन का आशय यह है कि पर्यावरण की रक्षा को केवल नियमों और योजनाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे प्रत्येक व्यक्ति की दिनचर्या और व्यवहार में शामिल करना चाहिए, जैसे – प्लास्टिक का प्रयोग कम करना, वृक्ष लगाना, जल और ऊर्जा की बचत करना आदि।
(vi) –
- वायु, जल और भूमि प्रदूषित होने से मनुष्य अनेक बीमारियों का शिकार होता है।
- प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में वृद्धि होती है जो जनजीवन को प्रभावित करती है।
(vii) –
- वृक्षारोपण अभियान का संचालन।
- प्लास्टिक के उपयोग पर रोक और स्वच्छता अभियान की शुरुआत।
- भारतीय लोककलाएँ और हस्तशिल्प देश की सांस्कृतिक विविधता और कलात्मक परंपरा का प्रतीक हैं। ये कलाएँ केवल सौंदर्य की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि जनजीवन से जुड़ी हुई सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक संरचनाओं का भी दर्पण हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट लोककलाएँ होती हैं—राजस्थान की मिट्टी की मूर्तियाँ, मध्यप्रदेश की गोंड चित्रकला, ओडिशा की पट्टचित्र शैली, बंगाल की कालीघाट पेंटिंग, और असम के रेशमी वस्त्र इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इन कलाओं के माध्यम से न केवल कलाकार अपनी सृजनात्मकता प्रकट करते हैं, बल्कि समाज में एक सांस्कृतिक संवाद भी स्थापित होता है। आज जब औद्योगिक उत्पादन और यांत्रिक जीवनशैली ने बाजार को घेर लिया है, तब भी लोककलाओं की प्रासंगिकता बनी हुई है। यह केवल ग्रामीण भारत की स्मृति नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है, जो समय के साथ नए रंग और रूप धारण कर रही है। शहरी क्षेत्रों में भी अब हस्तशिल्प मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से इन कलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कलाकारों को प्रशिक्षण, ऋण और विपणन सहायता दी जा रही है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से इन उत्पादों को अब वैश्विक पहचान भी मिलने लगी है। परंतु इसके बावजूद कई पारंपरिक कलाएँ विलुप्ति के कगार पर हैं, क्योंकि नई पीढ़ी का रुझान आधुनिक करियर की ओर बढ़ गया है। यदि इन लोककलाओं को संरक्षित करना है तो इन्हें शिक्षा, पर्यटन और बाजार से जोड़ना आवश्यक होगा, ताकि युवा पीढ़ी इसे केवल एक शौक नहीं, बल्कि एक समर्पित व्यवसाय के रूप में अपनाए। लोककलाएँ न केवल भारतीयता की पहचान हैं, बल्कि सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी हैं, जिसे सुरक्षित रखना हमारा सांझा दायित्व है।
प्रश्न –
(i) भारतीय लोककलाएँ किस बात की प्रतीक मानी गई हैं? (1)
(क) तकनीकी विकास की
(ख) सांस्कृतिक विविधता और कलात्मक परंपरा की
(ग) राजनीतिक चेतना की
(घ) वैज्ञानिक दृष्टिकोण की
(ii) कथन (A): लोककलाओं का संबंध केवल ग्रामीण भारत से है। (1)
कारण (R): शहरी क्षेत्रों में लोककलाओं को कोई स्थान नहीं दिया जाता।
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों गलत हैं।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) गोंड चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? (1)
(क) ओडिशा
(ख) राजस्थान
(ग) असम
(घ) मध्यप्रदेश
(iv) लोककलाओं को संरक्षित करने के लिए कौन-से क्षेत्र से जोड़ने की आवश्यकता है? (1)
(क) खेल और विज्ञान
(ख) शिक्षा, पर्यटन और बाजार
(ग) राजनीति और पत्रकारिता
(घ) वाणिज्य और चिकित्सा
(v) “लोककलाएँ सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं” – इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) लेखक के अनुसार आज की कौन-सी चुनौतियाँ पारंपरिक कलाओं के लिए खड़ी हो रही हैं? (2)
(vii) लेखक ने लोककलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए किन उपायों की चर्चा की है? (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ख) सांस्कृतिक विविधता और कलात्मक परंपरा की
(ii) – (ख) A और R दोनों गलत हैं।
(iii) – (घ) मध्यप्रदेश
(iv) – (ख) शिक्षा, पर्यटन और बाजार
(v) – इस कथन का आशय है कि लोककलाएँ हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती हैं और हमें आत्मनिर्भर बनाती हैं। जब हम अपने ही देश की कलाओं का समर्थन करते हैं, तो यह न केवल हमारी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करता है, बल्कि स्थानीय कलाकारों को आर्थिक स्थिरता भी प्रदान करता है।
(vi) – लेखक के अनुसार आधुनिक युग में नई पीढ़ी का रुझान पारंपरिक कलाओं से हटकर अन्य करियर विकल्पों की ओर बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त, कुछ कलाएँ पर्याप्त संरक्षण और बाज़ार न मिलने के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुँच रही हैं।
(vii) – लेखक ने सुझाव दिया है कि लोककलाओं को शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित किया जाए, पर्यटन से जोड़ा जाए और बाजार उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से इन्हें वैश्विक स्तर पर भी प्रचारित करने की आवश्यकता है।
- भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। इसकी शक्ति केवल मतों की संख्या में नहीं, बल्कि उसमें भाग लेने वाले जागरूक नागरिकों की सक्रियता में है। संविधान ने प्रत्येक नागरिक को मत देने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समान अवसर का अधिकार दिया है। परंतु लोकतंत्र केवल अधिकारों का विषय नहीं है, बल्कि यह कर्तव्यों की पूर्ति से ही सशक्त होता है। आज भी समाज में अनेक ऐसे वर्ग हैं जो मतदान के दिन को छुट्टी के रूप में लेते हैं, न कि राष्ट्रनिर्माण के एक अवसर के रूप में। वहीं कुछ लोग जाति, धर्म, क्षेत्र या व्यक्तिगत लाभ के आधार पर मत देते हैं, जो लोकतंत्र की मूल भावना को आघात पहुँचाता है। एक जागरूक नागरिक न केवल अपने मत का प्रयोग सोच-समझकर करता है, बल्कि वह सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समझता है। स्वच्छता, कर भुगतान, कानून का पालन, पर्यावरण संरक्षण, और दूसरों के अधिकारों का सम्मान – ये सभी ऐसे कार्य हैं जो लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली केवल सरकार बनाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह प्रशासन को जवाबदेह बनाने की एक प्रक्रिया है। आज सूचना का अधिकार, लोकपाल जैसी संस्थाएँ और मीडिया इस प्रक्रिया को गति प्रदान कर रहे हैं। परंतु इन सबके बावजूद जब तक प्रत्येक नागरिक अपने दायित्वों को नहीं समझेगा, तब तक लोकतंत्र केवल एक दिखावटी व्यवस्था बनकर रह जाएगा। अतः आवश्यकता इस बात की है कि लोकतंत्र की शिक्षा केवल पुस्तकों तक न रहे, बल्कि व्यवहार में उतर कर उसे जीवंत बनाए। जब हर नागरिक यह समझेगा कि उसका हर कदम राष्ट्र के भविष्य को आकार दे रहा है, तभी भारत एक सशक्त, न्यायपूर्ण और समानता आधारित लोकतंत्र बन सकेगा।
प्रश्न –
(i) भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति किसमें निहित है? (1)
(क) जनसंख्या में
(ख) कानून में
(ग) जागरूक नागरिकों की भागीदारी में
(घ) चुनाव आयोग में
(ii) कथन (A): लोकतंत्र केवल अधिकारों की व्यवस्था है। (1)
कारण (R): संविधान ने नागरिकों को मत देने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है।
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) निम्न में से कौन-सा कार्य एक उत्तरदायी नागरिक के व्यवहार को दर्शाता है? (1)
(क) चुनावों में भाग न लेना
(ख) केवल अपने लाभ के अनुसार मत देना
(ग) कर भुगतान करना और कानून का पालन करना
(घ) अफवाह फैलाना
(iv) लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सूचना का अधिकार और लोकपाल की क्या भूमिका है? (1)
(क) वे नागरिकों को डराते हैं
(ख) वे सरकार को बदलते हैं
(ग) वे प्रशासन को जवाबदेह बनाते हैं
(घ) वे कानून की व्याख्या करते हैं
(v) “लोकतंत्र केवल अधिकारों का विषय नहीं है, बल्कि यह कर्तव्यों की पूर्ति से ही सशक्त होता है।” – इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) लेखक के अनुसार भारतीय नागरिकों में लोकतंत्र को लेकर क्या प्रमुख समस्याएँ हैं? (2)
(vii) लेखक ने लोकतंत्र को जीवंत और व्यवहारिक बनाने के लिए क्या सुझाव दिया है? (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ग) जागरूक नागरिकों की भागीदारी में
(ii) – (घ) A गलत है, R सही है।
(iii) – (ग) कर भुगतान करना और कानून का पालन करना
(iv) – (ग) वे प्रशासन को जवाबदेह बनाते हैं
(v) – इस कथन का आशय है कि लोकतंत्र केवल अपने अधिकारों की माँग करने से नहीं चलता, बल्कि यह तभी मजबूत होता है जब नागरिक अपने कर्तव्यों जैसे मतदान, कर भुगतान, कानून पालन आदि को भी गंभीरता से निभाते हैं। दोनों का संतुलन लोकतंत्र की नींव है।
(vi) – लेखक के अनुसार कुछ नागरिक लोकतंत्र को केवल छुट्टी या व्यक्तिगत लाभ के अवसर के रूप में देखते हैं। वे जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर मत देते हैं, जिससे लोकतंत्र की निष्पक्षता प्रभावित होती है।
(vii) – लेखक का सुझाव है कि लोकतंत्र की शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि व्यवहार में लाकर उसे जीवन का हिस्सा बनाया जाए। हर नागरिक को यह समझना चाहिए कि उसका प्रत्येक कर्तव्य राष्ट्र के भविष्य को प्रभावित करता है।
- भारतीय रेल केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं, बल्कि देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक धड़कन है। यह न केवल शहरों और गाँवों को आपस में जोड़ती है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन का अनिवार्य अंग बन चुकी है। सुदूर गाँवों से लेकर महानगरों तक, रेल यात्रा आम नागरिक के लिए सुलभ, सस्ती और भरोसेमंद साधन है। यह भारत की विविधता को अपने डिब्बों में समेटे हुए चलती है—भाषाएँ बदलती हैं, खानपान बदलता है, वेशभूषा और रीति-रिवाज बदलते हैं, लेकिन रेल सबको एक डोर में बाँधती है। इसके डिब्बों में व्यापारी, विद्यार्थी, तीर्थयात्री, कामगार और पर्यटक सभी एक साथ सफर करते हैं। रेल न केवल देश के आर्थिक विकास को गति देती है, बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देती है। पर्यटन स्थलों तक रेल की पहुँच से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों का परिवहन, मजदूरों का आवागमन और छात्रों की शिक्षा के लिए आवश्क यात्रा, ये सब रेल के बिना अधूरे हैं। परंतु इतनी बड़ी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना एक बड़ी चुनौती भी है। समय पालन, सफाई, सुरक्षा और तकनीकी उन्नयन जैसे क्षेत्रों में निरंतर सुधार की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में बुलेट ट्रेन, सेमी-हाईस्पीड रेल और डिजिटल टिकटिंग जैसी पहलों ने आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाए हैं। बावजूद इसके, कई क्षेत्रों में भीड़भाड़, देरी, और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। भारतीय रेल की सफलता तभी संभव है जब वह अपने पारंपरिक मूल्यों—सहयोग, सेवा और समर्पण—को आधुनिक तकनीकी सुविधाओं के साथ संतुलित रूप से आगे बढ़ाए। देश की प्रगति की रफ्तार कहीं न कहीं रेल की गति से जुड़ी हुई है।
प्रश्न –
(i) भारतीय रेल को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? (1)
(क) केवल यातायात व्यवस्था
(ख) आर्थिक केंद्र
(ग) सामाजिक और सांस्कृतिक धड़कन
(घ) शहरी सुविधा
(ii) कथन (A): भारतीय रेल भारत की विविधता को एक सूत्र में बाँधती है। (1)
कारण (R): यह केवल महानगरों में ही चलती है।
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों गलत हैं।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) रेल किस प्रकार पर्यटन को प्रोत्साहित करती है? (1)
(क) पर्यटन स्थलों को जोड़कर
(ख) टूर गाइड भेजकर
(ग) हवाई टिकट देकर
(घ) होटल बुक करवा कर
(iv) भारतीय रेल की आधुनिक पहलों में कौन-सी पहल शामिल नहीं है? (1)
(क) बुलेट ट्रेन
(ख) मेट्रो रेल
(ग) डिजिटल टिकटिंग
(घ) सेमी-हाईस्पीड रेल
(v) “भारतीय रेल विविधता में एकता का प्रतीक है।” – इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) लेखक के अनुसार भारतीय रेल किन-किन क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग प्रदान करती है? (2)
(vii) भारतीय रेल को प्रभावी बनाए रखने के लिए किन चुनौतियों का समाधान आवश्यक है? (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ग) सामाजिक और सांस्कृतिक धड़कन
(ii) – (ग) A सही है, R गलत है।
(iii) – (क) पर्यटन स्थलों को जोड़कर
(iv) – (ख) मेट्रो रेल
(v) – यह कथन इस तथ्य को दर्शाता है कि भारतीय रेल देश की विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, और समुदायों को एक साथ यात्रा करने का अवसर देती है। लोग अलग-अलग स्थानों, धर्मों और जीवनशैली के होते हुए भी एक ही डिब्बे में सफर करते हैं, जिससे एकता की भावना उत्पन्न होती है।
(vi) – लेखक के अनुसार भारतीय रेल पर्यटन के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुँचाती है और श्रमिकों व छात्रों के आने-जाने को सुलभ बनाती है। इससे देश की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है।
(vii) – लेखक के अनुसार रेल को प्रभावी बनाए रखने के लिए समय पालन, सफाई, सुरक्षा और तकनीकी उन्नयन जैसे क्षेत्रों में सुधार आवश्यक है। भीड़भाड़, देरी और संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं का समाधान करके रेल व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है।
- भारतीय किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। वे न केवल देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि कृषि उत्पादों के माध्यम से औद्योगिक विकास में भी योगदान देते हैं। खेतों में पसीना बहाने वाला किसान मौसम की अनिश्चितताओं, बाजार की अस्थिरता, और सीमित संसाधनों के बावजूद देश के लिए अन्न उपजाता है। आज भी भारत की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, परंतु किसानों की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाओं, और उन्नत बीजों की कमी से उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। इसके साथ ही, फसल के उचित मूल्य न मिलने, बिचौलियों की भूमिका और ऋण के बोझ ने किसानों की समस्याओं को और भी जटिल बना दिया है। कुछ क्षेत्रों में किसानों ने आत्महत्या जैसा कठोर कदम भी उठाया है, जो इस संकट की गंभीरता को दर्शाता है। सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं जैसे – प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, परंतु इनका लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुँच पाता। किसानों को संगठित करना, कृषि शिक्षा का प्रसार, और सहकारी समितियों को सशक्त बनाना समय की आवश्यकता है। साथ ही, उपज के भंडारण और परिवहन की सुविधाओं को सुधारकर किसान को बाजार से सीधे जोड़ना होगा। कृषि केवल भूमि जोतने का काम नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच, प्रबंधन कौशल और नीति-निर्माण का केंद्र भी बननी चाहिए। जब तक किसान को उसकी मेहनत का पूरा मूल्य नहीं मिलेगा और उसे सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक भारत की समृद्धि अधूरी ही रहेगी।
प्रश्न –
(i) लेखक के अनुसार भारतीय किसान का सबसे प्रमुख योगदान क्या है? (1)
(क) उद्योगों का संचालन
(ख) शिक्षा का प्रचार
(ग) देश की खाद्य सुरक्षा
(घ) पर्यटन का विकास
(ii) कथन (A): किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक की आवश्यकता होती है। (1)
कारण (R): पुरानी कृषि पद्धतियाँ अधिक लाभदायक होती हैं।
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) निम्नलिखित में से कौन-सी योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई गई है? (1)
(क) उज्ज्वला योजना
(ख) जनधन योजना
(ग) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
(घ) आयुष्मान योजना
(iv) लेखक के अनुसार कृषि को किस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए? (1)
(क) केवल पारंपरिक काम
(ख) एक धार्मिक कर्तव्य
(ग) केवल ग्रामीण रोजगार
(घ) वैज्ञानिक सोच और नीति-निर्माण का केंद्र
(v) “कृषि केवल भूमि जोतने का काम नहीं है।” – इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) लेखक के अनुसार किसानों की प्रमुख समस्याएँ कौन-सी हैं? (2)
(vii) किसानों की स्थिति सुधारने के लिए लेखक ने क्या उपाय सुझाए हैं? (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ग) देश की खाद्य सुरक्षा
(ii) – (ग) A सही है, R गलत है।
(iii) – (ग) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
(iv) – (घ) वैज्ञानिक सोच और नीति-निर्माण का केंद्र
(v) – इस कथन का आशय है कि कृषि अब केवल परंपरागत तरीके से खेत जोतने तक सीमित नहीं रह गई है। इसमें अब वैज्ञानिक तकनीक, प्रबंधन कौशल, और आर्थिक रणनीति की भी आवश्यकता है। किसान को अब एक कुशल प्रबंधक और नवाचारकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए।
(vi) – लेखक के अनुसार किसानों को आधुनिक संसाधनों की कमी, फसल का उचित मूल्य न मिलना, ऋण का बोझ, बिचौलियों की भूमिका और प्राकृतिक आपदाओं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
(vii) – लेखक ने सुझाव दिया है कि किसानों को संगठित किया जाए, कृषि शिक्षा का प्रचार हो, सहकारी समितियाँ सशक्त बनाई जाएँ और भंडारण एवं परिवहन की व्यवस्था सुधारी जाए ताकि किसान सीधे बाजार से जुड़ सके और उसे उसकी उपज का पूरा मूल्य मिल सके।
- आज के डिजिटल युग में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे माध्यमों ने न केवल हमारी कार्यप्रणाली को बदला है, बल्कि सोचने और संवाद करने के ढंग को भी प्रभावित किया है। शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, कृषि, और प्रशासन — सभी क्षेत्रों में डिजिटल तकनीकों का प्रभाव देखा जा सकता है। अब विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, किसान मौसम और बाजार की जानकारी मोबाइल ऐप्स से प्राप्त कर सकते हैं, और नागरिक सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पोर्टल्स के माध्यम से पहुँच सकते हैं। यह डिजिटल परिवर्तन जीवन को सुगम, त्वरित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। परंतु इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। साइबर अपराध, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन, डिजिटल साक्षरता की कमी और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे मुद्दे इस युग की वास्तविकताएँ हैं। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच और तकनीकी जानकारी का अभाव डिजिटल असमानता को जन्म देता है। इसके अलावा, सोशल मीडिया के माध्यम से फैलने वाली झूठी खबरें और अफवाहें सामाजिक तनाव का कारण बनती हैं। अतः डिजिटल युग की सफलता केवल तकनीकी विकास पर नहीं, बल्कि उसके विवेकपूर्ण और जिम्मेदार उपयोग पर निर्भर करती है। सरकार द्वारा ‘डिजिटल इंडिया’ जैसी योजनाओं का उद्देश्य हर नागरिक तक डिजिटल सेवाओं की पहुँच बनाना है, जिससे पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित की जा सके। नागरिकों को चाहिए कि वे तकनीकी साधनों का उपयोग जागरूकता, शिक्षा और विकास के लिए करें न कि भ्रम और हिंसा फैलाने के लिए। यदि हम इस तकनीकी युग को संतुलित रूप से अपनाते हैं तो यह भारत को वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकता है।
प्रश्न –
(i) डिजिटल युग ने मानव जीवन में क्या परिवर्तन लाया है? (1)
(क) आर्थिक असमानता बढ़ाई है
(ख) कार्यप्रणाली और संवाद के तरीके बदले हैं
(ग) पारंपरिक शिक्षा को समाप्त कर दिया है
(घ) केवल शहरी विकास को बढ़ावा दिया है
(ii) कथन (A): डिजिटल तकनीकों से जीवन अधिक पारदर्शी और त्वरित बना है। (1)
कारण (R): डिजिटल सेवाओं की पहुँच केवल बड़े शहरों तक सीमित है।
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) डिजिटल युग की कौन-सी चुनौती नहीं है? (1)
(क) साइबर अपराध
(ख) डेटा गोपनीयता
(ग) डिजिटल साक्षरता
(घ) खेल-कूद का विकास
(iv) ‘डिजिटल इंडिया’ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? (1)
(क) इंटरनेट महँगा बनाना
(ख) सोशल मीडिया को बंद करना
(ग) हर नागरिक तक डिजिटल सेवाओं की पहुँच बनाना
(घ) केवल शहरी क्षेत्र में डेटा पहुँचाना
(v) “डिजिटल युग की सफलता केवल तकनीकी विकास पर नहीं निर्भर करती।” – इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) लेखक के अनुसार सोशल मीडिया से समाज पर कौन-से नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं? (2)
(vii) डिजिटल असमानता किन कारणों से उत्पन्न होती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ख) कार्यप्रणाली और संवाद के तरीके बदले हैं
(ii) – (ग) A सही है, R गलत है।
(iii) – (घ) खेल-कूद का विकास
(iv) – (ग) हर नागरिक तक डिजिटल सेवाओं की पहुँच बनाना
(v) – इस कथन का आशय यह है कि तकनीकी साधनों का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका उपयोग विवेकपूर्ण, नैतिक और जिम्मेदार ढंग से होना आवश्यक है। यदि तकनीक का दुरुपयोग हो तो यह समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है।
(vi) – लेखक के अनुसार सोशल मीडिया पर झूठी खबरों और अफवाहों का प्रसार होता है, जिससे समाज में भ्रम, तनाव और कभी-कभी हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करता है।
(vii) – डिजिटल असमानता का कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच की कमी और तकनीकी ज्ञान का अभाव। इसे दूर करने के लिए डिजिटल शिक्षा, किफायती उपकरणों की उपलब्धता और इंटरनेट सेवाओं का विस्तार आवश्यक है।
- भारत में जल संसाधनों की उपलब्धता और उनका समुचित प्रबंधन एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। एक ओर भारत में बड़ी संख्या में नदियाँ, झीलें और भूमिगत जल भंडार हैं, तो दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण जल संकट दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि अन्य हिस्सों में भीषण सूखा पड़ता है। यह विषमता केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं, बल्कि मानवजनित गतिविधियों से भी उत्पन्न होती है। नदियों के तटों पर अतिक्रमण, जल स्रोतों का प्रदूषण, और भूजल का अत्यधिक दोहन इस संकट को और गंभीर बना देते हैं। हाल के वर्षों में कई प्रमुख शहरों ने जल की भारी कमी का अनुभव किया है, जहाँ पीने योग्य जल के लिए लंबी कतारें लगती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएँ कई किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाती हैं। जल संकट केवल मानव जीवन को ही नहीं, बल्कि कृषि, पशुपालन और औद्योगिक विकास को भी प्रभावित करता है। फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त जल न मिलने से उत्पादन घटता है, जिससे आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। सरकार ने जल संरक्षण को लेकर कई योजनाएँ आरंभ की हैं, जैसे– ‘जल जीवन मिशन’, ‘अटल भूजल योजना’ और ‘नमामि गंगे कार्यक्रम’। इनका उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण, स्वच्छता और पुनर्भरण को बढ़ावा देना है। साथ ही, समाज को भी जागरूक होकर वर्षा जल संचयन, जल पुन: उपयोग और पारंपरिक जल प्रणालियों के संरक्षण की दिशा में कार्य करना चाहिए। जल को केवल प्राकृतिक संसाधन न समझकर, एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकारना होगा। तभी भावी पीढ़ियों को एक सुरक्षित और समृद्ध जल भविष्य प्रदान किया जा सकेगा।
प्रश्न –
(i) भारत में जल संकट का एक प्रमुख कारण क्या है? (1)
(क) अधिक वनों का होना
(ख) अत्यधिक वर्षा
(ग) जल का अनियंत्रित दोहन और प्रदूषण
(घ) समुद्री जल की उपेक्षा
(ii) कथन (A): जल संकट केवल प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है। (1)
कारण (R): मानवजनित गतिविधियाँ जैसे अतिक्रमण और प्रदूषण जल संकट को बढ़ाती हैं।
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों गलत हैं।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) जल संकट से कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं? (1)
(क) केवल उद्योग
(ख) कृषि, पशुपालन और उद्योग
(ग) केवल शहरी जीवन
(घ) केवल शिक्षा क्षेत्र
(iv) ‘जल जीवन मिशन’ योजना का उद्देश्य क्या है? (1)
(क) वर्षा जल को रोकना
(ख) पीने के पानी की आपूर्ति बढ़ाना
(ग) समुद्र में बाँध बनाना
(घ) केवल सिंचाई प्रणाली सुधारना
(v) “जल को केवल प्राकृतिक संसाधन न समझकर, एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकारना होगा।” — इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) लेखक के अनुसार जल संकट के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या हैं? (2)
(vii) जल संरक्षण की दिशा में सरकार और समाज द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ग) जल का अनियंत्रित दोहन और प्रदूषण
(ii) – (घ) A गलत है, R सही है।
(iii) – (ख) कृषि, पशुपालन और उद्योग
(iv) – (ख) पीने के पानी की आपूर्ति बढ़ाना
(v) – इस कथन का आशय है कि जल को केवल एक उपयोगी वस्तु मानना पर्याप्त नहीं है। इसके संरक्षण की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की है। वर्षा जल संचयन, जल का विवेकपूर्ण उपयोग, और जल स्रोतों की रक्षा करके हम सामाजिक उत्तरदायित्व निभा सकते हैं।
(vi) – जल संकट से सामाजिक रूप से लोगों को दूर-दराज से पानी लाना पड़ता है, जिससे श्रम और समय की हानि होती है। आर्थिक रूप से कृषि और उद्योगों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उत्पादन घटता है और आर्थिक अस्थिरता आती है।
(vii) – सरकार ने ‘जल जीवन मिशन’, ‘अटल भूजल योजना’ और ‘नमामि गंगे’ जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। समाज में वर्षा जल संचयन, जल पुनः उपयोग, और पारंपरिक जल प्रणालियों को संरक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल राजनीतिक आंदोलनों और नेताओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आम जनता की भावनाएँ, बलिदान और जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वतंत्रता की यह यात्रा दशकों तक चली जिसमें अनेक आंदोलनों, सत्याग्रहों, असहयोग और क्रांतिकारी प्रयासों ने मिलकर आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। इस संघर्ष में महात्मा गांधी के नेतृत्व ने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों को केंद्र में रखा, वहीं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान और संघर्ष का नया उदाहरण प्रस्तुत किया। भारत के ग्रामीण इलाकों में भी स्वतंत्रता की चेतना फैल गई थी। स्त्रियाँ, विद्यार्थी, मजदूर, किसान—सभी ने अपने-अपने तरीके से इस आंदोलन में योगदान दिया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना जैसे कदम जनता के बीच जागरूकता लाने में सहायक रहे। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 के स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत ने अनेकों उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन लोगों की इच्छाशक्ति कभी नहीं डिगी। ब्रिटिश शासन के दौरान हुए अत्याचारों, जैसे जलियाँवाला बाग हत्याकांड, ने जनसामान्य को झकझोर कर रख दिया और देशभर में आक्रोश की लहर दौड़ गई। ऐसे घटनाक्रमों ने आज़ादी की लौ को और प्रखर किया। स्वतंत्रता केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह आत्मसम्मान, स्वराज और आत्मनिर्भरता की भावना का पुनर्जागरण था। स्वतंत्र भारत की कल्पना केवल एक राजनीतिक इकाई नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और समग्र विकास के रूप में की गई थी। आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि हम केवल उत्सव न मनाएँ, बल्कि उन मूल्यों को भी आत्मसात करें जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया। स्वतंत्रता का सही सम्मान तभी है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और देश को प्रगति की राह पर अग्रसर करें।
प्रश्न –
(i) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किन-किन वर्गों ने भाग लिया? (1)
(क) केवल नेता और सैनिक
(ख) केवल किसान
(ग) स्त्रियाँ, विद्यार्थी, मजदूर, किसान आदि सभी
(घ) केवल शहरी लोग
(ii) कथन (A): स्वतंत्रता आंदोलन केवल अहिंसात्मक रहा। (1)
कारण (R): क्रांतिकारी प्रयासों ने स्वतंत्रता की राह प्रशस्त की।
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? (1)
(क) विदेशी वस्त्रों को खरीदना
(ख) ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली को अपनाना
(ग) स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करना
(घ) ब्रिटिश अधिकारियों को सम्मान देना
(iv) जलियाँवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव क्या हुआ? (1)
(क) जनता खुश हुई
(ख) लोग मौन रहे
(ग) देशभर में आक्रोश फैल गया
(घ) आंदोलन रुक गया
(v) “स्वतंत्रता केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था।” – इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) लेखक के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विशेषताएँ क्या थीं? (2)
(vii) आज़ादी का सही सम्मान किस प्रकार किया जा सकता है? (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ग) स्त्रियाँ, विद्यार्थी, मजदूर, किसान आदि सभी
(ii) – (घ) A गलत है, R सही है।
(iii) – (ग) स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करना
(iv) – (ग) देशभर में आक्रोश फैल गया
(v) – इस कथन का आशय है कि स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश शासन को हटाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और स्वराज की भावना से जुड़ी हुई थी। यह एक नए भारत के निर्माण की शुरुआत थी।
(vi) – लेखक के अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भागीदारी, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत, साथ ही क्रांतिकारी प्रयास – ये सभी इसकी प्रमुख विशेषताएँ थीं। यह केवल राजनैतिक नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का भी आंदोलन था।
(vii) – आज़ादी का सही सम्मान तभी है जब नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करें, सामाजिक मूल्यों को अपनाएँ, और देश को प्रगति, समानता और सद्भाव की दिशा में ले जाएँ। केवल उत्सव मनाना पर्याप्त नहीं है।
- पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाना आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। एक ओर जहाँ विकास के लिए उद्योगों, भवनों, सड़कों और विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर इनसे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है, जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, वायु और जल प्रदूषण, जैव विविधता का ह्रास—ये सभी आधुनिक विकास की वह कीमत हैं जिसे मानवता चुका रही है। विकास की होड़ में हम यह भूल जाते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता प्रकृति के संतुलन पर ही निर्भर है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, अगर जलस्रोत दूषित होंगे तो पीने का पानी समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि आज “सतत विकास” का विचार विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। सतत विकास का अर्थ है – ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता न करे। इसके लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों, हरित तकनीकों और पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली को अपनाना आवश्यक है। भारत में भी इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं जैसे – सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, एकल-प्रयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना, और वृक्षारोपण अभियानों को प्रोत्साहित करना। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। यदि हम बिजली की बचत करें, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें, सार्वजनिक परिवहन अपनाएँ और प्लास्टिक का प्रयोग कम करें तो यह छोटे-छोटे कदम भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देकर जागरूक पीढ़ी का निर्माण किया जा सकता है। हमें यह समझना होगा कि धरती केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे पश्चात् आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। यदि हम आज अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे, तो कल हमें जीवन के लिए मूलभूत संसाधनों का अभाव झेलना पड़ेगा।
प्रश्न –
(i) सतत विकास का उद्देश्य क्या है? (1)
(क) अधिक कारखाने लगाना
(ख) केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति
(ग) केवल पर्यावरण संरक्षण
(घ) वर्तमान और भविष्य दोनों की ज़रूरतों का ध्यान रखना
(ii) कथन (A): विकास के लिए वनों की कटाई आवश्यक है। (1)
कारण (R): बिना पेड़ों के जीवन संभव नहीं है।
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य पर्यावरण संरक्षण में सहायक नहीं है? (1)
(क) वृक्षारोपण करना
(ख) प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ाना
(ग) सार्वजनिक परिवहन अपनाना
(घ) जल संरक्षण करना
(iv) सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत में कौन-से प्रयास किए जा रहे हैं? (1)
(क) कोयले के उपयोग को बढ़ाना
(ख) नदियों का दोहन करना
(ग) एकल-प्रयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना
(घ) वनों की कटाई करना
(v) “पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है।” – इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) लेखक के अनुसार आधुनिक विकास के कारण पर्यावरण पर क्या-क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? (2)
(vii) सतत विकास के सिद्धांत को व्यवहार में लाने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है? (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (घ) वर्तमान और भविष्य दोनों की ज़रूरतों का ध्यान रखना
(ii) – (घ) A गलत है, R सही है।
(iii) – (ख) प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ाना
(iv) – (ग) एकल-प्रयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना
(v) – इस कथन का आशय यह है कि केवल सरकार द्वारा योजनाएँ बनाना पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जैसे बिजली-पानी की बचत, प्लास्टिक का कम प्रयोग, वनों की रक्षा आदि।
(vi) – लेखक के अनुसार आधुनिक विकास के कारण वनों की कटाई, जल और वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है।
(vii) – सतत विकास को व्यवहार में लाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, हरित तकनीकों को अपनाना, प्लास्टिक पर प्रतिबंध, पर्यावरण शिक्षा, और आम जनता की भागीदारी आवश्यक है।
- भारतीय समाज में त्योहारों का विशेष महत्व रहा है। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और मानवीय मूल्यों के संवाहक भी हैं। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में त्योहारों ने हमेशा लोगों को जोड़ने का कार्य किया है। दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व, बैसाखी, ओणम, पोंगल आदि पर्व न केवल विभिन्न धर्मों और समुदायों की पहचान हैं, बल्कि भारत की गंगा-जमुनी संस्कृति के प्रतीक भी हैं। त्योहारों के अवसर पर लोग भेदभाव भूलकर एक-दूसरे से मेल-मिलाप करते हैं, उपहारों का आदान-प्रदान होता है, और एक साझा उल्लास का वातावरण बनता है। इनसे न केवल भावनात्मक संबंध मजबूत होते हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है। मिठाइयों की दुकानों, कपड़ों, सजावट, खिलौनों और यात्रा सेवाओं में त्योहारों के समय भारी वृद्धि देखी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मेले और उत्सव सामूहिकता की भावना को जन्म देते हैं, जहाँ कला, शिल्प और लोक परंपराएँ सजीव होती हैं। त्योहारों के पीछे कोई-न-कोई ऐतिहासिक या पौराणिक कथा जुड़ी होती है जो नैतिक शिक्षा प्रदान करती है – जैसे दीपावली पर सत्य की विजय, होली पर बुराई का दहन, ईद पर त्याग और करुणा की भावना। इन कथाओं के माध्यम से नई पीढ़ी को अपने मूल्यों और परंपराओं से जोड़ा जाता है। परंतु आज आधुनिकता की दौड़ में त्योहारों की आत्मा कहीं-कहीं खोती जा रही है। दिखावा, अत्यधिक खर्च, पटाखों और ध्वनि प्रदूषण जैसे पहलुओं ने इन पवित्र अवसरों को प्रदूषण और तनाव का कारण बना दिया है। अतः आवश्यकता है कि हम त्योहारों को उनकी सादगी, पवित्रता और मूल भावना के साथ मनाएँ, जिससे सामाजिक समरसता, पर्यावरण संतुलन और सांस्कृतिक गौरव अक्षुण्ण रह सके।
प्रश्न –
(i) त्योहारों का प्रमुख सामाजिक उद्देश्य क्या है? (1)
(क) व्यापार में वृद्धि करना
(ख) धार्मिक श्रेष्ठता दिखाना
(ग) सामाजिक एकता और मेल-जोल बढ़ाना
(घ) मनोरंजन कराना
(ii) कथन (A): त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। (1)
कारण (R): त्योहारों से सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है।
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) त्योहारों से कौन-से व्यवसायों को लाभ नहीं होता? (1)
(क) मिठाइयाँ और सजावट
(ख) कपड़े और उपहार
(ग) औषधि निर्माण
(घ) यात्रा सेवाएँ
(iv) दीपावली पर्व किस बात का प्रतीक है? (1)
(क) बुराई पर बुराई की विजय
(ख) युद्ध का उत्सव
(ग) सत्य की विजय
(घ) मनुष्य की हार
(v) “त्योहार केवल उत्सव नहीं, मूल्य भी सिखाते हैं।” — इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) लेखक के अनुसार त्योहारों से स्थानीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति को कैसे बल मिलता है? (2)
(vii) त्योहारों के मनाने के आधुनिक तरीकों में आई समस्याओं का उल्लेख कीजिए और समाधान सुझाइए। (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ग) सामाजिक एकता और मेल-जोल बढ़ाना
(ii) – (घ) A गलत है, R सही है।
(iii) – (ग) औषधि निर्माण
(iv) – (ग) सत्य की विजय
(v) – इस कथन का आशय है कि त्योहार केवल आनंद मनाने का अवसर नहीं होते, बल्कि वे हमें करुणा, भाईचारा, सत्य, त्याग, और सहिष्णुता जैसे नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देते हैं।
(vi) – त्योहारों के समय दुकानों, बाजारों और सेवाओं में मांग बढ़ने से स्थानीय व्यापार को लाभ होता है। साथ ही, मेले और लोक परंपराओं के माध्यम से कला और संस्कृति को नया जीवन मिलता है।
(vii) – आज के समय में त्योहारों में अत्यधिक खर्च, ध्वनि और वायु प्रदूषण, और दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ गई है। समाधान के रूप में सादगीपूर्ण उत्सव, पर्यावरण-अनुकूल साधनों का उपयोग और मूल भावना को केंद्र में रखना आवश्यक है।
- शहरीकरण आधुनिक विकास का एक अनिवार्य परिणाम है, जो आर्थिक प्रगति, औद्योगीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण तेजी से हो रहा है। भारत में विशेष रूप से पिछले कुछ दशकों में शहरी क्षेत्रों का विस्तार बहुत तेज़ी से हुआ है। लोग बेहतर शिक्षा, रोजगार और जीवन-स्तर की आशा में गाँवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे जहाँ एक ओर महानगरों का विकास हुआ है, वहीं दूसरी ओर अनेक समस्याएँ भी उत्पन्न हो गई हैं। अत्यधिक जनसंख्या दबाव के कारण यातायात जाम, प्रदूषण, झुग्गी-झोपड़ियाँ, जल एवं स्वच्छता संकट जैसी समस्याएँ सामने आई हैं। शहरों की सीमाएँ अनियोजित ढंग से फैल रही हैं, जिससे हरियाली और खुले स्थान कम होते जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव पर्यावरण असंतुलन का कारण बनता है। शहरी जीवन की भागदौड़, एकाकीपन और तनाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। हालांकि शहरीकरण के कई सकारात्मक पहलू भी हैं—जैसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ, शैक्षिक संस्थान, तकनीकी नवाचार और आर्थिक अवसर। यदि शहरीकरण को योजनाबद्ध ढंग से अपनाया जाए तो यह विकास का एक सशक्त साधन बन सकता है। इसके लिए स्मार्ट सिटी परियोजना, हरित भवन निर्माण, सार्वजनिक परिवहन की मजबूती और झुग्गियों के पुनर्विकास जैसे उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित विकास कर वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएँ प्रदान की जाएँ तो शहरों पर बोझ कम किया जा सकता है। हमें समझना होगा कि शहरीकरण को न तो पूरी तरह रोका जा सकता है और न ही अनियंत्रित रूप से बढ़ने दिया जा सकता है। यह आवश्यक है कि शहरों को रहने योग्य, टिकाऊ और समावेशी बनाने के लिए नागरिकों, प्रशासन और नीति-निर्माताओं के बीच सहयोग हो। तभी हम एक संतुलित, सुरक्षित और संवेदनशील समाज की दिशा में बढ़ सकेंगे।
प्रश्न –
(i) लोग गाँवों से शहरों की ओर क्यों पलायन कर रहे हैं? (1)
(क) खेती से ऊबकर
(ख) आपदाओं के डर से
(ग) बेहतर शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर की तलाश में
(घ) मौसम परिवर्तन के कारण
(ii) कथन (A): शहरीकरण से केवल लाभ होते हैं। (1)
कारण (R): इससे तकनीकी नवाचार और आर्थिक अवसर मिलते हैं।
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) निम्नलिखित में से कौन-सी समस्या शहरीकरण से जुड़ी नहीं है? (1)
(क) जल संकट
(ख) हरियाली में वृद्धि
(ग) यातायात जाम
(घ) मानसिक तनाव
(iv) शहरीकरण को संतुलित करने के लिए कौन-सा उपाय उचित है? (1)
(क) गाँवों को उजाड़ना
(ख) झुग्गियों को नष्ट करना
(ग) ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना
(घ) शहरों में और अधिक जनसंख्या बढ़ाना
(v) “शहरीकरण को न तो रोका जा सकता है, न ही अनियंत्रित रूप से बढ़ने दिया जा सकता है।” – इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) लेखक के अनुसार शहरी जीवन के नकारात्मक पक्ष कौन-कौन से हैं? (2)
(vii) शहरीकरण को योजनाबद्ध और टिकाऊ बनाने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं? (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ग) बेहतर शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर की तलाश में
(ii) – (घ) A गलत है, R सही है।
(iii) – (ख) हरियाली में वृद्धि
(iv) – (ग) ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना
(v) – इस कथन का आशय यह है कि शहरीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसे पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, परंतु अगर यह बिना योजना और संतुलन के बढ़ता रहा तो इससे गंभीर समस्याएँ पैदा होंगी। इसलिए इसकी दिशा और गति नियंत्रित होनी चाहिए।
(vi) – लेखक के अनुसार अत्यधिक जनसंख्या दबाव, यातायात जाम, प्रदूषण, जल संकट, हरियाली की कमी, मानसिक तनाव और झुग्गी-झोपड़ियाँ शहरी जीवन के नकारात्मक पहलू हैं।
(vii) – शहरीकरण को टिकाऊ बनाने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं, हरित भवनों का निर्माण हो रहा है, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर किया जा रहा है और झुग्गियों का पुनर्विकास किया जा रहा है।
- आज के युग में पुस्तकें केवल ज्ञान का स्रोत ही नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, कल्पना की उड़ान और आत्मचिंतन का माध्यम भी बन गई हैं। एक अच्छी पुस्तक पाठक के जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। भारत में प्राचीन काल से ही पुस्तक संस्कृति रही है, चाहे वह वेद-उपनिषद हों या बाद के काल की साहित्यिक रचनाएँ। एक समय था जब पुस्तकालयों को विद्या का मंदिर माना जाता था और विद्यार्थियों को पुस्तकों से आत्मिक लगाव होता था। परंतु अब डिजिटल माध्यमों के आगमन से पाठन संस्कृति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट पर उपलब्ध जानकारी ने भले ही सूचना को त्वरित और व्यापक बनाया है, लेकिन गंभीर अध्ययन और गहन चिंतन की प्रवृत्ति में गिरावट आई है। विशेषकर युवाओं में पुस्तकों के स्थान पर सोशल मीडिया और लघु वीडियो देखने की रुचि अधिक हो गई है। इसका प्रभाव भाषा पर, सोचने की क्षमता पर और एकाग्रता पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पढ़ना केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं, बल्कि आत्मविकास के लिए आवश्यक होता है। पुस्तकों के माध्यम से व्यक्ति इतिहास, विज्ञान, साहित्य, मनोविज्ञान और समाज को समझ सकता है। एक शोध के अनुसार नियमित अध्ययन करने वाले लोगों में निर्णय लेने की क्षमता, सहानुभूति और तर्कशक्ति अधिक विकसित होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि पाठ्यपुस्तकों के साथ-साथ साहित्यिक, प्रेरणात्मक और ज्ञानवर्धक पुस्तकों को भी पढ़ने की आदत डाली जाए। विद्यालयों और परिवारों में पढ़ने के वातावरण को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी पुस्तकों को केवल जानकारी का साधन न समझे, बल्कि उन्हें जीवन का अभिन्न अंग बनाए। डिजिटल युग में भी यदि हम पुस्तकों की ओर लौटें, तो यह न केवल मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होगा, बल्कि हमें एक विचारशील और संवेदनशील नागरिक बनने में भी मदद करेगा।
प्रश्न –
(i) लेखक के अनुसार पुस्तकों का प्रमुख योगदान क्या है? (1)
(क) परीक्षा की तैयारी
(ख) त्वरित जानकारी
(ग) विचारों की स्वतंत्रता और आत्मचिंतन का माध्यम
(घ) मनोरंजन
(ii) कथन (A): डिजिटल युग में अध्ययन की प्रवृत्ति बढ़ी है। (1)
कारण (R): सोशल मीडिया और लघु वीडियो ने युवाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित किया है।
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों गलत हैं।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) पुस्तकों के स्थान पर युवाओं की रुचि किसमें अधिक हो गई है? (1)
(क) समाचार पत्र पढ़ने में
(ख) शास्त्रीय संगीत में
(ग) सोशल मीडिया और वीडियो देखने में
(घ) योगाभ्यास में
(iv) पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए क्या आवश्यक है? (1)
(क) किताबों की बिक्री बढ़ाना
(ख) विद्यालयों और परिवारों में पढ़ने का वातावरण बनाना
(ग) मोबाइल सस्ता करना
(घ) पुस्तकालय बंद करना
(v) “पढ़ना केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं, आत्मविकास के लिए आवश्यक होता है।” — इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) लेखक के अनुसार पुस्तकों की उपेक्षा से युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? (2)
(vii) डिजिटल युग में भी पुस्तक संस्कृति को जीवित रखने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा सकते हैं? (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ग) विचारों की स्वतंत्रता और आत्मचिंतन का माध्यम
(ii) – (ख) A और R दोनों गलत हैं।
(iii) – (ग) सोशल मीडिया और वीडियो देखने में
(iv) – (ख) विद्यालयों और परिवारों में पढ़ने का वातावरण बनाना
(v) – इस कथन का आशय यह है कि पढ़ना केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के सोचने, समझने और आत्मविश्लेषण करने की क्षमता को भी विकसित करता है। इससे व्यक्ति अधिक संवेदनशील और जागरूक बनता है।
(vi) – लेखक के अनुसार पुस्तकों की उपेक्षा के कारण युवाओं की एकाग्रता घट रही है, भाषा कमजोर हो रही है और तर्कशक्ति में कमी आ रही है। उनके मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
(vii) – डिजिटल युग में पुस्तक मेलों का आयोजन, ऑनलाइन पुस्तकालयों की सुविधा, स्कूलों में पुस्तक पाठन प्रतियोगिता और घरों में माता-पिता द्वारा बच्चों को नियमित रूप से पढ़कर सुनाना – ये प्रयास पुस्तक संस्कृति को जीवित रख सकते हैं।
- भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी सफलता इसके नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। लोकतंत्र का आधार जनता की सत्ता है, जिसमें नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपनी सरकार स्वयं चुन सकें। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, और न्याय के सिद्धांत लोकतंत्र के मूल स्तंभ हैं। लेकिन केवल अधिकार प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता, जब तक कि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन न करें। मतदान करना, कर अदा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना – ये सब नागरिक कर्तव्यों का हिस्सा हैं। दुर्भाग्यवश, कई बार देखा जाता है कि लोग अधिकारों की बात तो करते हैं, परंतु कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। उदाहरण के लिए, चुनाव के समय कुछ लोग मतदान न करने को अपना अधिकार मानते हैं, जबकि यह लोकतंत्र को कमजोर करने वाला व्यवहार है। लोकतांत्रिक प्रणाली तभी प्रभावी बनती है जब हर व्यक्ति अपने दायित्व को समझे और राष्ट्रहित को प्राथमिकता दे। नागरिकों की सजगता से ही सरकारें जवाबदेह बनती हैं और प्रशासन पारदर्शी होता है। जब जनता शिक्षित, सचेत और नैतिक होती है, तभी लोकतंत्र भी सशक्त होता है। लोकतंत्र का सौंदर्य इसमें है कि यह सबको समान अवसर देता है – गरीब, अमीर, ग्रामीण, शहरी, स्त्री, पुरुष सभी को एक मताधिकार प्राप्त है। यह प्रणाली केवल शासन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का उपकरण भी है। लोकतंत्र में संवाद, आलोचना और असहमति के लिए भी स्थान होता है, जो किसी भी समाज के विकास के लिए आवश्यक है। परंतु यदि लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना है तो हमें केवल उपभोक्ता बनकर नहीं, उत्तरदायी नागरिक बनकर कार्य करना होगा। नागरिकों और सरकार के बीच भरोसे का यह संबंध तभी मजबूत होता है जब दोनों अपने अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन बनाए रखें।
प्रश्न –
(i) लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? (1)
(क) सरकार की शक्ति पर
(ख) नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर
(ग) चुनाव आयोग पर
(घ) न्यायपालिका पर
(ii) कथन (A): लोकतंत्र में केवल अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। (1)
कारण (R): नागरिकों का कर्तव्यों के प्रति उदासीन होना सामान्य है।
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों गलत हैं।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) लोकतंत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? (1)
(क) पुलिस का
(ख) नागरिकों का
(ग) मंत्रीमंडल का
(घ) अफसरों का
(iv) मतदान करना किसका उदाहरण है? (1)
(क) मौलिक अधिकार
(ख) नागरिक कर्तव्य
(ग) विशेषाधिकार
(घ) संविधान संशोधन
(v) “लोकतंत्र केवल शासन का माध्यम नहीं, सामाजिक परिवर्तन का उपकरण भी है।” — इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) लेखक के अनुसार नागरिक कर्तव्यों की उपेक्षा से क्या हानियाँ होती हैं? (2)
(vii) लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए नागरिकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ख) नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर
(ii) – (ख) A और R दोनों गलत हैं।
(iii) – (ख) नागरिकों का
(iv) – (ख) नागरिक कर्तव्य
(v) – इस कथन का आशय है कि लोकतंत्र केवल शासक चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह समाज में समानता, स्वतंत्रता, और न्याय स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम है। इससे सामाजिक सुधार और जागरूकता संभव होती है।
(vi) – लेखक के अनुसार जब नागरिक अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं, तो शासन व्यवस्था कमजोर पड़ती है, सरकारें जवाबदेह नहीं बनतीं और लोकतंत्र में भ्रष्टाचार, असमानता और अव्यवस्था बढ़ती है।
(vii) – नागरिकों को चाहिए कि वे मतदान करें, कर अदा करें, कानून का पालन करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें। साथ ही संवाद, आलोचना और जागरूकता के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत बनाएँ।
- भारतीय कृषि व्यवस्था न केवल देश की आर्थिक रीढ़ है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की जीविका का आधार भी है। देश की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। परंतु यह विडंबना है कि जिस क्षेत्र पर देश की इतनी बड़ी आबादी आश्रित है, उसी क्षेत्र को सबसे अधिक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। आधुनिक तकनीक, सिंचाई व्यवस्था, भंडारण सुविधाएँ, और बाज़ार तक पहुँच—इन सब क्षेत्रों में अभी भी कृषि पिछड़ी हुई है। परिणामस्वरूप किसान समय पर फसल बो तो पाता है, परंतु उचित दाम नहीं मिलने के कारण घाटा सहता है। कई बार प्राकृतिक आपदाएँ जैसे सूखा, बाढ़ या ओलावृष्टि किसानों की मेहनत पर पानी फेर देती हैं। इसके अलावा बिचौलियों और महाजनों के चंगुल में फँसे किसान ऋण के बोझ तले दबते चले जाते हैं। हालांकि सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलाई गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि आदि, परंतु इनका लाभ सभी किसानों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाता। इसके पीछे जागरूकता की कमी, भ्रष्टाचार और जमीनी स्तर पर प्रणाली की धीमी गति प्रमुख कारण हैं। एक ओर हम कृषि क्षेत्र की समस्याओं की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई, सहकारी मंडियाँ, और किसान उत्पादक संगठन (FPOs) जैसे सकारात्मक प्रयास भी हो रहे हैं। यदि इन नवाचारों को सही दिशा में प्रोत्साहित किया जाए और किसानों को सशक्त किया जाए, तो कृषि फिर से लाभकारी व्यवसाय बन सकती है। इसके लिए किसानों को शिक्षित करना, कृषि अनुसंधानों को खेतों तक पहुँचाना और मूल्य समर्थन प्रणाली को प्रभावी बनाना अत्यंत आवश्यक है। भारत जैसा कृषि प्रधान देश तभी सशक्त हो सकता है, जब उसका अन्नदाता आत्मनिर्भर, जागरूक और सम्मानित हो।
प्रश्न –
(i) भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? (1)
(क) लगभग 40%
(ख) लगभग 60%
(ग) लगभग 80%
(घ) लगभग 20%
(ii) कथन (A): किसान खेती तो करता है पर लाभ नहीं कमा पाता। (1)
कारण (R): उसे फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) निम्नलिखित में से कौन-सी योजना किसानों के लिए है? (1)
(क) आयुष्मान भारत
(ख) प्रधानमंत्री आवास योजना
(ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
(घ) स्वच्छ भारत मिशन
(iv) किसानों की समस्याओं का एक मुख्य कारण क्या है? (1)
(क) मौसम की जानकारी
(ख) बिचौलियों का दबाव और ऋण का बोझ
(ग) अधिक फसल उत्पादन
(घ) कृषि भूमि की वृद्धि
(v) “किसानों को सशक्त करना आवश्यक है।” — इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) लेखक के अनुसार कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है? (2)
(vii) सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक समान रूप से क्यों नहीं पहुँच पाता? स्पष्ट कीजिए। (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ख) लगभग 60%
(ii) – (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(iii) – (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
(iv) – (ख) बिचौलियों का दबाव और ऋण का बोझ
(v) – इस कथन का आशय यह है कि किसानों को तकनीकी ज्ञान, वित्तीय सहायता, बाजार तक सीधी पहुँच और अधिकारों की जानकारी देकर सशक्त बनाना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन सकें।
(vi) – कृषि को लाभकारी बनाने के लिए जैविक खेती, आधुनिक सिंचाई पद्धतियाँ, प्रभावशाली मूल्य समर्थन प्रणाली, कृषि शिक्षा, और किसान संगठनों को बढ़ावा देना आवश्यक है।
(vii) – योजनाओं का लाभ समान रूप से न पहुँचने का कारण है – किसानों में जागरूकता की कमी, योजनाओं की जानकारी न होना, भ्रष्टाचार, और स्थानीय स्तर पर धीमी कार्यप्रणाली।
- पानी जीवन का मूल आधार है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जल की आवश्यकता हर जीव के लिए बनी रही है। मनुष्य के दैनिक कार्यों से लेकर कृषि, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन तक, जल का उपयोग हर क्षेत्र में होता है। परंतु आज जल संकट एक गंभीर वैश्विक समस्या के रूप में सामने आ रही है। जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन, प्रदूषण, और वर्षा जल का संरक्षण न होना इसके प्रमुख कारण हैं। भारत में भी अनेक क्षेत्रों में जल की भारी कमी महसूस की जा रही है, विशेष रूप से गर्मियों में अनेक गाँवों और नगरों में पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं होता। भूमिगत जल स्तर निरंतर घटता जा रहा है क्योंकि हम जल को संग्रहित करने से अधिक उसका दोहन कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा की अनियमितता और बर्फ के पिघलते ग्लेशियर भी जल संकट को और गहरा बना रहे हैं। स्थिति यह है कि ‘जल युद्ध’ जैसे शब्द अब केवल कल्पना नहीं रहे, बल्कि भविष्य की संभावित सच्चाई बनते जा रहे हैं। इसका समाधान केवल सरकारों के स्तर पर संभव नहीं है, अपितु हर नागरिक को इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। वर्षा जल संचयन, रिसाइकलिंग, टपक सिंचाई जैसी तकनीकों को अपनाकर हम जल की बर्बादी रोक सकते हैं। विद्यालयों में जल संरक्षण की शिक्षा, घरेलू स्तर पर उपयोग में संयम, और उद्योगों में जल शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना जैसे प्रयास अनिवार्य हैं। यदि हम आज जल की महत्ता को नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को पीने योग्य पानी भी नसीब नहीं होगा। हमें यह याद रखना होगा कि जल प्रकृति का उपहार है और इसकी रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है।
प्रश्न –
(i) भूमिगत जल स्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? (1)
(क) वर्षा का अधिक होना
(ख) जल का सीमित उपयोग
(ग) जल का अत्यधिक दोहन
(घ) जलवायु का ठंडा होना
(ii) कथन (A): जल संकट केवल सरकार की जिम्मेदारी है। (1)
कारण (R): जल संरक्षण में आम नागरिक की कोई भूमिका नहीं होती।
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों गलत हैं।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) जल संकट को दूर करने के लिए कौन-सी तकनीक उपयोगी है? (1)
(क) टपक सिंचाई
(ख) भारी मशीनरी
(ग) अधिक बोरवेल
(घ) जल का व्यापार
(iv) जलवायु परिवर्तन जल संकट को कैसे प्रभावित कर रहा है? (1)
(क) जलवायु परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं है
(ख) वर्षा नियमित और पर्याप्त होती है
(ग) बर्फ अधिक जमती है
(घ) वर्षा अनियमित होती है और ग्लेशियर पिघलते हैं
(v) “जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, जीवन का मूल आधार है।” — इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) लेखक के अनुसार जल संकट के क्या-क्या कारण हैं? (2)
(vii) जल संकट से निपटने के लिए किन उपायों को अपनाने की आवश्यकता है? (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ग) जल का अत्यधिक दोहन
(ii) – (ख) A और R दोनों गलत हैं।
(iii) – (क) टपक सिंचाई
(iv) – (घ) वर्षा अनियमित होती है और ग्लेशियर पिघलते हैं
(v) – इस कथन का आशय यह है कि जल केवल उपयोग की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। इसके बिना मनुष्य ही नहीं, संपूर्ण प्रकृति का अस्तित्व असंभव है।
(vi) – लेखक के अनुसार जल संकट के मुख्य कारण हैं: जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन, प्रदूषण, वर्षा जल का संरक्षण न होना, भूमिगत जल स्तर में गिरावट, और जलवायु परिवर्तन।
(vii) – जल संकट से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन, टपक सिंचाई, जल रिसाइकलिंग, शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना, घरेलू स्तर पर बचत, और जन जागरूकता जैसे उपाय आवश्यक हैं।
- आज के युग में पर्यावरण संरक्षण मानव अस्तित्व की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण, वन कटाई, और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर दिया है। कारखानों से निकलने वाला धुआँ, वाहनों से उत्पन्न गैसें, प्लास्टिक कचरे का बढ़ता ढेर और जल स्रोतों में गिरता हुआ स्वच्छता स्तर इस असंतुलन के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। यदि समय रहते इन समस्याओं पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वायु, जल और भूमि मिलना दुर्लभ हो जाएगा। प्रदूषण न केवल पर्यावरण को प्रभावित करता है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डालता है। साँस की बीमारियाँ, त्वचा रोग, जलजनित संक्रमण और यहाँ तक कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियाँ भी प्रदूषण की देन हैं। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। हमें अपने जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव करने होंगे—जैसे प्लास्टिक की बजाय कपड़े या जूट के थैले प्रयोग करना, वृक्षारोपण करना, जल और बिजली की बचत करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, और घरेलू कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित करना। विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य बनाकर बच्चों में शुरू से ही प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न की जा सकती है। साथ ही, सामुदायिक स्तर पर सफाई अभियान, हरित सप्ताह, और प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र जैसी पहलें सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दे सकती हैं। यदि हम आज अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएँ और प्रकृति के साथ सहअस्तित्व की भावना अपनाएँ, तो न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बल्कि मानवता की निरंतरता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
प्रश्न –
(i) लेखक के अनुसार पर्यावरण असंतुलन का एक प्रमुख कारण क्या है? (1)
(क) वन संरक्षण
(ख) कारखानों का विकास
(ग) प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन
(घ) वर्षा की अधिकता
(ii) कथन (A): प्रदूषण केवल वायुमंडल को प्रभावित करता है। (1)
कारण (R): जल, वायु और भूमि तीनों प्रदूषित होते हैं।
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों गलत हैं।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) पर्यावरण संरक्षण का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? (1)
(क) नई फैक्ट्रियों का निर्माण
(ख) वृक्षों की कटाई
(ग) वृक्षारोपण
(घ) अधिक वाहनों की खरीद
(iv) कौन-सी आदत पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है? (1)
(क) प्लास्टिक का उपयोग
(ख) घरेलू कचरे का उचित निपटान
(ग) जल का अपव्यय
(घ) बिजली की फिजूलखर्ची
(v) “पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है।” — इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर क्या-क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं? (2)
(vii) लेखक के अनुसार पर्यावरण के प्रति सामाजिक जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है? (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ग) प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन
(ii) – (घ) A गलत है, R सही है।
(iii) – (ग) वृक्षारोपण
(iv) – (ख) घरेलू कचरे का उचित निपटान
(v) – इस कथन का आशय यह है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें अपने व्यवहार में ऐसे बदलाव लाने चाहिए जिससे प्रकृति को नुकसान न हो और उसका संतुलन बना रहे।
(vi) – प्रदूषण के कारण मनुष्यों को साँस की बीमारियाँ, त्वचा रोग, जलजनित संक्रमण और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं।
(vii) – सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा, सामुदायिक सफाई अभियान, प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र की पहल, और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से संदेश प्रसारित किए जा सकते हैं।
- आज के समय में नैतिक शिक्षा का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। जब समाज में भौतिक प्रगति तो हो रही है, परंतु नैतिक मूल्यों में गिरावट देखी जा रही है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम नई पीढ़ी को न केवल ज्ञान, बल्कि चरित्र निर्माण की दिशा में भी मार्गदर्शन दें। नैतिक शिक्षा वह आधार है, जो व्यक्ति को सही और गलत में भेद करना सिखाती है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन में ईमानदारी, सहानुभूति, सत्य, कर्तव्यपरायणता और अनुशासन जैसे गुणों को आत्मसात करने की प्रेरणा देती है। जब कोई बच्चा सत्य बोलने, दूसरों की मदद करने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने का अभ्यास करता है, तभी वह एक उत्तरदायी नागरिक बनता है। दुर्भाग्यवश, आज विद्यालयों और परिवारों दोनों में नैतिक मूल्यों पर चर्चा कम होती जा रही है। प्रतिस्पर्धा की दौड़, अंकों की होड़ और तकनीकी व्यस्तता ने नैतिक शिक्षा को पीछे छोड़ दिया है। कई बार माता-पिता और शिक्षक स्वयं नैतिक व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाते, जिससे बच्चों में सही दिशा का अभाव रह जाता है। एक अच्छे समाज की नींव अच्छे नागरिकों से बनती है, और अच्छे नागरिक वही होते हैं जो अपने कर्तव्यों को समझते हैं, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं और सामाजिक हित को प्राथमिकता देते हैं। यदि नैतिक शिक्षा को प्रारंभिक स्तर से ही पढ़ाई का अनिवार्य हिस्सा बना दिया जाए, तो इससे आने वाले समय में ईमानदार, संवेदनशील और जिम्मेदार समाज का निर्माण किया जा सकता है। हमें यह समझना होगा कि प्रगति केवल तकनीकी उपलब्धियों से नहीं मापी जा सकती, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि समाज कितना न्यायपूर्ण, सहिष्णु और करुणाशील है।
प्रश्न –
(i) लेखक के अनुसार नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? (1)
(क) बच्चों को अधिक अंक दिलाना
(ख) प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी
(ग) सही और गलत में भेद करना सिखाना
(घ) तकनीकी ज्ञान बढ़ाना
(ii) कथन (A): नैतिक शिक्षा केवल धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त होती है। (1)
कारण (R): व्यवहारिक जीवन में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है।
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों गलत हैं।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) लेखक के अनुसार आज नैतिक शिक्षा में गिरावट का एक कारण क्या है? (1)
(क) पाठ्यक्रम की कठिनाई
(ख) विज्ञान विषयों का भार
(ग) अंकों की दौड़ और प्रतिस्पर्धा
(घ) खेलों की अधिकता
(iv) नैतिक शिक्षा किन गुणों को बढ़ावा देती है? (1)
(क) प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा
(ख) ईमानदारी और सहानुभूति
(ग) तर्क और गणित
(घ) शक्ति और अधिकार
(v) “एक अच्छे समाज की नींव अच्छे नागरिकों से बनती है।” — इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) लेखक के अनुसार नैतिक शिक्षा की अनुपस्थिति समाज पर किस प्रकार प्रभाव डालती है? (2)
(vii) विद्यालयों और परिवारों में नैतिक शिक्षा को कैसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है? (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ग) सही और गलत में भेद करना सिखाना
(ii) – (ख) A और R दोनों गलत हैं।
(iii) – (ग) अंकों की दौड़ और प्रतिस्पर्धा
(iv) – (ख) ईमानदारी और सहानुभूति
(v) – इस कथन का आशय यह है कि एक अच्छा समाज वही होता है जिसमें नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं, नैतिक व्यवहार अपनाते हैं और समाज के प्रति जिम्मेदारी महसूस करते हैं।
(vi) – नैतिक शिक्षा की अनुपस्थिति से समाज में भ्रष्टाचार, स्वार्थ, असहिष्णुता और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार बढ़ता है, जिससे सामाजिक ताना-बाना कमजोर होता है।
(vii) – नैतिक शिक्षा को पुनर्स्थापित करने के लिए विद्यालयों में नैतिक विषयों को अनिवार्य किया जाना चाहिए और परिवारों में माता-पिता को बच्चों के सामने नैतिक उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। साथ ही व्यवहार में अच्छे मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देनी चाहिए।
- स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी पूँजी होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति न केवल अपने जीवन का आनंद ले सकता है, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी सक्रिय भूमिका निभा सकता है। ‘स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है’ — यह उक्ति इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य अनिवार्य है। परंतु आज की जीवनशैली, खानपान की आदतें और भागदौड़ भरी दिनचर्या के कारण लोगों का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। जंक फूड, शारीरिक श्रम की कमी, देर रात तक मोबाइल या टीवी देखना, और तनावपूर्ण जीवन के कारण युवा से लेकर वृद्ध तक अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग, अनिद्रा और मानसिक अवसाद जैसी बीमारियाँ तेजी से फैल रही हैं। पहले जो रोग वृद्धावस्था में होते थे, अब वे किशोर अवस्था में ही दिखाई देने लगे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है — अनुशासनहीन जीवनशैली और स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा। एक ओर हम स्वास्थ्य बीमा और महंगे इलाज की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव करके अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। प्रतिदिन कम-से-कम 30 मिनट व्यायाम, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, समय पर खाना, और सकारात्मक सोच — ये पाँच बातें अगर हम अपने जीवन में नियमित करें, तो दवाओं पर निर्भरता काफी हद तक कम हो सकती है। इसके अतिरिक्त योग और ध्यान जैसी प्राचीन भारतीय पद्धतियाँ भी शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में अत्यंत लाभकारी हैं। स्वास्थ्य केवल शरीर की बीमारी से मुक्ति नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्ण सुख-शांति की स्थिति है। यदि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो न कोई सफलता टिकेगी, न कोई आनंद स्थायी रहेगा। अतः यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए और जीवनशैली को संतुलित एवं अनुशासित बनाया जाए।
प्रश्न –
(i) लेखक के अनुसार आज की स्वास्थ्य समस्याओं का एक प्रमुख कारण क्या है? (1)
(क) महंगा इलाज
(ख) समय की कमी
(ग) अनुशासनहीन जीवनशैली
(घ) अधिक पढ़ाई
(ii) कथन (A): युवा वर्ग में स्वास्थ्य समस्याएँ तेजी से बढ़ रही हैं।
कारण (R): जंक फूड और तनावपूर्ण जीवन इसका कारण है। (1)
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) स्वास्थ्य की देखभाल से क्या लाभ हो सकता है? (1)
(क) दवाइयाँ बंद हो सकती हैं
(ख) समाज से दूरी बनी रहती है
(ग) शिक्षा बाधित होती है
(घ) बीमारियाँ बढ़ती हैं
(iv) लेखक के अनुसार स्वास्थ्य का सही अर्थ क्या है? (1)
(क) अस्पताल न जाना
(ख) केवल शारीरिक शक्ति
(ग) बीमारियों से छुटकारा
(घ) शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन
(v) “स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।” — इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) लेखक ने स्वस्थ जीवन के लिए कौन-कौन सी पाँच आदतें आवश्यक बताई हैं? (2)
(vii) लेखक के अनुसार योग और ध्यान का क्या महत्त्व है? (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ग) अनुशासनहीन जीवनशैली
(ii) – (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(iii) – (क) दवाइयाँ बंद हो सकती हैं
(iv) – (घ) शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन
(v) – इस कथन का आशय है कि जब शरीर स्वस्थ होता है, तभी व्यक्ति मानसिक रूप से भी सक्रिय और सकारात्मक होता है। शारीरिक स्वास्थ्य मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बनाए रखने में सहायक होता है।
(vi) – लेखक के अनुसार प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, समय पर भोजन करना और सकारात्मक सोच — ये पाँच आदतें स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक हैं।
(vii) – लेखक के अनुसार योग और ध्यान शरीर और मन दोनों के संतुलन को बनाए रखने में सहायक हैं। ये बीमारियों से बचाने के साथ-साथ मानसिक शांति और अनुशासन भी प्रदान करते हैं।
- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक जागरूकता का आंदोलन भी था। इस आंदोलन की सफलता में जहाँ राजनीतिक नेताओं की भूमिका थी, वहीं समाज के प्रत्येक वर्ग ने भी इसमें भाग लिया। किसानों, मजदूरों, महिलाओं, विद्यार्थियों और यहां तक कि बच्चों ने भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाई। आंदोलन की विशेषता यह थी कि इसमें किसी एक वर्ग या समुदाय का वर्चस्व नहीं था, बल्कि यह एक सामूहिक चेतना का परिणाम था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को जन-जन से जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा और स्वदेशी जैसे सिद्धांतों के माध्यम से लोगों को आत्मबल और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। चरखा केवल एक औजार नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया था। खादी पहनना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और देशी माल का उपयोग करना केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का मुद्दा बन गया था। महिलाएँ भी पीछे नहीं रहीं — उन्होंने आंदोलनों में भाग लिया, जेल गईं, विदेशी वस्त्र जलाए और घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया। देश के विभिन्न क्षेत्रों में चलाए गए आंदोलनों ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक चेतना है, जो अन्याय के विरुद्ध संगठित हो सकती है। स्वतंत्रता आंदोलन ने देश को केवल राजनीतिक आज़ादी ही नहीं दी, बल्कि यह आत्मगौरव, एकता और राष्ट्रीयता की भावना भी लेकर आया। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी यह आंदोलन हमें प्रेरणा देता है कि जब समाज अन्याय, असमानता या भ्रष्टाचार से जूझ रहा हो, तो एकजुट होकर सत्य, अहिंसा और अनुशासन के मार्ग पर चलकर परिवर्तन लाया जा सकता है।
प्रश्न –
(i) स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? (1)
(क) केवल राजनीतिक दलों का समर्थन
(ख) एक वर्ग का आंदोलन होना
(ग) सभी वर्गों की भागीदारी
(घ) केवल सैनिकों की भागीदारी
(ii) कथन (A): महात्मा गांधी ने आंदोलन को सीमित लोगों तक रखा।
कारण (R): उन्होंने जन-जन को जोड़ने का प्रयास नहीं किया। (1)
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों गलत हैं।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) स्वतंत्रता आंदोलन में चरखे का क्या प्रतीकात्मक अर्थ था? (1)
(क) कृषि का प्रतीक
(ख) आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का प्रतीक
(ग) मशीन विरोध का प्रतीक
(घ) विदेशी वस्त्रों का प्रतीक
(iv) लेखक के अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन ने देश को क्या सिखाया? (1)
(क) केवल सरकार बदलना
(ख) विदेशी भाषा सीखना
(ग) असहयोग करना
(घ) आत्मगौरव, एकता और राष्ट्रीयता
(v) “स्वदेशी केवल आर्थिक नीति नहीं, आत्मसम्मान का प्रतीक था।” — इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) महिलाएँ स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार सक्रिय रहीं? (2)
(vii) आज के संदर्भ में स्वतंत्रता आंदोलन से क्या प्रेरणा ली जा सकती है? (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ग) सभी वर्गों की भागीदारी
(ii) – (ख) A और R दोनों गलत हैं।
(iii) – (ख) आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का प्रतीक
(iv) – (घ) आत्मगौरव, एकता और राष्ट्रीयता
(v) – इस कथन का आशय यह है कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि अंग्रेजों के प्रति विरोध और अपने देश के प्रति गर्व का प्रतीक था। यह आत्मसम्मान की भावना का प्रदर्शन था।
(vi) – महिलाएँ आंदोलनों में शामिल हुईं, विदेशी वस्त्र जलाए, जेल गईं, जन जागरूकता फैलाने में सहयोग किया और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष में भाग लिया।
(vii) – आज के संदर्भ में यह आंदोलन सिखाता है कि यदि समाज संगठित हो, तो सत्य और अहिंसा के माध्यम से किसी भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदला जा सकता है। यह नागरिक चेतना और उत्तरदायित्व की प्रेरणा देता है।
- शहरीकरण आधुनिक युग की एक बड़ी पहचान बन चुका है। गाँवों से लोग बेहतर सुविधाओं, रोजगार, शिक्षा और जीवनशैली की खोज में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। परिणामस्वरूप शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। यातायात का दबाव, वायु प्रदूषण, कचरे का ढेर, पेयजल की कमी, और आवास की समस्याएँ आज के शहरी जीवन का हिस्सा बन गई हैं। अधिक जनसंख्या के कारण संसाधनों पर बोझ बढ़ता है और नागरिक सुविधाएँ प्रभावित होती हैं। साथ ही, महानगरों में सामाजिक एकता की भावना भी कमजोर होती जा रही है क्योंकि यहाँ लोग अपने-अपने जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं कि पड़ोसी से भी परिचय नहीं होता। दूसरी ओर, गाँवों का खाली होते जाना एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि वहाँ की कृषि व्यवस्था, परंपराएँ और सांस्कृतिक विरासत धीरे-धीरे समाप्त हो रही हैं। यह असंतुलन न केवल सामाजिक, बल्कि आर्थिक समस्याओं को भी जन्म देता है। शहरीकरण को यदि नियोजित रूप से न बढ़ाया गया तो यह एक अभिशाप बन सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि गाँवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और रोजगार के साधनों का विकास किया जाए ताकि वहाँ के लोग अपने स्थान पर ही संतुष्ट और आत्मनिर्भर बन सकें। साथ ही, शहरों की योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर नागरिक को आवास, परिवहन, स्वच्छता और हरियाली जैसे मूलभूत अधिकार सुनिश्चित हों। स्मार्ट सिटी योजना, हरित परिवहन, कचरा प्रबंधन और नागरिक सहभागिता जैसे उपाय यदि ईमानदारी से लागू किए जाएँ, तो शहरीकरण को संतुलित और लाभकारी बनाया जा सकता है। शहरीकरण को पूरी तरह रोकना संभव नहीं, परंतु इसे सतत और समावेशी बनाना हमारे भविष्य के लिए अनिवार्य है।
प्रश्न –
(i) शहरीकरण की एक प्रमुख समस्या क्या है? (1)
(क) शिक्षा का अभाव
(ख) आबादी में कमी
(ग) वायु प्रदूषण और कचरा
(घ) अधिक हरियाली
(ii) कथन (A): गाँवों से पलायन शहरीकरण को बढ़ावा देता है।
कारण (R): गाँवों में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। (1)
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) लेखक के अनुसार शहरी लोगों में क्या कमी होती जा रही है? (1)
(क) शिक्षा की भावना
(ख) सामाजिक एकता की भावना
(ग) स्वास्थ्य की भावना
(घ) व्यवसाय की भावना
(iv) शहरीकरण की प्रक्रिया को लाभकारी कैसे बनाया जा सकता है? (1)
(क) गाँवों को नजरअंदाज करके
(ख) केवल बड़े शहर बसाकर
(ग) सतत और नियोजित विकास द्वारा
(घ) अधिक लोगों को शहर बुलाकर
(v) “शहरीकरण यदि नियोजित न हो तो अभिशाप बन सकता है।” — इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) लेखक के अनुसार गाँवों की उपेक्षा से कौन-कौन सी हानियाँ होती हैं? (2)
(vii) शहरी जीवन को संतुलित और सुविधाजनक बनाने के लिए किन उपायों को अपनाने की आवश्यकता है? (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ग) वायु प्रदूषण और कचरा
(ii) – (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(iii) – (ख) सामाजिक एकता की भावना
(iv) – (ग) सतत और नियोजित विकास द्वारा
(v) – इस कथन का आशय है कि यदि शहरों का विकास बिना योजना और नियंत्रण के किया गया, तो वहाँ भीड़भाड़, प्रदूषण, संसाधनों की कमी और जीवन की कठिनाइयाँ इतनी बढ़ जाएँगी कि जीवन असहज हो जाएगा।
(vi) – गाँवों की उपेक्षा से वहाँ की कृषि, परंपराएँ, संस्कृति और जनसंख्या प्रभावित होती है, जिससे सामाजिक असंतुलन और आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है।
(vii) – शहरी जीवन को संतुलित बनाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना, हरित परिवहन, कचरा प्रबंधन, स्वच्छता, हरियाली और नागरिक सहभागिता जैसे उपाय अपनाने चाहिए।
- भारतीय परिवार व्यवस्था दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। यह केवल एक सामाजिक ढाँचा नहीं, बल्कि जीवन के मूल्यों, परंपराओं और नैतिकताओं का स्रोत रही है। संयुक्त परिवार प्रणाली, जिसमें कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती थीं, ने भारतीय समाज को एकता, सहयोग, सहनशीलता और सेवा जैसे गुणों से भरपूर बनाया। बड़े-बुज़ुर्गों का मार्गदर्शन, बच्चों की सामूहिक परवरिश और पारिवारिक उत्तरदायित्वों का समान वितरण इस व्यवस्था की विशेषताएँ थीं। परंतु बदलते समय के साथ इस पारंपरिक व्यवस्था में भी कई बदलाव आए हैं। शहरीकरण, नौकरी के लिए स्थान परिवर्तन, आधुनिक जीवनशैली, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बढ़ती चाह ने संयुक्त परिवार को छोटे परिवारों में बदल दिया है। अब परिवार सीमित सदस्यीय होते जा रहे हैं, जिनमें एकल जीवनशैली और व्यक्तिगत प्राथमिकताएँ प्रमुख हो गई हैं। इससे पारिवारिक भावनाएँ, सामाजिक सहयोग और पीढ़ियों के बीच संवाद की कमी होने लगी है। बुज़ुर्गों को अकेलापन और उपेक्षा का अनुभव होता है, जबकि बच्चे अपने दादा-दादी या नाना-नानी से मिलने वाले नैतिक मूल्यों से वंचित रह जाते हैं। हालांकि, यह भी एक तथ्य है कि छोटे परिवारों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत विकास और आधुनिक जीवन के अनुकूलन की अधिक संभावनाएँ होती हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम दोनों व्यवस्थाओं की अच्छाइयों को आत्मसात करें। यदि हम पारिवारिक संबंधों में संवाद, सहयोग, आदर और स्नेह बनाए रखें, तो चाहे परिवार छोटा हो या बड़ा, वह आत्मिक सुख का केंद्र बन सकता है। भारतीय परिवार व्यवस्था की जड़ें गहरी हैं, और इन मूल्यों को आधुनिक संदर्भ में पुनः जाग्रत करना ही सच्चे अर्थों में प्रगति होगी।
प्रश्न –
(i) भारतीय संयुक्त परिवार की एक विशेषता क्या थी? (1)
(क) प्रतियोगिता
(ख) व्यक्तिगत स्वतंत्रता
(ग) सामूहिक उत्तरदायित्व
(घ) अकेलापन
(ii) कथन (A): आधुनिक जीवनशैली ने संयुक्त परिवारों को समाप्त कर दिया है।
कारण (R): लोग अब सामाजिक संबंधों को प्राथमिकता देते हैं। (1)
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, R गलत है।
(ग) A गलत है, R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
(iii) छोटे परिवारों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? (1)
(क) सामूहिक परवरिश
(ख) बड़े-बुज़ुर्गों का मार्गदर्शन
(ग) निर्णय लेने की स्वतंत्रता
(घ) पारिवारिक तनाव
(iv) लेखक के अनुसार पारिवारिक व्यवस्था की प्रगति किसमें निहित है? (1)
(क) केवल पारंपरिक मूल्यों में
(ख) संयुक्त परिवार को समाप्त करना
(ग) छोटे परिवार अपनाना
(घ) दोनों व्यवस्थाओं की अच्छाइयों को आत्मसात करना
(v) “भारतीय परिवार व्यवस्था केवल सामाजिक ढाँचा नहीं है।” — इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) संयुक्त परिवारों में किस प्रकार के नैतिक लाभ होते थे? (2)
(vii) आधुनिक जीवनशैली के बावजूद पारिवारिक मूल्यों को कैसे जीवित रखा जा सकता है? (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ग) सामूहिक उत्तरदायित्व
(ii) – (ख) A सही है, R गलत है।
(iii) – (ग) निर्णय लेने की स्वतंत्रता
(iv) – (घ) दोनों व्यवस्थाओं की अच्छाइयों को आत्मसात करना
(v) – इस कथन का आशय यह है कि भारतीय परिवार व्यवस्था केवल रिश्तों के नाम पर आधारित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने के संस्कार, नैतिकता, सहयोग और संस्कारों की एक जीवन शैली है।
(vi) – संयुक्त परिवारों में बड़े-बुज़ुर्गों का मार्गदर्शन, बच्चों को नैतिक शिक्षा, अनुशासन, सेवा, सहनशीलता और एकता जैसे गुण सिखाए जाते थे जो व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते थे।
(vii) – आधुनिक जीवनशैली में भी यदि पारिवारिक संवाद बनाए रखा जाए, बुज़ुर्गों का सम्मान किया जाए, बच्चों को पारंपरिक संस्कार सिखाए जाएँ और आपसी सहयोग की भावना हो, तो पारिवारिक मूल्य जीवित रह सकते हैं।
- भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहाँ विभिन्न धर्म, भाषाएँ, जातियाँ, और संस्कृतियाँ सह-अस्तित्व में हैं। यह विविधता केवल हमारी पहचान ही नहीं, बल्कि हमारी शक्ति भी है। भारत की सांस्कृतिक विविधता ने इसे एक समृद्ध और जीवंत राष्ट्र बनाया है, जहाँ हर पर्व, हर परंपरा, और हर भाषा अपनी अनूठी पहचान रखती है। उत्तर में हिमालय की चोटियाँ, दक्षिण में समुद्र की लहरें, पूरब की पर्वत श्रृंखलाएँ और पश्चिम के रेगिस्तान — ये सब मिलकर भारत की भौगोलिक विविधता को दर्शाते हैं। फिर भी, इतनी विविधता के बावजूद भारतीय समाज में एकता की भावना बनी रहती है। यह भावना ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की अवधारणा में निहित है, जिसका अर्थ है — ‘पूरा विश्व एक परिवार है’। भारत के संविधान में भी इस एकता को सर्वोपरि माना गया है। धर्मनिरपेक्षता, समानता और बंधुता जैसे सिद्धांत इसी एकता को बनाए रखने के लिए हैं। हालाँकि, समय-समय पर कुछ ऐसे क्षण आए हैं जब इस एकता को चुनौतियाँ मिली हैं — जैसे भाषायी संघर्ष, सांप्रदायिक तनाव, और क्षेत्रीय मतभेद। परंतु भारतीय समाज ने हर बार इन मतभेदों को पार करके एकता को प्राथमिकता दी है। यह एकता केवल राजनीतिक या कानूनी नहीं, बल्कि भावनात्मक है। जब कोई राष्ट्रीय आपदा आती है, तो देशभर से लोग बिना भेदभाव के एक-दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। त्योहारों पर, खेलों में, और राष्ट्रीय आयोजनों में यह भावना और अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। विविधता में एकता भारत की आत्मा है, और यही विशेषता उसे अन्य राष्ट्रों से अलग करती है। हमें इस विरासत पर गर्व है और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है।
प्रश्न –
(i) लेखक के अनुसार भारत की विविधता किस बात की परिचायक है? (1)
(क) दुर्बलता की
(ख) असमानता की
(ग) शक्ति की
(घ) विघटन की
(ii) कथन (A): भारतीय समाज में केवल भौगोलिक एकता है।
कारण (R): भारत में अलग-अलग धर्म और भाषाएँ हैं। (1)
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, R गलत है।
(ग) A गलत है, R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
(iii) विविधता में एकता की भावना किस सिद्धांत से जुड़ी है? (1)
(क) ‘स्वदेशी’
(ख) ‘अहिंसा’
(ग) ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’
(घ) ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’
(iv) लेखक के अनुसार भारत की एकता किस प्रकार की है? (1)
(क) केवल संवैधानिक
(ख) केवल धार्मिक
(ग) केवल भाषायी
(घ) भावनात्मक
(v) “विविधता में एकता भारत की आत्मा है।” — इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) लेखक के अनुसार भारत में एकता को कौन-कौन सी चुनौतियाँ मिलती रही हैं? (2)
(vii) भारत की एकता को बनाए रखने के लिए नागरिकों को क्या करना चाहिए? (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ग) शक्ति की
(ii) – (ग) A गलत है, R सही है।
(iii) – (ग) ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’
(iv) – (घ) भावनात्मक
(v) – इस कथन का आशय यह है कि भारत में अनेकता होते हुए भी एकता की भावना गहराई से जुड़ी हुई है। अलग-अलग धर्म, भाषा और क्षेत्र होते हुए भी लोग एक राष्ट्र के रूप में संगठित रहते हैं।
(vi) – लेखक के अनुसार भारत की एकता को भाषायी संघर्ष, सांप्रदायिक तनाव और क्षेत्रीय मतभेद जैसी चुनौतियाँ मिली हैं।
(vii) – भारत की एकता बनाए रखने के लिए नागरिकों को सभी धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, समानता और बंधुता को अपनाना चाहिए और समाज में सौहार्द बनाए रखना चाहिए।
- आज का युग सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है। कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकों ने मानव जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। संचार, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग—हर क्षेत्र में तकनीकी प्रगति ने न केवल कार्य को सरल बनाया है, बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत की है। आज व्यक्ति कुछ ही क्षणों में दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकता है, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकता है, डॉक्टर से वीडियो कॉल पर सलाह ले सकता है, या अपने घर बैठे आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सकता है। यह सब तकनीक की देन है। परंतु हर परिवर्तन के साथ कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं। तकनीकी विकास के कारण मनुष्य की शारीरिक सक्रियता में कमी आई है। मशीनों पर बढ़ती निर्भरता ने श्रम को कम कर दिया है, जिससे अनेक शारीरिक और मानसिक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। इसके अतिरिक्त, इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग बच्चों में ध्यान की कमी, सामाजिक अलगाव और मानसिक तनाव का कारण बन रहा है। तकनीकी उपकरणों का असंतुलित प्रयोग पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। कई बार परिवार के सदस्य एक ही घर में होते हुए भी एक-दूसरे से संवाद नहीं करते, क्योंकि वे मोबाइल या कंप्यूटर में व्यस्त रहते हैं। इसके बावजूद, यदि तकनीक का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, तो यह मानव जीवन की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा सकती है। हमें यह समझना होगा कि तकनीक एक साधन है, साध्य नहीं। इसका उपयोग सुविधा, विकास और सेवा के लिए होना चाहिए, न कि आलस्य, असामाजिकता और निर्भरता के लिए। यदि हम तकनीक को अपने नियंत्रण में रखें और उसके सकारात्मक पक्ष को अपनाएँ, तो यह युग वास्तव में मानव सभ्यता के उत्कर्ष का युग बन सकता है।
प्रश्न –
(i) तकनीकी प्रगति से मानव जीवन में कौन-सा लाभ नहीं हुआ है? (1)
(क) समय की बचत
(ख) संचार में सुविधा
(ग) शिक्षा में बाधा
(घ) संसाधनों की बचत
(ii) कथन (A): तकनीक का असंतुलित प्रयोग परिवारिक संबंधों को प्रभावित करता है।
कारण (R): लोग तकनीकी उपकरणों में अधिक समय बिताते हैं। (1)
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) लेखक के अनुसार तकनीक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? (1)
(क) मनुष्य को पूर्णतः मशीनों पर निर्भर बनाना
(ख) समाज में असामाजिकता फैलाना
(ग) सुविधा, विकास और सेवा
(घ) शिक्षा को कठिन बनाना
(iv) तकनीकी विकास की एक चुनौती क्या है? (1)
(क) संचार में वृद्धि
(ख) ज्ञान का प्रसार
(ग) श्रम की अधिकता
(घ) शारीरिक सक्रियता में कमी
(v) “तकनीक एक साधन है, साध्य नहीं।” — इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) लेखक के अनुसार बच्चों पर तकनीकी उपकरणों का क्या प्रभाव पड़ रहा है? (2)
(vii) तकनीक के विवेकपूर्ण प्रयोग से मानव जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ग) शिक्षा में बाधा
(ii) – (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(iii) – (ग) सुविधा, विकास और सेवा
(iv) – (घ) शारीरिक सक्रियता में कमी
(v) – इसका आशय यह है कि तकनीक को केवल एक माध्यम की तरह प्रयोग करना चाहिए, वह जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। हमें तकनीक का प्रयोग अपने कार्यों को सरल और उपयोगी बनाने के लिए करना चाहिए, न कि उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाना चाहिए।
(vi) – लेखक के अनुसार तकनीकी उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से बच्चों में ध्यान की कमी, सामाजिक अलगाव और मानसिक तनाव जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
(vii) – यदि तकनीक का उपयोग सीमित, संतुलित और सकारात्मक कार्यों के लिए किया जाए तो इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और जीवन की गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार लाया जा सकता है।
- भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से मत देने का अधिकार प्राप्त है, जिससे वह देश की सरकार चुन सकता है। यह अधिकार भारतीय संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है और इसका उद्देश्य है — जनता को शासन में भागीदारी का अवसर देना। लोकतंत्र का मूल आधार है – “जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए।” इसका अर्थ है कि सरकार जनता की इच्छाओं के अनुरूप काम करे, उसकी समस्याओं को समझे और उनके समाधान के लिए उत्तरदायी हो। परंतु लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। एक सच्चे लोकतंत्र में नागरिकों की सहभागिता हर स्तर पर आवश्यक होती है — जैसे कानूनों के पालन में, अपने कर्तव्यों को निभाने में, भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज़ उठाने में और समाज के कल्याण में भागीदारी निभाने में। दुर्भाग्यवश, आज कई नागरिक अपने अधिकार तो मांगते हैं, पर कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। मताधिकार का प्रयोग न करना, गलत लोगों को चुनना, या केवल जाति, धर्म, या भावनात्मक मुद्दों पर वोट देना — ये लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे हैं। एक जागरूक नागरिक ही स्वस्थ लोकतंत्र की नींव रख सकता है। इसके लिए शिक्षा, सूचना का अधिकार और पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक हैं। जब जनता शिक्षित, जागरूक और संगठित होती है, तो सरकार की जवाबदेही भी बढ़ती है। लोकतंत्र की सफलता किसी एक संस्था पर नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच, व्यवहार और सक्रियता पर निर्भर करती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र सशक्त और न्यायपूर्ण हो, तो हमें अपने कर्तव्यों को भी उतनी ही गंभीरता से निभाना होगा, जितनी गंभीरता से हम अपने अधिकारों की अपेक्षा रखते हैं।
प्रश्न –
(i) लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है? (1)
(क) सरकार को शक्तिशाली बनाना
(ख) केवल मतदान कराना
(ग) जनता को शासन में भागीदारी देना
(घ) केवल राजनीतिक दलों को बढ़ावा देना
(ii) कथन (A): लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित होता है।
कारण (R): चुनाव के बाद नागरिक की कोई भूमिका नहीं होती। (1)
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A सही है, R गलत है।
(ग) A गलत है, R सही है।
(घ) A और R दोनों गलत हैं।
(iii) लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा किससे होता है? (1)
(क) उच्च शिक्षा से
(ख) जाति, धर्म या भावना आधारित मतदान से
(ग) राष्ट्रीय पर्व से
(घ) विदेशी यात्राओं से
(iv) लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? (1)
(क) केवल नेताओं पर
(ख) एक संस्था पर
(ग) पूरे समाज की सोच और सक्रियता पर
(घ) केवल संविधान पर
(v) “लोकतंत्र केवल अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी है।” — इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) लेखक के अनुसार एक जागरूक नागरिक किन-किन कार्यों में भागीदारी निभाता है? (2)
(vii) लोकतंत्र को सशक्त और न्यायपूर्ण बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ग) जनता को शासन में भागीदारी देना
(ii) – (घ) A और R दोनों गलत हैं।
(iii) – (ख) जाति, धर्म या भावना आधारित मतदान से
(iv) – (ग) पूरे समाज की सोच और सक्रियता पर
(v) – इस कथन का आशय है कि लोकतंत्र में नागरिकों को केवल अधिकारों की माँग नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने कर्तव्यों जैसे मतदान करना, नियमों का पालन करना और ईमानदारी से समाज का भला सोचना भी निभाना चाहिए।
(vi) – एक जागरूक नागरिक मतदान करता है, कानूनों का पालन करता है, भ्रष्टाचार का विरोध करता है और समाज के कल्याणकारी कार्यों में सक्रिय रहता है।
(vii) – लोकतंत्र को सशक्त और न्यायपूर्ण बनाने के लिए शिक्षा का प्रसार, सूचना का अधिकार, पारदर्शिता, और नागरिकों की सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है।
- आज की दुनिया में समय का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। आधुनिक जीवनशैली, तकनीकी प्रगति और बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने समय के मूल्य को अत्यधिक बढ़ा दिया है। समय एक ऐसा संसाधन है जिसे न तो संचित किया जा सकता है, न ही वापस पाया जा सकता है। हर दिन के 24 घंटे सभी को समान रूप से मिलते हैं, परंतु जो व्यक्ति इन घंटों का सदुपयोग करना जानता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय प्रबंधन केवल एक कला नहीं, बल्कि एक आवश्यक जीवन-कौशल है। इसका सीधा संबंध व्यक्ति की उत्पादकता, मानसिक संतुलन और लक्ष्य-प्राप्ति से होता है। यदि कोई छात्र समय पर अध्ययन करता है, तो परीक्षा के समय उसे तनाव नहीं होता। एक व्यवसायी यदि अपने कार्यों की योजना बनाकर चले, तो उसे बेहतर निर्णय लेने और अवसरों का लाभ उठाने में सुविधा होती है। वहीं जो लोग समय को हल्के में लेते हैं, वे अक्सर बाद में पछताते हैं। समय की अवहेलना करना आलस्य, असफलता और असमय तनाव का कारण बन सकता है। समय के साथ चलना और उसका सम्मान करना न केवल व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि जीवन को अनुशासित, लक्ष्य-केंद्रित और संतुलित बनाता है। आज के विद्यार्थी और युवा यदि समय का मूल्य पहचानें और उसे व्यर्थ न गँवाएँ, तो न केवल वे अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए कहा गया है – “काल चक्र कभी रुकता नहीं, जो इसके साथ चलता है, वही आगे बढ़ता है।”
प्रश्न –
(i) लेखक के अनुसार समय का सबसे बड़ा गुण क्या है? (1)
(क) इसे संचित किया जा सकता है
(ख) यह लौटकर आता है
(ग) यह सबको समान रूप से मिलता है
(घ) यह धीरे चलता है
(ii) कथन (A): समय प्रबंधन एक आवश्यक जीवन-कौशल है।
कारण (R): यह लक्ष्य-प्राप्ति और मानसिक संतुलन में सहायता करता है। (1)
(क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(ख) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(ग) A सही है, R गलत है।
(घ) A गलत है, R सही है।
(iii) समय की उपेक्षा का एक परिणाम क्या हो सकता है? (1)
(क) आत्मनिर्भरता
(ख) सकारात्मक सोच
(ग) आलस्य और असफलता
(घ) जीवन में प्रेरणा
(iv) समय का सम्मान करने से व्यक्ति में कौन-से गुण विकसित होते हैं? (1)
(क) आलस्य और संदेह
(ख) अनुशासन और लक्ष्यबोध
(ग) क्रोध और अव्यवस्था
(घ) नकारात्मक सोच
(v) “हर दिन के 24 घंटे सभी को समान मिलते हैं” — इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(vi) लेखक के अनुसार एक छात्र के लिए समय प्रबंधन का क्या लाभ होता है? (2)
(vii) युवा पीढ़ी यदि समय का सदुपयोग करे तो समाज को क्या लाभ हो सकता है? (2)
उत्तर कुंजी
(i) – (ग) यह सबको समान रूप से मिलता है
(ii) – (क) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(iii) – (ग) आलस्य और असफलता
(iv) – (ख) अनुशासन और लक्ष्यबोध
(v) – इसका आशय यह है कि हर व्यक्ति को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि वह इन घंटों का उपयोग कैसे करता है। समय का सही उपयोग व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, जबकि उसका दुरुपयोग पीछे धकेलता है।
(vi) – लेखक के अनुसार यदि छात्र समय का सही उपयोग करता है, तो उसे परीक्षा के समय तनाव का सामना नहीं करना पड़ता और वह आत्मविश्वास के साथ सफलता प्राप्त कर सकता है।
(vii) – यदि युवा समय का सदुपयोग करें तो वे अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।